फिल्म
द फर्स्ट फिल्म को बेस्ट फिल्म और पीयूष ठाकुर को मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड
फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का समापन
पांच श्रेणियों में वितरित किए गए पुरस्कार... तीन फिल्मों को मिला विशेष जूरी पुरस्कार
मैक्सिको से सेसेलिया डियाज़ और अमेरिका से कवि किरण भट्ट हुए शामिल
रायपुर / रायपुर आर्ट, लिटरेचर एवं फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। पद्मश्री पंडी राम मंडावी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। फेस्टिवल के तीसरे संस्करण में 5 फिल्मों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही 3 फिल्मों को विशेष जूरी अवॉर्ड दिया गया। फिल्म समारोह के उपरांतअवॉर्ड सेरेमनी में द फर्स्ट फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म पुरस्कार, पीयूष ठाकुर को द फर्स्ट फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर, थुनई को सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी अवॉर्ड और सुमित्रा साहू को जमगहीन फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। RALFF25 के विशेष पुरस्कार की श्रेणी में मन आसाई को सर्वश्रेष्ठ सामाजिक फिल्म अवॉर्ड से पुरस्कृत किया गया। विशेष जूरी पुरस्कार की श्रेणी में कमजखिला, ब्यांव, हेल्प योरसेल्फ को सम्मानित किया गया।
इस मौके पर मुख्य अतिथि पद्मश्री पंडी राम मंडावी ने सभी पुरस्कृत फिल्म और निर्माताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन कलाकारों को मंच प्रदान करते हैं और लोक कलाओं को नई पहचान दिलाने में सहायक होते हैं। पंडी राम मंडावी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल कला-संस्कृति को बढ़ावा देते हैं बल्कि युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का अवसर भी प्रदान करते हैं। फिल्म फेस्टिवल में मैक्सिको से आई सेसेलिया डियाज़ ने कहा कि फिल्म समाज का दर्पण है। समाज को जागरूक करने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। सेसेलिया डियाज़ मैक्सिको में स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार काम कर रहीं हैं वहीं अमेरिका से आए कवि किरण भट्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ कला संस्कृति का गढ़ है। यह कार्यक्रम कला और संस्कृति को सहजने का अच्छा प्रयास है। फिल्म फेस्टिवल में शामिल होकर बहुत रोमांचित हूं।
इस अवसर पर कवि एवं गीतकार मीर अली मीर ने कहा कि आज के दौर में कहानी कहने के माध्यम बदल रहे हैं और फिल्मों के ज़रिये सामाजिक विषयों को प्रस्तुत करना एक प्रभावशाली तरीका बन चुका है। यह फेस्टिवल हमारी कला और संस्कृति को सहेजने और संरक्षित करने का एक सराहनीय प्रयास है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति बलदेव भाई शर्मा ने कहा कि यह फेस्टिवल कला, साहित्य और फिल्म का एक अनोखा संगम है, जो युवा पीढ़ी को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने का अद्भुत अवसर देता है। आने वाले समय में यह फेस्टिवल भारतीय सिनेमा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा।
फेस्टिवल क्यूरेटर प्रीति उपाध्याय शुक्ला ने बताया कि यह फेस्टिवल केवल फिल्म प्रदर्शन का माध्यम नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक अनूठा प्रयास है। यहां क्षेत्रीय और राष्ट्रीय फिल्मकारों के बीच संवाद स्थापित हुआ है, जो कला के नए आयामों को जन्म देगा। हमारा उद्देश्य है कि इस मंच से छत्तीसगढ़ की कहानियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। अगले संस्करण में और अधिक फिल्मों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जोड़ने की योजना है।
रायपुर आर्ट, लिटरेचर एवं फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर कुणाल शुक्ला ने कहा कि यह फेस्टिवल नए और प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओं को मंच प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हमारी कोशिश है कि यहां प्रदर्शित होने वाली फिल्मों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों और जीवन की कहानियों को एक नई दिशा मिले। फेस्टिवल ने छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माताओं के लिए भी नई संभावनाएं खोली हैं।
चाइल्ड फिल्म मेकर ने बनाई फिल्म
बी-साइड फिल्म फेस्टिवल में 15 साल के चाइल्ड फिल्म मेकर की फिल्म बी-साइड का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की पहली बायोपिक फिल्म मंदराजी की भी स्क्रीनिंग की गई।
परिचर्चा, कार्यशाला और फिल्म की स्क्रीनिंग
फेस्टिवल के अवसर पर परिचर्चा और कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। परिचर्चा के पहले सत्र में जिंदगी... कैसी है पहेली विषय पर मुकेश पांडेय , अज़ीम उद्दीन, भागवत जायसवाल और दिव्यांश ने अपनी बात रखी। वहीं दूसरे सत्र में दिस क्राइंग अर्थ, दीज़ वीपिंग शोर्स (ट्रांसनेशनल इंडिजिनस डायलॉग) पर मीर अली मीर, सेसिलिया डियाज़, और किरण भट्ट ने अपनी राय रखी। हिंदी शॉर्ट फिल्में - कदम, बंटू'स गैंग, बोटल, द स्ट्रीट एंजल, 04, बिटवीन वर्ल्ड्स तथा डॉक्यूमेंट्री - चिंताराम, जुनून और ज़माना का प्रदर्शन किया गया। साथ ही जम्मू-कश्मीर से केरल तक की बहुभाषी शॉर्ट फिल्में - ब्यांव (राजस्थानी), प्रदक्षिणा (मराठी), एनाउंसमेंट - ए मार्टर स्टोरी (हिंदी), थुनाई (तमिल), हेल्प योरसेल्फ (अंग्रेज़ी/हिंदी), मन आसाई (तमिल), जमगहीन (छत्तीसगढ़ी), कमजखिला (अन्य), द फर्स्ट फिल्म (हिंदी) की स्क्रीनिंग की गई। कार्यशाला के पहले सत्र में कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्म मेकिंग पर डॉ. नरेंद्र त्रिपाठी, परफेक्ट योर मैन्युस्क्रिप्ट विषय पर लक्ष्मी वल्लुरी और इमोशन्स थ्रू एडिटिंग पर बिरजू कुमार रजक ने स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और फिल्म निर्माण की बारीकियों पर अपनी बात रखी।
फेस्टिवल में डॉ. अनिल द्विवेदी (फ़िल्म क्रिटिक और वरिष्ठ पत्रकार) मॉडरेट किया। साथ ही स्वाति पांडे और आरजे नमित ने कार्यक्रम को होस्ट किया।
अवॉर्ड सेरेमनी में मनोज वर्मा, अनिरुद्ध दुबे, नीरज ग्वाल, रॉकी दासवानी, छत्तीसगढ़ इप्टा की टीम, रुचि शर्मा, राजकुमार सोनी,संजय शेखर,ओंकार धनगर, डॉ. अशोक बैरागी, ऋषव लोध, तनवीर अरिद,विजय जैन ,मनोज पाठक,ओंकार धनगर,मुकेश अग्रवाल समेत कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय और आफ्ट यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी सहित कई सिनेप्रेमी शामिल हुए.
आठ फरवरी को छत्तीसगढ़ के सिने प्रेमी फ्री में देख सकेंगे शानदार और जानदार फिल्में
रायपुर आर्ट लिट्रेचर एंड फिल्म फेस्टिवल का धमाकेदार आयोजन
डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग समेत फिल्म मेकिंग पर कार्यशाला
रायपुर. रायपुर आर्ट लिट्रेचर एंड फिल्म फेस्टिवल (RALFF) का आयोजन 8 फरवरी 2025 को रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया जा रहा है. इस महत्वपूर्ण आयोजन में पद्मश्री पंडी राम मंडावी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे.कार्यक्रम दोपहर ठीक एक बजे से प्रारंभ हो जाएगा. रायपुर आर्ट लिट्रेचर एंड फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर कुणाल शुक्ला और फेस्टिवल क्यूरेटर प्रीति उपाध्याय ने बताया छत्तीसगढ़ के सभी सिने प्रेमियों के लिए इंट्री पूरी तरह से फ्री है.
उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की कला और सिनेमा को नई दिशा प्रदान करना है. उन्होंने कहा कि फिल्म स्क्रीनिंग, डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शनी, परिचर्चा सत्र और कार्यशालाओं के साथ इस फेस्टिवल में दर्शकों को भारतीय भाषाओं की शॉर्ट फिल्मों और रचनात्मक चर्चाओं का आनंद लेने का भरपूर अवसर मिलेगा. शाम को अवार्ड सेरेमनी भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा.
यह है मुख्य आकर्षण
स्क्रीनिंग: फिल्म मंदराजी की स्क्रीनिंग, हिंदी शॉर्ट फिल्में: कदम, बंटू'स गैंग, बोटल, द स्ट्रीट एंजल, 04, बिटवीन वर्ल्ड्स, डॉक्यूमेंट्री: चिंताराम, जुनून और ज़माना, बहुभाषी शॉर्ट फिल्में: ब्यांव (राजस्थानी), प्रदक्षिणा (मराठी), एनाउंसमेंट - ए मार्टर स्टोरी (हिंदी), थुनाई (तमिल), हेल्प योरसेल्फ (अंग्रेजी/हिंदी), मन आसाई (तमिल), जमगहीन (छत्तीसगढ़ी), कमजखीला (अन्य), द फर्स्ट फिल्म (हिंदी).
परिचर्चा सत्र
पहले सत्र में "जिंदगी...कैसी है पहेली" विषय पर संजय अलंग, रवि वल्लुरी, अज़ीम उद्दीन, भगवत जायसवाल और दिव्यांश चर्चा करेंगे। वहीं दूसरे सत्र में "दिस क्राइंग अर्थ, दीज वीपिंग शोर्स (ट्रांसनेशनल इंडिजिनस डायलॉग)" पर सेसिलिया डियाज़, किरण भट, मीर अली मीर और मुकेश पांडे अपनी राय रखेंगे.
कार्यशाला
फिल्म निर्माण की अवधारणा पर डॉ. नरेंद्र त्रिपाठी, परफेक्ट योर मैन्युस्क्रिप्ट विषय पर लक्ष्मी वल्लुरी और इमोशन्स थ्रू एडिटिंग पर बिरजू कुमार रजक की क्लास होगी. कार्यक्रम से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इस मोबाइल नंबर 9926555050 पर संपर्क किया जा सकता है.
हमारे हिस्से का इरफ़ान
“अबे तरसते हैं लोग मुझसे acting सीखने के लिए, और तेरे पास टाइम नहीं है”
कुछ ऐसे ही शब्दों थे इरफान साहब के, जब बाबिल उन्हें ‘आज नहीं बाबा कल, कल पक्का’ कहके गच्चा दे रहा था।
बाबिल की परवरिश आम सेलेब्रिटी बच्चों से नहीं हुई थी। उसको इरफान साहब स्कूल नहीं भेजते थे। वो होम ट्यूशन पढ़ता था। वो नदी में तैरना सीखता था, वो पेड़ों पर चढ़ता-उतरता था। इनशॉर्ट, इरफान साहब के घर एक मोगली रहता था। इस मोगली को एक रोज़ एहसास हुआ कि उसके पिता क्या चीज़ हैं, क्या ग़जब फ़नकार हैं।
मोगली ने अपने बाबा से गुज़ारिश की कि वो actor बनना चाहता है।
इरफ़ान साहब ये सुना और कहा “धत्त तेरे की, बेटा जी, लग गए आपके”
इसके बाद बाबिल की ट्रैनिंग तो शुरु हुई, पर इरफ़ान साहब खुद दुनिया भर की फिल्मों में इतने मसरूफ़ रहने लगे कि घर में उनकी हाज़िरी घटती चली गई। छोटा बाबिल अपने जंगल का मोगली बना, कुछ समय तो उछल-कूद से दिल बहलाता रहा, पर एक उम्र बाद उसे भी संगी-साथियों की ज़रूरत महसूस होने लगी।
नतीजतन बाबिल लड़कपन की उम्र में पहुँचते ही मुंबई के टॉप स्कूल में एजुकेशन के साथ-साथ बढ़िया एसयूवी गाड़ी का भी मालिक बन गया। अब पासा घूम गया, इरफ़ान साहब उसके पीछे भागने लगे कि “अबे सुन ले, सीख ले, आ जा एक सीन है इसको ब्रेक करते हैं” पर बाबिल है तो लड़का ही, और लड़के जब हमउम्र लड़कों की दोस्ती और लड़कियों की संगत में आते हैं तो अनजाने में ही घर-परिवार को किनारे करने लगते हैं।
हालाँकि बाबिल आम बच्चों से ज़रा बेहतर है, इसलिए अचानक स्कूल में मिली पॉपुलरिटी से जल्द ही ऊबने लगा। पर तबतक वो मनहूस घड़ी आ चुकी थी, इरफ़ान साहब को बीमारियों के भेड़िये ने दबोच लिया था। इलाज चलता रहा, पहले घर पर, फिर अमेरिका में! इस दौरान बाबिल से जितना बन पड़ा, वो अपने बाबा के साथ ही रहा।
फिर कैंसर सुधरने लगा। घर वापसी हो गई। हालात उम्मीदज़दा लगने लगे पर आह-री किस्मत, पेट में एक इन्फेक्शन हो गया! डॉक्टर ने अंदाज़न कहा कि मैक्सिमम 3 दिन के लिए एडमिट कर दीजिए। हमें उम्मीद है कि उससे पहले ही हम घर वापस भेज देंगे।
इरफ़ान साहब घर से निकलने से पहले बोले “3 दिन में आता हूँ, फिर सिखाऊँगा तुझे, बस तीन दिन और इंतेज़ार कर...”
पर मगर अफ़सोस, इरफ़ान साहब लौटकर नहीं आए और अपना अर्बन मोगली, एक बार फिर अकेला रह गया।
CUT TO:
मैं रेलवे मैन से जुड़ा एक इंटरव्यू देख रहा था। चंद बातों के बाद ही बाबिल ने बड़ी मासूमियत से कहा कि “केके सर के सेट पर होने से, मुझे एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि बाबा नहीं हैं, मैं इनसे जो पूछता था, वो झट से बता देते थे”
इसके साथ ही बाबिल बोला “मेरी हिन्दी बहुत अच्छी नहीं है और मुझे इस बात पर शर्म आती है, मैं सीख रहा हूँ और बेहतर कर रहा हूँ”
इसके तुरंत बाद ही ऑडियंस में से किसी ने इरफ़ान साहब की एक फिल्म के बारे में कुछ कहा तो बाबिल बच्चों की तरह उछलकर अपना इक्साइट्मेंट दिखाने लगा।
एक बात गौर करिए कि हम उस दौर में हैं जहाँ दुनिया की, साथी कलाकारों की, यहाँ तक की अपने बाप तक की इज्ज़त भी फॉर्मैलिटी में की जा रही है क्योंकि इंडस्ट्री में ये सब कूल नहीं लगता है।
ऐसे माहौल के बीच, एक 25 साल का लड़का, बिना किसी फूँ-फाँ के, बॉय नेक्स्ट डोर सूरत वाला, जो दिल में है वही मुँह पर लाने में संकोच न करता, जिसकी मुस्कुराहट में इरफ़ान साहब झलक बसती हो, वो इंडस्ट्री में आता है और तुरंत सबका लाड़ला बन जाता है।
सबसे अच्छी बात ये है कि बाबिल acting करते वक़्त इरफ़ान खान बनने की कोशिश नहीं करता। पर फिर भी, हम सिनेमा दीवाने लोग, उसको देखकर अपने हिस्से का इरफ़ान खान जी लेते हैं।
#सहर
भूलन द मेज... अपनी शिकायत फाड़कर फेंकता हूं मैं
राजकुमार सोनी
संभावनाओं से भरे युवा फिल्मकार मनोज वर्मा की फिल्म भूलन द मेज अगर आपने नहीं देखी है तो पहली फुरसत में इसे देख लीजिए. यह फिल्म छत्तीसगढ़ में निर्मित होने वाली सुंदरानी और जैन मार्का फिल्मों से बेहद अलग और जानदार है. फिल्म में थोड़ी-बहुत खामियां भी है बावजूद इसके यह फिल्म अंत तक बांधकर रखती है और अपनी बात कहने में सफल रहती हैं.
यहां मैं बताना चाहूंगा कि मनोज वर्मा के फिल्मी कामकाज को लेकर मेरी धारणा अच्छी नहीं रही हैं. दरअसल उनकी पुरानी फिल्मों का नाम ही महूं दीवाना... तहूं दीवानी, मिस्टर टेटकूराम और लफाडू-फफाडू टाइप का रहा है तो मेरी क्या गलती है ? उन्हें लेकर जो कुछ भी फिल्मी प्रचार रहा है वह यहीं रहा है कि उनके भीतर सतीश जैन का भूत सवार हैं और वे उनके नक्शे-कदम पर चलकर अपनी अच्छी-खासी सृजनात्मकता का गला घोंट रहे हैं.
लेकिन भूलन द मेज ने मेरी इस धारणा को ध्वस्त कर दिया है. कई बार धारणाओं का धवस्त हो जाना अच्छा भी होता है.
मंगलवार को छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति प्रेमी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सौजन्य से मेरी धारणा टूट गई. वे भूलन द मेज देखने गए तो मीडिया के अन्य साथियों के साथ मेरा भी जाना हो गया. हालांकि निर्देशक मनोज वर्मा शायद जानते थे कि मैं उनकी पुरानी फिल्मों को लेकर अच्छी राय नहीं रखता हूं इसलिए उन्होंने मुझसे एक मर्तबा पूरी विनम्रता से कह भी रखा था कि आप भूलन द मेज को अवश्य देखिए...शायद आपकी शिकायत दूर हो जाए.
यह कहने में कोई गुरेज़ नहीं है कि भूलन द मेज को देखकर मेरी धारणा चकनाचूर हो गई हैं. मेरी शिकायत दूर हो गई हैं. मैं अपनी शिकायत को अपने जेब में वापस रखता हूं.
जेब में भी क्यों ? शिकायत को सीधे-सीधे फाड़कर फेंकता हूं.
मनोज वर्मा ने अंचल के बेहतरीन लेखक संजीव बख्शी की लिखी हुई शानदार सी कहानी पर शानदार और जानदार फिल्म बनाई है. यहां कहानी का जिक्र करना ठीक नहीं होगा क्योंकि इस बारे में सोशल मीडिया व प्रचार के अन्य माध्यमों पर काफी कुछ लिखा जा चुका है. बस...इतना बताना चाहूंगा कि यह फिल्म हमारी प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था पर जबरदस्त चोट करती है. फिल्म को देखते हुए आप हंसते हैं. रोते हैं और मन ही मन अपने अराध्य या ईश्वर से यह प्रार्थना करने लग जाते हैं कि ' हे...ईश्वर...किसी भी भोले-भाले... सीधे-सादे इंसान को कोर्ट-कचहरी के दिन देखने के लिए मजबूर मत करना. हे परमपिता... परमेश्वर...आप जहां कहीं भी हो...आप यह सब देखो कि इस धरती के गांवों में...छोटे कस्बों में अपनी छोटी-छोटी खुशियों के साथ जीने वाले लोग भी रहते हैं. कौन हैं वे लोग जो उनकी खुशियों में खलल डालते हैं. कानून किसके लिए बनता है ? अगर बनता भी है तो उसकी शुद्धता को खत्म करने वाले लोग कौन हैं ? कानून थोपा क्यों जाता है ?
फिल्म का एक पात्र भकला और उसकी पत्नी प्रेमिन बाई अपने गांव के एक साथी को जेल से छुड़ाने के लिए शहर आते हैं. बाबुओं की वजह से काम नहीं बनता तो उन्हें फुटपाथ पर रात गुजारनी पड़ती हैं. दोनों आकाश की तरफ देखते हैं. आधा-अधूरा चांद तो नज़र आता है मगर तारा नहीं आता. दोनों के बीच संवाद में एक बात सामने आती हैं- शायद शहर में आने के बाद तारा नज़र नहीं आता है. यह संवाद भीतर तक हिला देता है. सच तो यह है कि शहर में इधर-उधर भटकते हुए लोग तो दिखते हैं लेकिन मददगार नज़र नहीं आते.फिल्म में जब गांव के सारे लोग जेल की सज़ा भुगतने को तैयार हो जाते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं. अपने साथी को बचाने के लिए जब सारे गांव वाले जज को पैसा देने के लिए अपनी मेहनत की कमाई को एक गमछे में एक इकट्ठा करते हैं तो आंसू बह निकलते हैं. मैंने मुंबइया फिल्मों में कोर्ट के भीतर और बाहर गुंडे- माफियाओं के द्वारा गोली चलाने के सैकड़ों दृश्य देखें हैं, लेकिन कोर्ट के भीतर न्यायाधीश की कुर्सी के आसपास ग्रामीणों का सामूहिकता के साथ नाचना-गाना पहली बार देखा है. गाने के पहले एक बच्चा न्याय की मूर्ति की आंखों में बंधी हुई पट्टी उतारता है तो कई सवाल और जवाब खुद से टकराने लगते हैं. कोर्ट परिसर में गांव वालों के द्वारा भोजन पकाने और वहीं परिसर में ही ठहरकर जज का फैसला सुनने के लिए ग्रामीणों की बेचैनी को देखना आंखों को खारे पानी के समन्दर में बदल डालता है.
मनोज वर्मा ने फिल्म के एक-एक फ्रेम पर खूबसूरत काम किया है. फिल्म का एक-एक गीत और उसका संगीत जानदार है. बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाले मोंटी शर्मा से भी उन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि के मद्देनजर शानदार काम लिया है. नंदा जाही रे... जैसा गीत सैकड़ों बार सुना गया है, लेकिन मनोज और प्रवीण की आवाज में इसे फिल्म में सुनना अलग तरह के अनुभव से गुजरने के लिए बाध्य कर देता है.
वर्ष 2000 में जब से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है तब से अपसंस्कृति फैलाने वालों की बाढ़ आई हुई है. सतीश जैन की फिल्म मोर छइंया-भुइंया के संयोगवश हिट हो जाने के बाद से जिसे देखो वहीं डेविड धवन बनकर कचरा परोसने के खेल में लग गया था. हालांकि यह सिलसिला अभी भी थमा नहीं है. यह सब कुछ कब जाकर खत्म होगा और कहां जाकर खत्म होगा कहना मुश्किल है.
मनोज वर्मा अपनी इस फिल्म के जरिए धारा को मोड़ते हुए दिखते हैं. वे हमें यह आश्वस्त करते हैं कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है.वे सभी दर्शक जो सुंदरानी और जैन मार्का फिल्मों में कला-संस्कृति के नाम पर नकली पहनावा, नकली नाक-नक्श, नकली गांव-घर, नकली बोली-बानी और लोक धुनों में मिलावट को देख और सुनकर परेशान हो चुके हैं उन्हें असली मेला मंडई, स्थानीयता की रंगत, लोक के रंग, सुआ, नाचा गीत और शोक में बजने वाले बांस की धुन को शिद्दत से महसूस करने के लिए भूलन द मेज देख लेनी चाहिए. महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया को भारतीय सिनेमा की आत्मा कहा जाता है. भूलन द मेज भी हमारी उस आत्मा से मुलाकात करवाती है जिसे हमने बिसरा दिया है.
मनोज वर्मा को लेकर मेरी उम्मीद और अधिक बढ़ गई हैं. मैं उनसे सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के गांव-देहात और जंगलों में सैकड़ों-हजारों कहानियां बिखरी हुई हैं. जरूरत है उन कहानियों में से कुछ चुनिंदा कहानियों को समेटने की. जब सत्यजीत रे यहां छत्तीसगढ़ आकर प्रेमचंद की कहानी पर सदगति जैसे फिल्म बना सकते हैं. जब राजकुमार राव की फिल्म न्यूटन की शूटिंग छत्तीसगढ़ में हो सकती हैं और आस्कर में जा सकती हैं तो फिर यहां के निर्माता निर्देशक चल हट कोनो देख लिही और हंस झन पगली फंस जाबे से ऊपर क्यों नहीं उठ सकते हैं ?
यह सही है कि व्यवसायिकता भी फिल्म का एक जरूरी पार्ट है, लेकिन क्या सिनेमा के इतिहास में किसी भी तरह का कोई रेखांकन सिर्फ पैसे और पैसों के दम पर ही किया जाना ठीक होगा ? या किया जा सकता है ?
स्मरण रहे कि आपकी अपनी मौलिकता ही आपको स्थापित करती है और पहचान दिलाती है. भूलन द मेज में काम करने वाले मास्टर जी यानि अशोक मिश्र को कौन नहीं जानता. उन्होंने भी एक से बढ़कर एक फिल्में लिखी है. वे स्थापित हैं और लोग उन्हें अलग तरह की लकीर खींचकर काम करने वाला लेखक मानते हैं. लोग अगर आज राजमौली की फिल्मों के दीवाने हैं तो उसके पीछे भी भेड़चाल नहीं है.
मनोज वर्मा को मैं निकट भविष्य में भेड़चाल से बचने की सलाह दूंगा. ( यह आवश्यक नहीं है कि मेरी सलाह मानी जाय )
एक बात और मनोज वर्मा चुस्त-दुरुस्त कहानी और पटकथा के बावजूद कुछ कलाकारों से ही बेहतर काम ले पाए है. पूरी फिल्म में ओंकार दास मानिकपुरी, अशोक मिश्र, राजेन्द्र गुप्ता, मुकेश तिवारी, आशीष शेंद्रे, भकला की पत्नी प्रेमिन बाई यानी अणिमा पगारे, कोटवार बने संजय महानंद, मुखिया की पत्नी गौंटनिन अनुराधा दुबे और सुरेश गोंडाले का अभिनय ही याद रह जाता है. फिल्म में कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर लगा कि मनोज वर्मा ने संबंधों के चलते उनके लिए गुंजाइश निकाली है. जब कोई काम बड़ा हो और लगे कि पूरी ताकत झोंकने से ही असर पैदा होगा तो गुंजाइश निकालने और गुंजाइश निकालने के लिए मजबूर कर देने वाले लोगों से बचा जाना चाहिए.
यार...उसको बुरा लग जाएगा... यार... वो क्या सोचेगा...यार उसको रख लेने से अपना काम बन जाएगा जैसी स्थिति फिल्म में ब्रेकर का काम करती है.
सच कह रहा हूं मैं
ह...हह...हव....हव
एकदम सच..... हव....हव....हहहहव
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी को लेकर पत्रकार रवीश कुमार की मजेदार पोस्ट
आरआरआर ने किया कश्मीर फाइल्स का डब्बा गुल तो बिलबिला उठे भक्त
इस वक्त देश में चारों तरफ एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर की चर्चा हो रही है. जिसे देखो वह RRR की ही बात कर रहा है. फिल्म में कलाकारों की मेहनत और अभिनय पर बात हो रही हैं तो तकनीक और निर्देशन को लेकर भी लोग कहना और सुनना पंसद कर रहे हैं. सच तो यह हैं कि फिल्म के एक-एक फ्रेम और एक-एक दृश्य पर लोग बात कर रहे हैं और खुद को समृद्ध कर रहे हैं.
किसी फिल्म को लेकर ऐसी दीवानगी हैरत में डालती है. साठ-सत्तर और अस्सी के दशक में जब फिल्मों का जबरदस्त क्रेज हुआ करता था तब इस तरह की बातचीत देखने-सुनने को मिलती थीं. तब लोग पहले दिन पहला शो देखकर आते थे और पुल-पुलियों पर बैठकर सनीमा की स्टोरी सुनाया करते थे. अब तो सार्वजनिक पुलियाएं बची नहीं सो चाय की गुमटियों, दफ्तरों, कॉफी हाउस और मोबाइल के जरिए फिल्म की विशेषताओं का बखान हो रहा है.
लोग स्वस्फूर्त ढंग से सिनेमा हॉल जा रहे हैं. मॉल जा रहे हैं. लाइन में खड़े होकर टिकट ले रहे हैं या ऑनलाइन टिकट बुक करवा रहे हैं. पिक्चर देखकर तालियां बजा रहे हैं. सीटियां बजा रहे हैं.
केंद्र की मोदी सरकार के चलते लोग-बाग एक लंबे अरसे से गाल ही बजा रहे थे. गाल बजाने वाले लोगों को अपना गम भूलकर सीटी बजाते हुए देखना सुखद लग रहा है. हालांकि पायजामा कुर्ता पहनकर शास्त्रीय संगीत सुनने वाले संभ्रांत किस्म के दर्शकों को सीटियां परेशान कर सकती हैं, लेकिन संभ्रांत दर्शकों को पता भी नहीं होगा कि उनके संतानें इस्ट्राग्राम पर रोजाना आंख दबा रही है और वक्त-बेवक्त सीटियां बजा रही है. खैर...कई बार सामूहिक सीटियां आनंद से भर देने वाले कोरस का काम करती हैं... इसलिए बरसों बाद सिनेमा हॉल में लौटी हुई इन सीटियों का स्वागत किया जाना चाहिए.सीटियों का सम्मान होना चाहिए. इन सीटियों के सम्मान में हमें भी एक जोरदार सीटी बजा ही लेनी चाहिए.
हमें यह सीटी इसलिए भी बजानी चाहिए क्योंकि आरआरआर ने सहमति और असहमति के बीच झूलते हुए देश के सीधे-साधे आमजन को नफरत की आग में झुलसने से बचा लिया है. इस फिल्म ने लोगों को नफरत के विषाक्त किटाणुओं से भरी हुई फिल्म कश्मीर फाइल्स से थोड़े समय के लिए ही सही मगर मुक्ति दिलवा दी हैं. ऐसा महसूस हो रहा है कि नफरती चिन्टुओं के द्वारा पैदा किए गए बेमतलब के शोर पिंड छूट गया है.
अब कश्मीर फाइल्स बड़े से बड़े शहर में एकाध शो में चल रही है. ( उज्जड़ प्रदेश का नहीं बता सकता ) यह फिल्म जहां कहीं भी चल रही हैं वहां पहले की तरह इसे वहीं लोग देखने जा रहे हैं जो सदियों से बोरिया-बिस्तर और चना-सत्तू बांधकर हिन्दुओं को जागृत करने के गोरखधंधे में लगे हुए थे.
बहरहाल आरआरआर ने कश्मीर फाइल्स का डब्बा गुल कर दिया है तो भक्त बुरी तरह से फड़फड़ा उठे हैं. उन्हें लग रहा कि साला... ये क्या हो गया ? अच्छी-खासी नफरत की खेती चल रही थीं. दो सौ करोड़ कमाने वाली फिल्म ने सौ करोड़ हिन्दुओं को जगाने का काम प्रारंभ कर दिया था. चारों तरफ बामन-बामन-पंड़ित-पंड़ित हो रहा था... लेकिन अचानक सारा किया धरा फेल हो गया ?
ये घनचक्कर बाहुबली वाले को भी अभी ही फिल्म रीलिज करनी थीं ? हॉल बुक करके लोगों को फ्री में फिल्म दिखाकर जनसेवा करने का मौका मिल रहा था. हॉल में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे जैसी प्रार्थना गाने और भगवा गमछा धारण करके सेल्फी लेने का आनंद ही कुछ और था लेकिन सब चौपट हो गया. भैय्या जी के कहने पर मोटर साइकिल में पेट्रोल डलवाते थे. जय-जय श्रीराम का नारा लगाते हुए रैली निकालते थे. ढोल बजाते थे. फिल्म देखने जाते थे. इंटरवेल में समोसा खाते थे... सब खत्म हो गया है.
अब आरआरआर आ गई तो लोग आदिवासी नायकों की बात करने लगे हैं. लोग झूठी कहानी के जरिए खड़े किए गए किसी भी एजेंडे का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है. ऐसा कैसे चलेगा ? नफरत का धंधा तो चौपट हो जाएगा ?
दर्शकों की अब सारी दिलचस्पी दूसरी तरफ टर्न हो गई है. वे आंध्र प्रदेश के सीतारामा राजू और तेलंगाना के कुमारम भीम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं. इन जगहों के आदिवासी अपने इन दोनों नायकों को भगवान की तरह पूजते हैं. कहा जाता है कि अल्लूरी ने मनयम इलाके के आदिवासियों को जल-जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए एकजुट किया जिससे अंग्रेजों में खौफ पसर गया था वहीं कुमारम भीम ने गोंड आदिवासियों के अधिकारों के लिए निजाम से टक्कर ली थीं. बताते हैं कि दोनों आदिवासी नायक अपने-अपने इलाके में आदिवासियों के अधिकारों के लिए काम कर रहे थे. दोनों व्यक्तिगत जीवन में कभी भी एक-दूसरे से नहीं मिले. फिल्मकार राजामौली ने दोनों नायकों को अपनी फिल्म में एक साथ मिलाया और अपनी शानदार कल्पनाशीलता से यह बताया कि जब दो क्रांतिकारी एक साथ मिल जाते हैं तो कैसा धमाल मचा सकते हैं ?
यहीं एक वजह से फिल्म में रामायण के राम का जिक्र होता है. सीता का जिक्र होता है और महाभारत के भीम की उपस्थिति भी देखने को मिल जाती है. राम और भीम के साथ-साथ गाड़ियों के पंचर बनाने वाले अख्तर की भी बात होती है. ( भीम अपनी पहचान छिपाने के लिए कुछ समय तक अख्तर बने रहता है ) इस फिल्म में कई महत्वपूर्ण दृश्य है. एक महत्वपूर्ण दृश्य यह भी है कि राम और भीम ( अख्तर ) एक मुसलमान के घर पर बड़ी सी थाली में भोजन करते हैं. एक गाने में राम अपने कंधों पर भीम को घुमाता है तो संकट के एक दृश्य में भीम... राम को कांधे पर लेकर चलता है.
भक्त यह सब देखकर परेशान चल रहे हैं. वे यह सोच नहीं पा रहे हैं कि यह सब कैसे हो रहा है. और क्यों हो रहा है ? जिस टोपी और पंचर बनाने वाले से नफरत करते हैं उसके मारधाड़ से भरे एक्शन पर जनता ताली क्यों बजा रही है. ? जबकि थाली और ताली तो तब बजानी होती है जब मोदी जी का आदेश होता है.
मौली का भीम अंग्रेजों से लड़ता है और मौली का राम भी अंग्रेजों पर बाण चलाता है... लेकिन फिल्म को देखकर लौटे एक भक्त का कहना था कि प्रभु राम जी को कहीं और मतलब टुकड़े-टुकड़े गैंग पर बाण चलाना था. अंग्रेज राक्षस नहीं थे. ( जब भक्त के पूर्वजों ने कभी अंग्रेजों से युद्ध नहीं किया तो भक्त को कैसे पता चलेगा कि अंग्रेज राक्षस थे या नहीं ?)
बहरहाल आरआरआर की जोरदार सफलता ने भक्तों को परेशान कर दिया है. वे अब फिल्म को लेकर दुष्प्रचार में जुट गए हैं. एक बार फिर बरसों से सोए हुए हिन्दुओं को जगाने वाली फिल्म यानि कश्मीर फाइल्स का प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया व गोदी मीडिया में तेज कर दिया गया है. अपनी गैरत को बेचने के लिए मशहूर अखबार की वेबसाइट में खबर चल रही है कि आरआरआर के कलेक्शन में गिरावट आ रही है जबकि कश्मीर फाइल्स की जवानी बरकरार है वह अंगडाई लेते हुए उठ खड़ी हुई है. खबर है कि आरआरआर के दुष्प्रचार के लिए आईटीसेल की टीम भी सक्रिय हो गई है.
चाहे कितनी भी टीम सक्रिय हो जाए... आरआरआर इसलिए चलेगी क्योंकि इस फिल्म में भाजपा और संघ का थोथा राष्ट्रवाद मौजूद नहीं है. फिल्म के राम में धैर्य है. ऊर्जा है. संतुलन है तो भीम में बेशुमार ताकत के बावजूद संवेदनशीलता है. फिल्म में जल-जंगल और जमीन के लिए लड़ने वाले नायकों और उनका साथ देने वाली जनता का गुणगान है. यह फिल्म अपने दर्शक को उन्माद नहीं बल्कि उर्जा से भर देती है.
मुझे यह फिल्म बेहद अच्छी लगी हैं इसलिए इसकी कुछ टूटी-फूटी समीक्षा दोबारा लिख रहा हूं. यह फिल्म अभी एक बार टू डी में देखी है. दोबारा फिर देखूंगा और थ्रीडी में देखूंगा.
राजकुमार सोनी
9826895207
फिज़ा में घोल दिया गया था नफरत का जहर... अगर आप दोस्ती...भाई-चारे और मोहब्बत के झोंके से गुजरना चाहते हैं तो जाकर देख आइए राजामौली की फिल्म आरआरआर
राजामौली की फिल्म आरआरआर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है. इस फिल्म ने अपने प्रदर्शन के पहले ही दिन में वह कमाई कर ली जिसे छू पाना किसी भी दूसरी फिल्म के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है. मीडिया की खबरों पर भरोसा करें तो फिल्म ने पहले ही दिन में पांच सौ करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया है. सत्तर और अस्सी के दशक में लोगों के भीतर फिल्मों को लेकर जो क्रेज देखने को मिलता था कमोबेश वहीं क्रेज इस फिल्म को लेकर भी देखने को मिल रहा हैं. यह फिल्म सिंगल थियेटर और मॉल में जहां- जहां भी लगी हैं वहां नौ बजे सुबह का पहला शो भी हाउसफुल जा रहा है और रात का आखिरी शो भी. लोग रात को तीन बजे भी फिल्म देखकर अपने घर लौट रहे हैं.
आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में जिसके चलते थियेटर में भारी भीड़ उमड़ रही हैं. दरअसल यह फिल्म साधारण सी कहानी पर बनी आसाधारण फिल्म हैं. यह फिल्म तकनीक की दृष्टि से समृद्ध तो हैं ही...यह हिन्दुस्तान के भविष्य का सिनेमा भी हैं.
इस फिल्म की सबसे खास बात यह हैं कि इसमें कश्मीर फाइल्स की तरह एक कौम विशेष के लिए नफरत नहीं परोसी गई हैं. इस फिल्म में हिन्दू चेहरे हैं तो सिक्ख, मुसलमान और दलित का चेहरा भी दिखाई देता है. इस फिल्म का एक पात्र राम है तो दूसरा महाभारत का भीम हैं. यहीं भीम अख्तर बनकर एक मुसलमान परिवार के यहां शरण लेता हैं और वह परिवार उसके क्रांतिकारी मसूंबों को पूरा करने में सहयोग करता है. फिल्म का एक नायक राम जब अंत में राम बनकर अंग्रेजों पर बाण चलाता है तो दर्शक भौचक होकर देखते रह जाता है. दर्शक के भीतर से आवाज़ आती हैं- इस देश में भी एक न एक रोज चमत्कार होगा. कोई न कोई राम बनकर लौटेंगा और देश को बरबाद करने वाले काले अंग्रेजों को अपने नुकीले बाणों से भेद डालेगा.
राजामौली एक ऐसे फिल्मकार हैं जिनके पास देश के इतिहास, भूगोल, पुरातत्व, धर्म और संस्कृति को समझने की एक अलग दृष्टि विद्यमान हैं. अपनी इसी दृष्टि के चलते वे अपनी हर फिल्म में कला का ऐसा तड़का लगाते हैं कि दर्शक वाह-वाह करने लगता है. अपनी इस फिल्म में उन्होंने ब्रिटिशकाल के दो स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम की युवा दिनों की कहानी को अपनी रचनात्मकता से जानदार और शानदार बना दिया है. कैनवास पर नए ब्रश के साथ उन्होंने जो कुछ भी चित्रित किया है उसमें वीरता, ऊर्जा और धैर्य का विराट स्वरूप देखने को मिलता है. वे पहले भी अपनी कई फिल्मों में असंभव से लगने वाले दृश्यों को संभव बना चुके हैं इसलिए उनका हर पात्र अविश्वसनीय होते हुए विश्वसनीय लगने लगता है. इस फिल्म में भी उन्होंने असंभव से दिखने वाले कई दृश्य को अपनी कल्पनाशीलता से संभव बना दिया है. निर्देशक ने एक-एक फ्रेम पर काम किया है. क्या लाइट... क्या बैकग्राउंड म्यूजिक, क्या वेशभूषा और क्या लोकेशन. कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो मजबूत नहीं हैं. एक-एक फ्रेम पर मेहनत दिखाई देती है.
फिल्म आरआरआर में ऐसे कई दृश्य मौजूद हैं जिसके चलते आप दांतों तले ऊंगली दबा लेते हैं. फिल्म में शेर हैं. अंग्रेज हैं.तीर है.भाला है. गोला-बारूद है तो बंदूक भी हैं. फिल्म में बघ्घी भी हैं तो अंग्रेजों के जमाने में चलने वाली मोटरसाइकिल भी है. क्रांति की मशाल और आग के जोरदार दृश्यों के साथ जबरदस्त घुड़सवारी भी है. प्यार, मोहब्बत, दोस्ती और भाई-चारे का संदेश तो हैं ही.
इस फिल्म को देखने के लिए किसी भी भक्त को चौक-चौराहे पर पोस्टर चिपकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. इस फिल्म के लिए किसी भी उन्मादी को हॉल बुक करके फ्री में टिकट बांटने की भी जरूरत नहीं है. फिल्म को हर वर्ग का दर्शक स्वस्फूर्त ढंग से थियेटर जाकर देख रहा है. हॉल में सीटियां बज रही हैं. लोग-बाग सीट से खड़े होकर जोरदार तालियां बजा रहे हैं. फिल्म को देखने के दौरान हर दर्शक अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर रहा है. किसी को भी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे जैसी प्रार्थना गाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और ना ही जोर-जोर से जय-जय श्री राम का नारा लगाने की. उन्मादी भक्तों और तथाकथित राष्ट्रवादियों के लिए यह बुरी खबर है कि आरआरआर ने महज एक दिन में ही कश्मीर फाइल्स का डिब्बा गुल कर दिया है. आरआरआर को मिल रही बेतहाशा कामयाबी के बाद नफरती चिंटू कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स के बजट और आरआरआर के बजट में बहुत फर्क हैं. ऐसे चिन्टुओं के लिए एक ही जवाब है कि फिल्म शोले के समय प्रदर्शित हुई जय संतोषी मां भी दस-बीस लाख में बनी थीं. इस फिल्म ने भी कमाई का रिकार्ड तोड़ डाला था. कश्मीर फाइल्स ने भले ही बिजनेस कर लिया है, लेकिन देर-सबेर यह फिल्म इतिहास के कूड़ेदान में ही फेंकी जाने वाली है.
यह देश सबका है. इसलिए सबके लिए फिल्म बनाई जानी चाहिए. यदि किसी एक वर्ग के लिए भी फिल्म बनती हैं तो कम से कम उस फिल्म से नफरत और शत्रुता को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए. सच तो यह है कि नफरती चिन्टुओं के लिए फिल्म बनाकर खुद को देश का महान फिल्मकार समझने वाले अग्निहोत्री को भी आरआरआर जैसी फिल्म बनाने के लिए सात जन्म लेने पड़ेंगे. वे जितनी बार भी जन्म लेंगे उतनी बार उनकी खराब नीयत उन्हें कामयाब होने से रोक देगी.
जो लोग भी सिनेमा और कला से मोहब्बत करते हैं उन्हें राजामौली की आरआरआर जल्द से जल्द देख लेनी चाहिए. क्योंकि यह फिल्म ऐसी हैं कि जो कोई भी देख रहा है वह इसकी कहानी सुनाने लगता है. दृश्यों की भव्यता और उसके फिल्मांकन के बारे में बात करने लगता है. इस फिल्म को देखकर जो भी दर्शक बाहर निकल रहा है वह कह रहा है- यार...काम हो तो ऐसा.भई वाह... क्या बात है.
राजकुमार सोनी
9826895207
पुष्पा का नायक अपनी दाढ़ी से तिनके निकाल-निकालकर अलाव सुलगा रहा है ?
टीवी पर मोदी का झूठ देखने और सुनने से अच्छा है कि पुष्पा ही देख लो
पुष्पा पूरी तरह से एक मनोरंजक फिल्म है. यह फिल्म उन आत्ममुग्ध लोगों के लिए नहीं बनी जो हर दूसरे दिन फेसबुक पर यह बताते रहते हैं कि अमुक जगह से उनकी किताब छपकर आ गई है. यह फिल्म फेसबुक पर लाइव कविता-कहानी और विमर्श ठेलने वालों के लिए भी नहीं बनाई गई है. साठ और सत्तर के दशक के चूके हुए कारतूसों को इस फिल्म में सब कुछ बकवास नजर आएगा. जॉय मुखर्जी, अनिल धवन, धीरज कुमार और सुजीत कुमार जैसी जीवन शैली रखने वालों को भी यह फिल्म पसंद नहीं आने वाली हैं.
यह फिल्म उन लोगों के लिए बनी है जो टीवी पर मोदी का झूठ सुनकर और देखकर परेशान हो चुके हैं या परेशान चल रहे हैं. पूरी फिल्म आपको पूरे तीन घंटे तक एक अकल्पनीय और अविश्वसनीय दुनिया की सैर कराती है. फिल्म को देखते हुए आप अमिश देवगन, दीपक चरसिया अंजना ओम, सुधीर तिहाड़ी, नफरती चिंटू अर्णब गोस्वामी और रजत शर्मा के झूठ से भी थोड़े समय के लिए ही सही मगर मुक्ति पा सकते हैं. आदर्श और नैतिकता को खूंटी पर टांगकर सबसे ज्यादा आदर्श और नैतिकता पर ही प्रवचन देने वालों को भी यह फिल्म घनघोर ढंग से निराश कर सकती है. राजनीति, समाज और दीन-दुनिया से दूर गंभीर किस्म के लेखकों, बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों को इस फिल्म को देखने से बचना चाहिए. इस फिल्म में उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके भीतरी तत्वों को सामान्य करने में झंडू पंचारिष्ट की तरह काम करता हो. इस चेतावनी के बावजूद जो लोग फिल्म देखने के इच्छुक हैं उनके बारे में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि वे समय से पहले बूढ़े नहीं हुए हैं.
जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है. अब प्रकाश मेहरा वाली जंजीर का जमाना नहीं है. नई पीढ़ी के भीतर गुस्सा तो है, लेकिन वह 77 एमएम के पर्दे पर लात चलाकर अपने गुस्से को जाहिर नहीं करना चाहता. इस पीढ़ी के सामने झूठ-फरेब और चालाकी की जो दुनिया खड़ी कर दी गई हैं वह उस दुनिया से उसी चालाकी और फरेब से निपटना चाहता है. पुष्पा का किरदार जो अल्लू अर्जुन ने निभाया है वह किरदार तमाम तरह के गलत कामों के बावजूद अपनी मां और अपनी प्रेमिका का सम्मान करता है. इस किरदार को स्त्री जाति से नफरत नहीं है. यह किरदार औरतों को छिनाल नहीं बोलता और रात को अपनी प्रेमिका को ( केवल उसे ही भाव देने वाली ) लेखिका समझकर फोन भी नहीं करता है. यह किरदार दबंग है. स्टाइलिश है मगर प्यार का भूखा है. फिल्म में सस्ती सी लॉरी है. पुराने ट्रक है. हिरोइन की सस्ती सी मोपेड़ है. हीरो के कपड़े गंदे हैं. वह स्लीपर पहनता है. बीड़ी पीता है. जुबान भी शुद्ध और साफ नहीं है, लेकिन उच्च, मध्य और सामान्य वर्ग का दर्शक पुष्पा की हरकत को पसंद कर रहा है.
पुष्पराज उर्फ पुष्पा जैसा किरदार हजारों बार फिल्मों में दोहराया जा चुका है. पुष्पा एक नामी बाप की अवैध संतान है. वह बिना बाप के नाम के बड़ा होता है. पैसा कमाना चाहता है तो रिस्क लेता है. वह दीवार फिल्म के अभिताभ बच्चन की तरह मामूली मजदूर है, लेकिन लाल चंदन की तस्करी करने वालों के बीच मे रहकर काम करता है और उन्हें झटके पर झटके देता है. अपने रास्ते में आने वाले तमाम खलनायकों को वह अपने हथकंडों से धाराशाही करता है. फिल्म में मारधाड़, खून-खराबा, एक्शन, डॉयलागबाजी और आयटम नंबर सब कुछ जबरदस्त है. फिल्म का हीरो अल्लू-अर्जुन बहुत ही चालाक है. दमदार है. बातों को बाजीगर है और लुंगी में भी डैशिंग लगता है.
पिछले कुछ समय से दक्षिण भारतीय फिल्मों ने सब तरफ कब्जा जमा लिया है. इन फिल्मों की सबसे खास बात यह है कि वह मास एंटरटेनिंग है. इसके अलावा साउथ का सिनेमा गंभीर विषयों को भी दमदार तरीके से उठा रहा है. हाल ही में रीलिज हुई जय भीम इतनी ज्यादा चर्चित हुई कि उसे हर वर्ग ने देखा. एक्टर फाजिल फहाद की फिल्म मलिक की भी सब जगह तारीफ हुई. यदि आप कभी यूपी-बिहार, झारखंड, बंगाल, ओड़िशा जाय तो सैलून की दुकान, भोजनालय अथवा किराने की दुकानों पर टीवी चलते हुए पाएंगे. यहां साउथ की फिल्में आपको गरदा उड़ाते हुए मिल जाएगी. हिंदी फिल्मों के मुकाबले साउथ की फिल्मों का सबजेक्ट एक बड़े वर्ग के द्वारा इसलिए भी पंसद किया जा रहा है क्योंकि इन फिल्मों में एक्शन, ड्रामा होता है. कहानी गांव से प्रारंभ होती है और फिर शहर पहुंचती है. फिल्म में गांव भी दिखता है और शहर भी. जबकि हिंदी फिल्मों से गांव गायब हो गया है. तकनीक और पटकथा के स्तर पर भी साउथ का सिनेमा मजबूत दिखाई देता है. जो बुद्धिजीवी पुष्पा को देखकर अपनी बौद्धिकता बघार रहे हैं उन्हें शायद यह नहीं पता होगा कि अब हिंदी का आधे से ज्यादा सिनेमा साउथ की स्क्रिप्ट पर जाकर टिक गया है. एक जमाने में जितेंद्र, मिथुन और अभिताभ बच्चन जैसे स्टार दक्षिण भारतीय फिल्मों की डब फिल्मों में काम कर रहे थे तो अब हिंदी सिनेमा के अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, आमिर खान जैसे बूढ़े एक्टर जोर आजमाइश कर रहे हैं. हिंदी सिनेमा का कोई भी एक्टर एक या दो फ्लाप फिल्म के बाद दर्शकों की नजर से उतर जाता है. हिंदी सिनेमा के बूढ़े हीरो का तिलस्म टूट भी रहा है, लेकिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है. वहां एक्टर आपको चौकाने के लिए तैयार रहता है. बूढ़े तो रजनीकांत भी हो चुके हैं , लेकिन जब भी उनकी कोई मूवी रीलिज होती है वह रिकार्ड बना डालती है. साउथ में हर कलाकार की अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. हिंदी बेल्ट में भी लोग प्रभाष, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, विजय देवरकोंडा को पहचानने लगे हैं.
बहरहाल पुष्पा ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और इसके ताबड़तोड़ मीम भी बन रहे हैं. जब जनता किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाती है तो फिर उसे मजा आने लगता है. हमको यह तो सोचना ही होगा कि पुष्पा ने हमारे भीतर के किस खालीपन को भरने का काम किया है. लोग कोरोना नाम की बीमारी से परेशान है. रोजी-रोटी के छिन जाने से परेशान है. राजनेताओं के झूठ और फरेब से परेशान है. कुछ तो ऐसा मिले जो परेशानी को कम करें. पुष्पा का एक गीत ही पूरी फिल्म का सार है- पत्तियों को खाती है किरणें / पत्तियों को खाता है बकरा / बकरे को शेर दबोचे / भूख से कोई न बचे. अभी चंद रोज पहले एक नेताजी ने एक अफसर को डांट दिया. अफसर ने भी दाढ़ी खुजाते हुए कहा- चाहे जो कुछ कर लीजिए...पुष्पराज झुकने वाला है. मैं झुकूंगा नहीं...अफसर..... तेरी झलक-अशर्फी...श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी गाते हुए निकल गया.
राजकुमार सोनी
9826895207
शैलेंद्र को कविराज पुष्किन कहते थे राजकपूर
मनोहर महाजन
14 दिसबंर, 1966...मेरा नाम जोकर की शूटिंग चल रही थी.सेट पर सभी लोग राज कपूर के जन्मदिन जश्न मना रहे थे. जश्न के शोर-शराबे के बीच कई बार फ़ोन बज चुका था. इस फ़ोन को लगातार कर रहे थे महान गायक मुकेश.आखिरकार फ़ोन उठाया गया और उन्होंने राज कपूर बताया कि उनके जिगरी दोस्त शैलेंद्र नहीं रहे.43 वर्ष की यंग ऐज में दुनिया को अलविदा कह देने वाले शैलेंद्र की अचानक मौत से राज कपूर को हिला कर रख दिया.
फ़िल्मी दुनिया में हम अक़सर मनमुटावों और सेलेब्स के प्रतियोगी स्वभाव और काम निकलवाने वाली दोस्ती की कहानियां ही सुनते हैं. लेकिन फ़िल्मी दुनिया में कई ऐसी जोड़ियां भी हुई हैं,जिनका याराना आम लोगों के लिए एक मिसाल है. कुछ ऐसा ही दोस्ताना था एक्टर,डायरेक्टर प्रोड्यूसर राज कपूर और गीतकार शैलेंद्र का था. दोनों के बीच दोस्ती के अलावा एक कलात्मक डोर थी,जिसने अनेकानेक क्लासिक और लोकप्रिय कृतियों को जन्म दिया. शैलेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत indian People s Theatre Association (IPTA) में लिखने से की. IPTA के ही एक समारोह में शैलेंद्र, राज कपूर से मिले. राज कपूर ने शैलेंद्र की मशहूर कविता जलता है पंजाब को सुना.विभाजन पर लिखी गई ये कविता राज कपूर के दिल को छू गई थी. राज कपूर ने शैलेंद्र को अपनी डेब्यू फिल्म आग (1948) के गाने लिखने का ऑफ़र दिया.शैलेंद्र उस वक़्त भारतीय रेल में काम करते थे और उन्होंने राज कपूर का ऑफ़र ठुकरा दिया. फिर वो समय भी आया जब राज कपूर बरसात के प्रोडक्शन में व्यस्त थे तब शैलेंद्र आर्थिक संकट से जूझ रहे शैलेन्द्र को राजकपूर के पास काम मांगने जाना पड़ा.राजकपूर ने उन्हें हाथों हाथ लिया.500 रुपये प्रति गाना लिखने का ऑफर दिया.शैलेन्द्र ने उसी समय बरसात का टाइटल-सांग बरसात में हमसे मिले तुम ओ सजन तुमसे मिले हम और पतली कमर है तिरछी नज़र है... लिखकर उनके हवाले किया.दोनों ही गाने सुपरहिट हुए.इसके बाद इस जोड़ी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
राज कपूर-शैलेंद्र ने 21 फिल्मों में साथ काम किया जिनमें मेरा नाम जोकर, तीसरी कसम, सपनों का सौदागर, संगम,अनाड़ी और जिस देश में गंगा बहती है शामिल थीं. राज कपूर का शैलेंद्र के घर पर आना-जाना लगा रहता था. राज कपूर शैलेंद्र को पुष्किन या कविराज बुलाते थे.जब भी शैलेंद्र कोई गीत लिखते तो राज कपूर कहते- वाह पुष्किन! क्या गाना लिखा है!
एक बार शैलेंद्र का लिखा गाना सुन रो पड़े थे राज कपूर
ये बात उस दौर की है जब फिल्म अनाड़ी (1959) का गाना सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी...रिकॉर्ड किया जा रहा था. यह गाना राज कपूर के पसंदीदा शैलेंद्र ने ही लिखा था. उस दिन वो रिकॉर्डिंग पर स्टूडियो नहीं पहुंचे थे. राज कपूर ने उस गाने की कॉपी अपने घर मंगवाई ताकि सुकून से उसे सुन सकें. वह कई घंटों तक लगातार इस गाने को सुनते रहे लेकिन जब उनसे रहा नहीं गया तो वह रात दो बजे शैलेंद्र से मिलने उनके घर पहुंच गए. वहां राज कपूर शैलेंद्र को गले लगाकर रो पड़े और कहने लगे-क्या गाना बना दिया शैलेंद्र, मेरे आंसू नहीं थम रहे. आवारा हूं.., मेरा जूता है जापानी.., रमैया वस्तावैया.., दोस्त दोस्त ना रहा.., प्यार हुआ इकरार हुआ.., सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है.., ये रात भीगी भीगी…, पान खाए सैंया हमारो…, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी…,हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा…, चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनियां,जीना यहां मरना यहां इसके सिवा जाना कहां…. राज कपूर के ऐसे पचासों सुपरहिट गाने हैं, जिनके बिना राज कपूर का सिनेमा अधूरा सा लगता है, और ये सभी गाने शैलेंद्र ने लिखे थे. गीतकार गुलजार साहब शैलेंद्र को हिंदी-सिनेमा का आज तक का सबसे बड़ा गीतकार मानते हैं.वो कहते हैं: उनके गीतों को खुरच कर देखें तो आपको सतह के नीचे दबे नए अर्थ प्राप्त होंगे. उनके एक ही गीत में न जाने कितने गहरे अर्थ छिपे होते थे. शैलेंद्र की मौत से टूट गए थे राज कपूर. फिल्मफेयर मैगज़ीन में अपने दोस्त शैलेंद्र की असमय मौत से दुखी राजकपूर ने एक ओपन लैटर लिखा था और कहा था: ऐसा लगता है कि जैसे मेरी आत्मा का एक हिस्सा चला गया.यह सही नहीं हुआ.मैं रो रहा हूं और चीख रहा हूं कि मेरी बगिया के सबसे खूबसूरत गुलाब को कोई तोड़ ले गया. वह बेहतरीन इंसान थे और मेरी ज़िन्दगी का अभिन्न अंग थे जो अब नहीं हैं.मैं केवल शोक मना सकता हूं और उनकी यादों में खो सकता हूं।
मनु भंडारी की रजनीगंधा
पहले रजनीगंधा फिल्म देखी थी, बाद में बीए हिंदी के पाठ्यक्रम में यही सच है नाम की कहानी पढ़ी. मेरे लिए दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है.खुले आसमान के नीचे बहती हवा सी हैं ये दोनों कृतियां. निःसंदेह इसके पीछे कहीं मन्नू भंडारी हैं.सत्तर के दशक में जब सिनेमा पर एंग्री यंग मैन का राज था, एक ऐसी फिल्म देखना जो पूरी कहानी को एक स्त्री की निगाह से कहती है, जिसे आज हम कहते द गेज़ ऑफ अ वुमन बिल्कुल अलग अनुभव रहा होगा. सिर्फ इतना ही नहीं उस स्त्री के चित्रण में जो ईमानदारी है, वह तो आज भी दुर्लभ है. उसकी दुविधा, उसका भय और उस स्त्री का अनुराग... सब कुछ कितना तटस्थ और सहज है फिल्म में.
नायिका दीपा (विद्या सिन्हा) के अवचेतन में छुपे एक डर से यह फिल्म आरंभ होती है, एक स्वप्न से... अकेले रह जाने, कहीं छूट जाने का भय. कहानी में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है. मगर जब फिल्म स्वप्न से शुरू होती है तो दर्शक की यात्रा भी भीतर से बाहर की ओर होती है.नायिका की निगाह अहम हो जाती है.उसी निगाह से हम उसके जीवन में आए पुरुषों को भी देखते हैं. हिंदी सिनेमा की बहुत बोल्ड या रैडिकल फेमिनिस्ट फिल्मों में भी स्त्री को इतना सहज और स्पष्ट नहीं दिखाया गया है.संगम जैसी फिल्म में दो नायक यह तय करना चाहते हैं कि नायिका किससे प्रेम करे, रजनीगंधा में यह फैसला नायिका पर छोड़ दिया गया है.उसके सामने दोनों ही राहें खुली हुई हैं. अभी उसके जीवन में शामिल संजय (अमोल पालेकर) लापरवाह है. उसकी छोटी-छोटी चीजों की परवाह वैसे नहीं करता जैसे कि कभी नवीन (दिनेश ठाकुर) करता था. जब कलकत्ता जाने पर दीपा की दोबारा नवीन (मूल कथा में यह नाम निशीथ है) से मुलाकात होती है तो पुरानी स्मृतियां उसे घेरने लगती हैं. इस दौरान बड़े खूबसूरत से प्रसंग हैं. खास तौर पर यह गीत दोबारा मिलने के इस प्रसंग को विस्तार देता है- कई बार यूँ ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है. दिनेश ठाकुर इस रोल में खूब जंचे हैं. लंबे बाल, आंखों में काला चश्मा, होठों में दबी सिगरेट.एक छोटे से फासले के बीच तैरती विद्या सिन्हा की निगाहें बहुत कुछ कह जाती हैं. हर बार उनके देखने में कुछ ऐसा है जैसे कि वह पुराने नीशीथ को तलाश रही हों.
यही सच है में दो शहरों का बार-बार जिक्र आता है, जैसे वह नायिका के बंटे हए मन को परिभाषित कर रहा हो, तो वहीं बासु चटर्जी ने रजनीगंधा में समय, शारीरिक दूरियों और शहर के बीच दूरियों के फासलों से कविता रच दी है. कहानी में मन्नू कलकत्ता में निशीथ से मुलाकातों के प्रसंग को कुछ इस तरह लिखती हैं, विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी. उसके इस अपनत्व-भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती थी, नकार भी नहीं पाती थी. सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही; पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की. मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी. दीपा के मन में सचमुच यह दुविधा है कि वह किसे प्रेम करती है? उसको अपने जीवन में किसे चुनना चाहिए? मन्नू लिखती हैं- ढलते सूरज की धूप निशीथ के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशीथ इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा-सा लगा. कलकत्ता से वापसी का कहानी में कुछ इस तरह जिक्र है, गाड़ी के गति पकड़ते ही वह हाथ को ज़रा-सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मुंद जाती हैं. मुझे लगता है, यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाक़ी सब झूठ है; अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है. दीपा कलकत्ता से जब कानपुर लौटती है तो अकेली नहीं, अपने साथ थोड़ा सा कलकत्ता भी साथ लेकर आती है. दुविधा, दो फांक में बंटा हुआ मन. संजय से मुलाकात नहीं होती है क्योंकि वह कहीं बाहर गया हुआ है. एक दिन तार आता है कि उसकी नियुक्ति कलकत्ता में हो गई. निशीथ का एक छोटा सा खत भी आता है. लेकिन जब संजय लौटता है तो... मन्नू ने इसे बयान किया है- बस, मेरी बांहों की जकड़ कसती जाती है, कसती जाती है.रजनीगंधा की महक धीरे-धीरे मेरे तन-मन पर छा जाती है. तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ, और मुझे लगता है, यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था...
फिल्म देखते वक्त शब्दों की यही अनुभूति एक गुनगुनाती हुई धुन में बदल जाती है. रजनीगंधा फूल तुम्हारे, महके यूँ ही जीवन में...यूँ ही महके प्रीत पिया की, मेरे अनुरागी मन में. सत्तर के दशक में विद्या सिन्हा ने जिस तरह का किरदार निभाया था, वह अपने-आप में अनूठा था.एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर स्त्री. उसके परिचय के लिए किसी पुरुष की दरकार नहीं थी. न हम उसके घर-परिवार के बारे में जानते हैं, न कोई अन्य रिश्ता. बस, वह शहर में एक किराए के मकान में रहती है. उसमें अपने करियर और जीवन के प्रति एक आश्वस्ति है. उसके अपने भय हैं, अपनी दुविधाएं हैं, उसका अपना अधूरापन है.वह परफेक्ट होने के बोझ से नहीं दबी है. फिल्म देखते समय, जीवन में आए दो पुरुषों के बीच आवाजाही करते उसके मन के प्रति हम जजमेंटल नहीं होते. उसे तो खुद नहीं पता है कि कौन सही है कौन गलत? मन्नू ने उसके मन पर नैतिकता का कोई बोझ नहीं रखा है. अंततः उसको ही अपना पुरुष चुनना है. मन्नू भंडारी ने इस कहानी के माध्यम से जो स्त्री रची है, वह इतनी ज्यादा सच है, इतनी साधारण है कि असाधारण बन गई है. राजेंद्र यादव ने स्त्री विमर्श में देह से मुक्ति की खूब बातें कीं, मगर कितनी रचनाओं में मन से मुक्त ऐसी स्त्रियां दिखती हैं? वापस फिल्म की तरफ लौटता हूँ तो योगेश का लिखा वह गीत याद आ जाता है, जो यही सच है कहानी की खुशबू को हम तक किसी हवा के झोंके की तरह पहुँचा जाता है. कई बार यूँ भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है मन तोड़ने लगता है अनजानी प्यास के पीछे अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है.
दिनेश श्रीनेत का लेख
चमन बहार: एक भयावह यथार्थ से परिचय
हेमलता महिश्वर
‘चमन बहार’ छत्तीसगढ़ के एक छोटे से कस्बेनुमा नगर की एक कहानी है जो जिला बन गया है। यहॉं का सारा समाज ग्रामीण परिवेश से शहरी परिवेश की ओर जाने को अग्रसर है। पर यह सोपान मूलत: भौतिक है। इसमें भावात्मकता तो है, भौतिक विकास की चाहत भी है पर वैचारिकता सिरे से नदारत है।
यहॉं का युवा वर्ग इसी सपने में जी रहा है। वह सपने तो देख रहा है पर सपनों को पूरा करने के लिए उसके पास कोई दिशा-निर्देश नहीं है। ऐसी स्थिति में वह स्वत: जितना कुछ समझ पाता है, उतना ही करने के लिए न केवल प्रयासरत है बल्कि सन्नद्ध भी है।
विवेच्य फ़िल्म के अनुसार छत्तीसगढ़ में यह युवा चार तरह का है -पहला तो वह जो निपट स्थानीय है, दूसरा वह जो बाहर से आया है और प्रभुत्व हासिल कर चुका है, तीसरा वह जो स्थानीय नेतागीरी में दाख़िला ले रहा है और चौथा वह जो इन दोनों के बीच तालमेल बिठाते हुए अपने पौ बारह करना चाहता है। सारी फ़िल्म इसी कथानक के इर्द-गिर्द बुनी गई है।
फ़िल्म का नायक जो पहली तरह का युवा ‘बिल्लू’ है जो वन विभाग के चौकीदार पिता की तरह जीवन नहीं जीना चाहता। वह स्वप्नदर्शी है। वह सरकारी नौकरी करते हुए जीवन बीताना नहीं, जीवन जीना चाहता है इसलिए जंगल का सुरक्षाकर्मी बनने के बजाय अपनी दुकान खोलना चाहता है। चूँकि मुँगेली को शहर में तब्दील करने की योजना है, सो वह संभावित हाइवे पर एक पान की दुकान खोलता है। यह जगह उसे अचानक ही सस्ते में मिल जाती है। पर इस जगह की बहार उजाड़ में बदल जाती है और ग्राहक न मिलने के कारण वह मक्खी मारता, उंघता हुआ ट्रांजिस्टर सुनता है। जगह ऐसी बियाबान है कि ट्रांजिस्टर की फ़्रीक्वेंसी तक मैच नहीं करती। इस समय चौथी तरह के दो युवक उसके पास आते हैं और उसे सूचना देते हैं कि तुम्हें यह जगह सस्ते में बेचकर जानेवाला अपना मुनाफ़ा कमा गया। अब यहॉं हाइवे नहीं बनेगा और तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। इतनी सूचना देकर वे बिल्लू की दुकान से बिना पैसे दिए गुटका आदि ले लेते हैं और बिल्लू के पैसे माँगने पर उसे उल्टे धमका भी देते हैं। अब बिल्लू की चिंता शुरू होती है। एकाएक वह समझ नहीं पाता कि उसे करना क्या चाहिए। अगले दिन से वह फिर से दुकान में जाकर के बैठ जाता है। घूरे के दिन फिरते हैं - बिल्लू के दिन भी फिरने का अवसर आया। सड़क के दूसरी तरफ़ एकमात्र खड़े डुप्लेक्स मकान का रंग-रोगन होना आरंभ होता है। एक दिन वह देखता है कि एक परिवार उसकी दुकान के ठीक सामने सड़क पार बने इसी एकमात्र भवन में आकर उसे गुलज़ार करता है।
अचानक बारिश होती है जो इस बात का संकेत है कि उजाड़-बियाबान हरियाली में परिवर्तित होनेवाला है। सामानवाले ट्रक के पीछे एक कार आती है जिसमें से उस परिवार के सदस्य उतरते हैं। अचानक बारिश अच्छी तेज होती है और उस तेज बारिश में ही एक लड़की अपने कुत्ते के साथ उतरती है और दौड़कर मकान के भीतर चली जाती है। तेज बारिश के साथ लड़की का देखना एक फैंटेसी क्रिएट करता है, एक संकेत देता है। निर्देशक यहॉं पर पौराणिक कथा का आधार लेने से बिलकुल नहीं चूकता। ठीक इस समय यही बिल्लू अपनी दुकान में लक्ष्मी का फ़ोटो टाँगने के लिए कील ठोंकता भी है और सामने की तरफ़ देखता भी है जिससे हथौड़ी से उसे चोट लग जाती है। इसी समय चौथे नंबर के दो युवक है उससे कहते हैं कि लक्ष्मी आ गई है, लड़की आ गई है, अब दुकान चलेगी। इस तरह से निर्देशक जनता में निर्मित भाववाद को हरियाने में सफल हो जाता है। ये दोनों लड़के शहर के दूसरे और तीसरी श्रेणी के युवकों को बिल्लू की दुकान तक लाने के तरह-तरह के जतन करते हैं। बिल्लू की दुकान चल पड़ती है।
निर्देशक युवकों में लहलहाती पितृसत्तात्मक मानसिकता की उपस्थिति दर्ज़ करने लगता है। लड़की जो स्कूल गोइंग है, वह सारे शहर के युवा वर्ग का आई-टॉनिक बन जाती है। स्कूल गोइंग लड़के हों या शहर के युवा नेता या शहर का युवा व्यवसायी कोई भी। कोई भी लड़का उस लड़की की झलक पाने के लिए, उसको अपना बताने के लिए इस पान की दुकान तक आता है और उस लड़की को अपना बताने का प्रयास करता है। ये लड़के साइकिल, पैदल, जीप या मोटरसाइकिल आदि जो हर तरह के वर्ग के संबंधित हैं, पान की दुकान पर अड्डेबाज़ी करने लगते हैं। यह युवा वर्ग इस बात की चिंता ही नहीं करता कि लड़की क्या चाहती है। लड़की और लड़की का परिवार बहुत ही पॉलिश्ड है और अड्डेबाज़ी करते युवकों के समूह में लड़की और लड़की के परिवार से मैच करता कुछ भी नहीं है। न रहन-सहन, न बोली-भाषा, न मानसिकता, पान चबाते, सिगरेट-शराब पीते, मॉं-बहन एक करते हर तरह के लड़के उस लड़की को पाने का ख़्वाब लिए पान की दुकान पर मंडराने लगे। चौथी श्रेणी के दो युवकों ने पूरे शहर के प्रभावशाली युवकों को बिल्लू की दुकान की ओर भेज दिया। इन दोनों लड़कों की लफुटई को इससे स्थायित्व प्राप्त हो रहा था। एक नेता और एक व्यवसायी को आपस में भिड़ाकर इनका उल्लू सीधा होने लगा था। ऐसा नहीं है कि यह बिल्लू नहीं समझ रहा था। बिल्लू की दुकान अच्छी चलने लगी। चौथी श्रेणी के युवकों ने दुकान के बाजू में कैरम बोर्ड भी रखवा दिया। सिगरेट, गुटका, कोल्डड्रिंक के अलावा प्रभावशाली लड़के शराब लेकर वहॉं जम जाते। बिल्लू को यह पसंद नहीं आ रहा था। एक बार लड़की उसकी तरफ़ देखकर मुस्कुराई थी क्योंकि एक आवारा कुत्ते से बिल्लू ने लड़की के कुत्ते को बचाया था। बिल्लू ने लड़की के एक सहज मानवीय शिष्टाचार का ग़लत मतलब निकाला जो पुरुष मानसिकता ‘लड़की हँसी तो फँसी’ का द्योतक है।
लड़की की इच्छा हो या न हो, इसे जाने बग़ैर लड़के उसके आस-पास मंडराने लगते हैं। यह जिला मुंगेली की ही नहीं, पूरे भारत की ही दशा है। लड़की का यह परिवार मिडिल क्लास परिवार है। इस परिवार की यह लड़की स्कूल जाती है, स्कूटी चलाती है और अपने कुत्ते को लेकर घुमाने जाती है। कुल मिलाकर यह लड़की अपने घर से तीन बार ही निकलती है। बिल्लू यह नोटिस लेता है कि लड़की अपनी स्कूटी से पहले अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़ने जाती है। दूसरी बार वो निकलती है तो स्कूटी से अपने स्कूल जाती है और तीसरी बार शाम को वो अपने कुत्ते को बाहर पैदल घुमाने ले जाती है। इस ताज़ा-ताज़ा जिला बने शहर में किसी लड़की का स्कूटी चलाना एक बड़ा आश्चर्य है, दूसरे लड़की का लंबे खुले सीधे बाल रखना बहुत बड़ा आश्चर्य है, तीसरा जो क़हर बरपाता हुआ आश्चर्य हैं कि लड़की शॉर्ट्स पहनती है और कुत्ते को घुमाने ले जाती है, फिर चौथी परेशानी यह है कि लड़की किसी की तरफ़ देखती तक नहीं। वह सिर्फ़ अपने काम से काम रखती है। अपना काम करती है और घर वापस चली जाती है। जिस जीवन स्तर को वो लड़की अपने परिवार के साथ जी रही है, समान जीवन स्तर तो दूर, इनके आस-पास एक भी घर भी नहीं है ताकि वह इधर-उधर कहीं जा सके। आज भी लड़कियों की कंडीशनिंग ऐसे ही होती है कि वह चुपचाप अपने घर से निकलकर चुपचाप अपना काम करके वापस आ जाए। उसका इधर-उधर देखने का मतलब चरित्र ढीला है। यह लड़की भी किसी की तरफ़ देखती तक नहीं है। लड़की की भूमिका सिर्फ़ इतनी है कि वह घर से निकलती है स्कूटी से और घर वापस आती है स्कूटी से। वह स्कूटी से ही स्कूल से भी निकलती दिखाई देती है। वहॉं भी उसके कोई दोस्त या सहेलियां नहीं हैं। निर्देशक इस मामले में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लड़की वाला पात्र उसके चित्रण का हिस्सा नहीं है, वो केवल और केवल युवकों की मानसिकता पर केंद्रित हो रहा है।
शहरी आबादी से दूर अकेला परिवार निपट अकेले मकान में है और सड़क के इस तरफ़ बिल्लू की दुकान जहॉं शहर के तमाम लड़के जमा होना शुरू हो जाते हैं। लड़के बिल्लू से यह पता करने का प्रयास करते हैं कि लड़की किस-किस समय घर से बाहर निकलती है पर बिल्लू अंजान बना रहता है। एक बार पूरे हुजूम के डटे रहने पर बिल्लू देखता है कि लड़की अपने कुत्ते को घुमाने बाहर लेजा रही है, वह लड़कों का पूरा ध्यान कैरम पर केंद्रित करवाता है।
बिल्लू न तो ताक़तवर है न ही प्रभावशाली। सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट की तर्ज़ पर वह तरह- तरह के षडयंत्र रचता हुआ युवा नेता और युवा व्यवसायी को भिड़ाकर अपने लिए सुरक्षित स्थान बनाना चाहता है। वह अपने एकतरफ़ा प्यार में इतना सघन है कि वह यह चुनौती भी ले लेता है कि अपने ही पिता के बॉस को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि अपने बेटे को सिगरेट पीने से मना करो। बॉस का यह बेटा भी लड़की के चक्कर में उसकी दुकान पर सिगरेट फूँकता बैठा रहता था।
वह आम लड़कों की तरह अपनी साक्षरता बस इतना सा लाभ ले पाता है कि जगह-जगह दिल का तीर लगा निशान अपने और रिंकू के नाम के साथ उकेर देता है। वह ‘आर’ अक्षर अपने हाथ में गुदवा लेता है। वह पिता द्वारा पसंद की गई लड़की से शादी नहीं करना चाहता। यहॉं पिता एक सूत्र वाक्य कहता है-“औरत है तो समाज है।” स्त्री की ऐसी ही महत्ता बुद्ध भी स्थापित करते हैं।
बिल्लू अपना प्यार जताने के लिए लड़की को एक लव-कार्ड देना चाहता है। लड़की को वह कार्ड नहीं दे पाता तो उसकी बालकनी की तरफ़ उछाल देता है। निर्देशक ने यहॉं लड़के की मनोदशा को बड़ी ही ख़ूबसूरती से चित्रित किया है। पर यह कॉर्ड लड़की के पिता के हाथ लगता है। पिता के द्वारा पूछे जाने पर कि कार्ड किसने डाला, बिल्लू साफ़ नट लेता है और अपनी अनभिज्ञता ज़ाहिर करता है।
अब पुलिस आती है और बिल्लू की खूब पिटाई करती है और अन्य लड़कों की भी पिटाई करती है। इसके बाद जब एक दिन लड़की रस्सी पर सूख रहे कपड़े भितराने के लिए टैरेस पर आती है तो बिल्लू को अपनी ओर देखता पाकर तुरंत वापस चली जाती है। बिल्लू का एक तरफ़ा प्यार इस उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह दुकान नहीं खोलता, उधारी सामान देनेवाले तगादा करते हैं। पर वह तो अब लड़की से बदला लेने को आतुर है। वह लड़की का पीछा करता है और कुछ करने के पहले ही नाकाम हो जाता है। वह ‘सोनम गुप्ता बेवफ़ा है’ की तर्ज़ पर ‘रिंकू नोनारिया बेवफ़ा है’ नोटों पर लिखता है, तगादा करनेवालों को वही नोट देकर लड़की को बदनाम करता है। पुलिस को इस हरकत का पता चलते ही वह उसे न केवल पकड़कर ले जाती है अपितु उसकी दुकान भी तोड़ देती है। अब तो शहर की पितृसत्ता जाग जाती है और ख़ुद को बचाए रखने के लिए मानवाधिकार के छद्म में अपनी आवाज़ बुलंद करती है। बिल्लू की दुकान का न होना मतलब नैन सुख का अवसर न होना। सारे दुष्ट मर्द इकट्ठे होकर पुलिस थाने में अपनी मॉंग दर्ज करते हैं कि बिल्लू निर्दोष है, कमज़ोर पर पुलिस रौब झाड़ती है। स्थानीय न्यूज़ चैनल इसे हॉट टॉपिक बनाते हैं। अंतत: लड़की का पिता ही उसकी बेल कराता है। इससे यह ज़ाहिर होता है कि यह परिवार किसी का बुरा नहीं चाहता। ‘क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात’ की तर्ज़ पर या बुद्ध दर्शन की करूणा पर संचालित होता हुआ यह परिवार बिल्लू को सुधार का अवसर देना चाहता है। बिल्लू के जेल से रिहा होने पर उसे हीरो बनाकर युवा राजनेता द्वारा अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास किया जाता है। इसमें युवा राजनेता की मॉं भी शामिल है। पितृसत्ता उन महिलाओं को खुलकर सामने आने देती है जो पितृसत्ता की जड़ें मज़बूत करने में सक्रिय सहयोग देती हैं।
पर बिल्लू लड़की के पिता की सह्रदयता से प्रभावित है। वह लड़की के घर जाता है। लड़की की मॉं बग़ैर किसी द्वेष के बिल्लू को ससम्मान भीतर बुलाती है। बिल्लू अपने जूते उतारने लगता है, वह उसे जूतों सहित अंदर बुलाती है। सोफ़े पर लड़की के पिता के सामने उसे बैठने को कहती है। बिल्लू के लिए यह एक नई दुनिया है। वह पूरे कमरे को झिझकती नज़र से देखता है। लड़की के माता-पिता का सामने बैठना, लड़के का सामने टेबल पर पढ़ाई करना, दीवार पर पूरे परिवार की तस्वीर का अलग-अलग अंदाज़ में होना, परिवार के सदस्यों का पोर्ट्रेट होना, लड़की का पोर्ट्रेट होना यह सब देखता हुआ वह पर्दे के पीछे खड़ी लड़की को देखते रह जाता है। यहॉं निर्देशक ने क़माल किया कि कोई सीन क्रियेट नहीं किया। मॉं यह भाँपकर अपनी बेटी से कहती है-“बेटा, चाय लाना तो।” और निर्देशक ने दिखाया कि बिल्लू जैसे ज़मीन में गड़ गया। उसकी नज़रें उठती ही नहीं जबकि लड़की चाय देकर भी चली जाती है। परिवार बिल्लू को सूचना देता है कि यह शहर उनके लायक़ नहीं है। वे अपना परिवार वापस बिलासपुर शिफ़्ट कर देंगे। बिल्लू वापस होता है और पश्चाताप करता है। वह अपनी ही चप्पल से अपने ही सिर को मारता है। स्थिर होकर पुनः उसी जगह पर अपनी वही दुकान खोलता है और वैसे ही मक्खी मारता ट्रॉंजिस्टर सुनता है। एक दिन मकान में वह एक गुलाबी काग़ज़ फड़फड़ाते हुए देखता है। वह उस काग़ज़ को ले आता है और देखता है कि काग़ज़ के एक तरफ़ कोई डायग्राम बना है और दूसरी तरफ़ उसी की तस्वीर है जिसमें वह अपनी विशिष्ट मुद्रा में अपनी दुकान के सामने खड़ा रहता था। इससे यह ज़ाहिर होता है कि जिसने भी लाइव पेंटिंग की थी, उसने बिल्लू को अपना सब्जेक्ट बनाया था। निर्देशक ने बड़े चातुर्य के साथ इसे संशय की तरह उपस्थित करने का प्रयास किया है। जैसी पात्रता होगी, वही ग्रहण किया जा सकेगा। मेरे नज़रिए से इस निर्जन स्थान में यही एक जीवन था जिसे लाइव पेंटिंग में दर्ज किया गया। अपनी दुकान में मक्खी मारता बिल्लू एक दिन देखता है कि सामनेवाले मकान में फिर कोई सामान से लदा ट्रक आकर खड़ा हुआ है, स्कूटी उतारी जा रही है और बिल्लू पुन: उसी पेंटिंग वाली मुद्रा में खड़ा है।
यह फ़िल्म छत्तीसगढ़ के युवकों की स्थिति पर सोचने के लिए बाध्य करती है। छत्तीसगढ़ भारत का वह राज्य है जहाँ आज भी स्त्री और पुरुष जनसंख्या का अनुपात लगभग बराबर है और ग्रामीण क्षेत्र में तो और भी समानुपातिक जनसंख्या है। इसका मतलब है कि वहॉं लड़की का पैदा होना सामाजिक शर्म का कारण नहीं है। छत्तीसगढ़ की औरतें दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करने में अभी भी काफ़ी स्वतंत्र हैं। यदि पति से पटरी नहीं बैठ रही है तो उसे यह सामाजिक अधिकार प्राप्त है कि वह पति का घर छोड़ सकती है। साथ ही, उसे यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह दूसरा विवाह रचा सकती है। उत्तर भारत की औरतें यह सोच भी नहीं सकतीं। उनकी संस्कृति तो पति के घर में जाने के बाद अर्थी उठने की ही है। पितृसत्ता का जैसा शिकंजा और जकड़न उनके भीतर कसा हुआ है यह छत्तीसगढ़ की औरतों के साथ नहीं है। छत्तीसगढ़ में तमाम पितृसत्ताक व्यवस्था के बावजूद स्त्री सहमति/असहमति मायने रखती है।
इस फ़िल्म को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि उत्तर भारतीय जनता जो छत्तीसगढ़ में निवासरत है, अपनी कुसंस्कृति की जड़ें जमा रही है।
कितने ही समझदार माता-पिता क्यों ना यदि लड़की के लिए इतना प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा तो ऑनर किलिंग की नौबत आते देर न लगेगी। छत्तीसगढ़ के लड़के स्त्री को इस तरह से वस्तु में बदल देंगे?
छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी और शिक्षा का दर और स्तर क्या है कि युवकों की इतनी बड़ी संख्या एक लड़की के पीछे पड़ जाएगी?
इस फ़िल्म का कथानक भयावह है। फ़िल्म के निर्देशक ने एक भयावह सचाई सामने रखी है। हमें छत्तीसगढ़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक पड़ताल वर्तमान संदर्भ में करने की अनिवार्य आवश्यकता है। इन सारे मुद्दों पर चिंतन करने के लिए बाध्य करना ‘चमन बहार’ के निर्देशक की सफलता है। फ़िल्म यथास्थिति से परिचय कराती है।
बाक़ी कलाकारों का अभिनय उम्दा है, कहीं भी नकलीपन ज़ाहिर नहीं होता। गीत-संगीत, संवाद यथावसर उचित हैं।
उजड़े चमन में नई बहार
अंजन कुमार
हाल में ही मुझे अपूर्वधर बड़गैया के द्वारा निर्देशित फिल्म चमन बहार को देखने का अवसर मिला। कोई भी फिल्म अपने समय से अलग नहीं होती और समय से काटकर उसका मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता हैं। इसलिए फिल्म पर बात करने से पहले थोड़ी-सी बात यदि वर्तमान संदर्भ पर कर ली जाए तो मुझे लगता है कि फिल्म को और भी बेतहर व नये ढंग से समझने के कुछ नए सूत्र मिल सकते हैं.
सबसे पहले हम अपने बाजारवाद से पनपे उपभोक्तावादी संस्कृति की बात करते हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि बाजारवाद ने गांव और शहर के बीच एक गहरी खाई को जन्म दे रखा है. इसने साथ ही व्यक्ति के भीतर असंतोष की उस कुंठा को भी जो उसे कहीं न कहीं से हिंसक बनाती है. जब कोई बाजार आधारित जीवन के तमाम सुख-सुविधाओं से खुद को वंचित पाता है तो एक आधुनिक खूबसूरत लड़की से प्रेम की इच्छा उसके लिए स्वप्नमात्र बनकर रह जाती हैं। यह वंचित वर्ग आत्महीनता, घृणा, नफरत जैसी कुंठाओं से भरा हुआ है और असंतोष का जीवन जीने के लिए बाध्य है. इसी असंतोष के चलते स्त्रियों पर तथा दूसरे तरह के अपराध हो रहे हैं. उपभोक्तावादी संस्कृति ने मनुष्य को उपभोग की वस्तु या फिर उपभोक्ता पशु में तब्दील कर दिया हैं। मनुष्य के भीतर की संवेदना, संबंधों की गरिमा, प्रेम की कोमल भावना और सुंदरता जैसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों को बुरी तरह विकृत कर दिया है। आजकल की अधिकतर फिल्में, वेब सीरिज इन्हीं विकृतियों का शिकार है और पैसा कमाने में लगी हुई है। इस तरह से यह समय कई तरह की विद्रूपताओं से भरा है।
मगर इस खौफनाक समय में जब हम चमन बहार से गुजरते हैं तो पाते हैं कि यह फिल्म सारी विकृतियों से बचते हुए और उसका बेहद सुंदर ढंग से प्रतिरोध करती हैं। इस फिल्म का नायक बिल्लू इसी प्रतिरोध का प्रतीक है। जो पढ़ा-लिखा होने के बावजूद बाजार के इन सारे प्रभावों से मुक्त एक स्वप्नजीवी पात्र हैं। जो फिल्म की नायिका को लगातार उन बाजारू नजरों से बचाने की कोशिश करता नजर आता है जो उसे एक आकर्षक वस्तु की तरह देखते है। बिल्लू इस समाज का वही वंचित वर्ग है जो किसी आधुनिक सुंदर लकड़ी से प्रेम करने का स्वप्न देखता है, लेकिन उन कुंठाओं से मुक्त है जो उसे हिंसक बना सकती थीं...क्योकि बिल्लू के जीवन में रिंकू उसके स्वप्न को साकार करने वाली एक आशा या उम्मीद की तरह आती हैं। इस बात को समझने के लिए फिल्म के एक दृश्य याद करना पड़ेगा। बिल्लू अपने ठेले पर माता लक्ष्मी की फोटो को टांगने के लिए कील ठोंक रहा होता है तब रिंकू अपनी गाड़ी से कुत्ते को लेकर उतरती है. बारिश होती है. फिल्म का पात्र सोमू डैडी बिल्लू से कहता है - ’’लड़की शुभ है तेरे लिए डैडी’’। फिर लक्ष्मी की तस्वीर की तरफ कैमरा घूमता है। बिल्लू की आंखों में अपने स्वप्न के पूरे होने की उम्म्मीद की चमक तैर जाती है। बिल्लू, रिंकू को अपने पहचान की आशा के रूप में देखता है और उससे मन ही मन प्यार करने लगता है। यह प्रेम बाजारू संस्कृति के दुष्प्रभाव से मुक्त बेहद स्वभाविक और कोमल भावों से युक्त प्रेम है। जिससे वंचित हो जाने का डर उसे लगातार उन छुटभैय्ये नेता शीला, आशु और अन्य आवारा लड़कों से बना रहता है। जिसे फिल्म बीच-बीच में चल रहे एक गाने - ‘भौरें ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर’ के माध्यम से समझा जा सकता हैं। प्रेम भावनाओं के साथ कैसे राजनीतिक समझ को भी विकसित करता हैं। इसे बिल्लू के द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वियों को रास्ते से हटाने की चालों से समझा जा सकता हैं। निम्न वर्ग का बिल्लू संभ्रात परिवार की रिंकू को प्रेमपत्र के रूप में ग्रिटिंग देना चाहता है, लेकिन उसकी गरीबी उसे कमजोर बनाती है तो वह गले में एक लॉकेट अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने उद्देश्य से पहनता है। क्योंकि उसके जीवन ऐसा कुछ भी नहीं जो उसे आत्मविश्वास से भर सकें. जिसे बाद में उतारकर भी फेंक देता है। पुलिस के द्वारा पीटे जाने के बाद उसका प्रेम से भरा संवेदनशील हृदय अपनी आत्महीनता के और गहरे तल में जा गिरता हैं। पिता उसकी शादी कर देना चाहते है। वे कहते हैं - ‘‘एक स्त्री समाज से जोड़ती है। शादी कर लेगा तो समाज से फिर जुड़ जायेंगे’’ यह संवाद स्त्री के महत्व के साथ ही उनकी सामाजिक स्थिति व पीड़ा को भी उजागर करता है। इसी तरह साधु और उसके बीच का संवाद जहां साधु, बिल्लू से कहता है - ‘‘जीवन कुछ नहीं नदिया का पानी है, या तो खुद को नाव बना लें या धारा के साथ हो जाओ, उल्टा तैरेगा तो मारा जायेगा’’ यह कहते हुए साधु अपने प्रेम की विफलता अपनी प्रेमिका के बेवफा हो जाने को बताता हैं। जिसका जिक्र करते हुए साधु मर जाता है। बिल्लू छाती पर उसकी प्रेमिका का नाम खुदा हुआ देखता है और फिर अपने हाथ को जिसमें रिंकू के नाम का पहला अक्षर आर खुदा रहता हैं। यहां साधु के प्रेम और अपने प्रेम की विफलता को वह एक साथ महसूस करता है...और वह रिंकू को बेवफा के रूप में प्रचारित करने के लिए पूरे गांव में जगह-जगह और नोट में लिख देता कि रिंकू बेवफा है। अपने इस कृत्य के कारण वह पुलिस की पिटाई भी खाता है। उसका पान ठेला पलट दिया जाता हैं। फिल्मकार ने इस दृश्य को बहुत अच्छे से फिल्माया है। उसे जेल में डाल दिया जाता है। जिस पर शीला भईया और उसकी मां आंटी जी राजनीति करने लगती हैं। रिंकू के पिता सारा कुछ हो जाने के बावजूद बिल्लू को थाने से छुड़ाते हैं। यह उनकी मानवीय संवेदना को दर्शाता है। थाने से राजनीतिक रैली निकाली जाती है। बिल्लू अपने घर से सीधा रिंकू के घर जाता है। जहां वह उसके घरवालों का व्यवहार और घर में लगी रिंकू और उसके परिवार की तस्वीरों को देखता हैं और अपने किए गलती पर आत्मग्लानि से भर जाता है। घर से निकलकर रास्ते भर वह खुद को चप्पल से मारता है और रोते हुए पश्चाताप करता है। यह दृश्य भी बेहद ही संवेदनशील है। कुछ दिनों के बाद रिंकू के घरवाले गांव छोड़कर चले जाते है। बिल्लू अपने ठेले पर उदास बैठा रहता है। तेज हवा चलती वह उस खाली पड़े घर में जाता है, जहां उसे गुलाबी रंग का एक कागज हवा में लटका हुआ मिलता हैं। जिसके एक तरफ विज्ञान का कोई चित्र और दूसरी तरफ उसके पान ठेले में खडे़ होने की एक खास मुद्रा का चित्र बना होता हैं। जिससे रिंकू के भी प्रेम में होने का पता चलता है। कुछ दिन बाद फिर उस घर में एक नया परिवार उतरता है। एक स्कूटी ट्रक से उतारी जाती है। बिल्लू फिर अपनी उसी मुद्रा में खड़ा हुआ, उस घर की तरफ देखता रहता हैं।
फिल्म फिर एक उम्मीद की तरफ इशारा करते हुए खत्म हो जाती है। लेकिन दर्शक बिल्लू की इस उम्मीद को अपने साथ घर लेकर जाता है कि एक न एक दिन बिल्लू का जीवन संवर जाएगा. इस तरह यह फिल्म प्रेम को उसकी स्वभाविकता के साथ बहुत ही सुंदर व यथार्थ पूर्ण ढंग में प्रस्तुत करती है। जो प्रेम की कई सुंदर कहानियों और बेहतरीन फिल्मों की याद ताजा कर देती है। इसके साथ ही यह फिल्म स्त्री को एक उपभोग की वस्तु के रूप में देखे जाने वाली सामंती और बाजार की मानसिकता का प्रतिरोध भी करती है। इस फिल्म के सभी दृश्यों को कैमरे के माध्यम से बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया हैं। फिल्म में सभी कलाकारों ने बहुत शानदार अभिनय किया है। इसके सारे संवाद रचनात्मक और रोचक है। फिल्म के गानों को भी एक नए ढंग से इस्तेमाल किया गया है उसकी अर्थवत्ता के साथ। फिल्म को इस तरह से बुना गया है कि दर्शक अंत तक इस फिल्म से अपना जुड़ाव बनाए रखता है। यह फिल्म एक क्षेत्र विशेष में फिल्माए जाने के बावजूद देश के हर हिस्से में मौजूद गांव-कस्बे की कहानी बन जाती हैं। इस फिल्म को क्षेत्र विशेष की सीमा में रखकर देखना उचित नहीं है. कुल मिलाकर यह फिल्म इस हिंसक और विद्रूप समय में प्रेम को, सुंदरता को, मानवीय संवेदनाओं को उसकी स्वभाविकता में पुर्नस्थापित करती एक खूबसूरत फिल्म है। जिसमें निर्देशन की एक नई दृष्टि देखने को मिलती जो इस फिल्म को अलग व महत्वपूर्ण बनाती है। यह फिल्म उजड़ते हुए चमन में एक नये बहार की शुरूआत है। संवेदनशील और समझदार दर्शकों को इस नए अनुभव से अवश्य गुजरना चाहिए।
हे समीक्षकों... हम दर्शकों से भी तो पूछ लीजिए कि कैसी लगी चमन-बहार
सत्यप्रकाश सिंह
ये तो अपने कांकेर जैसा है यार...जब आपके और हमारे लबों पर ऐसी कोई बात किसी फिल्म को या किसी स्टोरी को पढ़ते- पढते मचल जाये तो समझ लीजिये रचनाकार का पसीना मोती में तब्दील हो रहा है.
मै बात कर रहा हूँ चमनबहार फिल्म की जिसने मुझे तारूण्य की स्मृतियों के उन लम्हातों से जोड़ दिया जहाँ कस्बाई जीवन की भावनाएं इसी प्रकार जीवन्त होती है जो परदे पर उतारी गई है !
मैं एक आम दर्शक हूं
हम पूरी फैमिली के साथ ही कोई मूवी देखते है और जब गृहस्वामिनी ने कहा कि नेटफ्लिक्स पर छत्तीसगढ़ के एक लड़के की मूवी देखनी है तो मेरा पहले मेरा साहस डगमगा गया.दरअसल आजकल नेटफ्लिक्स हो या अमेज़न इन पर सस्ती उत्तेजना का नशीला बाज़ार सजा हुआ है. बहरहाल बात जब छत्तीसगढ़ की हो तो सारा परिवार था स्क्रीन के सामने था. फिल्म के प्रारंभ होते ही मै उसकी सहजता से जुड़ता चला गया. एक आम दर्शक चाहता है कि स्वस्थ मनोरंजन हो. यही इस फिल्म की बुनियाद है.एक साधारण सी कहानी कैसे असाधारण बन जाती है. यह मुझे चमनबहार में नजर आया. सच कहूं तो मुझे बेहद खुशी हुई अपनी माटी की इस अशेष प्रतिभा के लिए जिसनें मुट्ठी भर लाई को जीवन की सहजताओं के साथ पिरों कर आसमां में बिखेर दिया है.
अप्रतिम अपूर्व !
आंचलिकता के नाम पर यहां की छत्तीसगढ़ी फिल्मों में जो फूहड़ता चल रही है अपूर्व ने उस फूहड़ता से अपनी फिल्म के कथानक को बचाकर रखा है.फिल्म को जब हम देखने बैठते है तो ऐसा नहीं कि इसमें कमी नहीं दिखती मगर खूबियां इतनी है कि कमियां नजरअंदाज हो जाती है और वह भी तब जब निर्देशक की यह प्रथम फिल्म हो. कम से कम संवाद में मुखर संसार का सृजन इस फिल्म की एक ख़ास विशेषता भी है. ग़ौरतलब है नायिका का एक भी संवाद ना होना इस फ़िल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है.दरअसल निर्देशक ने नायिका की भाव-भंगिमाओं और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को ही संवाद का सेतु बना दिया है. फिल्म के नायक ने अपने कसे हुए अभिनय के साथ कस्बों में या कह ले शहरों के गली-मुहल्लों के उस किरदार को जिंदा कर दिया है जिससे हम और आप अक्सर मिलते रहते है. इस फिल्म से एक बड़ा दर्शक इसलिए भी जुड़ रहा है क्योंकि ज्यादातर लोगों ने यह यथार्थ भोगा है.
फ़िल्म को लेकर समीक्षकों के बीच बहस का दौर जारी है. कोई आदर्शवाद की दुहाई दे रहा है कोई पितृसत्ता का परचम लहरा रहा है और कोई बस अपने नज़रिए की बात कर रहा है. एक बार जनाब हम दर्शकों से भी तो पूछ लीजिए हमें यह फिल्म क्यों अच्छी लग रही है.क्या चमनबहार की कहानी मेरे और आपके समाज में रोज घटने वाली सच्ची कहानी नही है? कौन इस कहानी को बढ़ावा देना चाहेगा मगर इस सच को छत्तीसगढ़ के अपूर्वधर ने जिन बारीक़ियों के साथ परदे पर उकेरा है वो अद्भुत है. हम सबके लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के इस युवा को आज पूरे देश में उसकी इस फिल्म के लिए सम्मान मिल रहा है और उसके काम पर बाते हो रही है. हबीब साहब की माटी पर अपूर्व का यह आगाज़ नयी इबादत रचेगा यह तो तय है.
अगर मेरी तरह आप भी उनचास के है और बीस-तीस बरस पुराने दिनों को एकबार फ़िर से जीना चाहते है तो चमनबहार हाज़िर है. अगर आप जीना नहीं जानते. जीना नहीं चाहते तो सड़ते रहिए. मरते रहिए. मरने से कौन रोकता है.
|
|
|
किसी शाम प्यार आएगा: अपूर्व का चमनबहार
भुवाल सिंह
अपूर्व निर्देशित 'चमनबहार 'की कहानी छत्तीसगढ़ के लोरमी कस्बे के युवक बिल्लू के इर्द गिर्द घूमती है. बिल्लू पहचान के संकट से गुजर रहा है. अपनी पहचान बनाने के लिए वह वन विभाग की चौकीदारी छोड़कर दिनेश की मदद से लोरमी रोड पर 'चमनबहार' नाम से पानठेला खोलता है. कथा के केंद्र में रिंकू नामक लड़की है जो फ़िल्म में लगभग न के बराबर बोलते हुए भी फ़िल्म की असल गति है. रिंकू के पिता इंजीनियर है और लोरमी में नए-नए शिफ़्ट हुए हैं. इंजीनियर का आवास ठीक पानठेला के सामने है. मुंगेली जिला बनने के बाद लोरमी का बाजार गड़बड़ा गया है और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित चमनबहार पानठेला है.लेकिन इंजीनियर साहब के आने के बाद यानी रिंकू की उपस्थिति से यह वीरान पान की दुकान चल निकली है.
यहीं से कथानक में गति आती है. पान की दुकान की रंगीनी रिंकू की उपस्थिति से लालिमा धारण कर लेती है. लोरमी के व्यापारी पुत्र शीला और स्थानीय नेता पुत्र आशु की दिलचस्पी भी पान की दुकान में रिंकु को एक नजर देख लेने की है.
अब फ़िल्म को एक पाठ की तरह देखते हैं. यह फ़िल्म जीवन के एकाकी, मां की ममता से वंचित एक युवा की कहानी है. इस युवक को प्रेम की तलाश है. पिता शराब पीता है. बिल्लू बचपन में डीएफओ की बेटे की तरह हैप्पी बर्थ डे मनाने का शौक रखता है. उसके पिता इन्हीं सब जिद्द की वजह से बिल्लू को साहब के घर नहीं ले जाते. बचपन जीवन का एक ऐसा दौर है जिसमें वह दुनिया को समान दृष्टि से देखता है. उसे साहब और चपरासी का अंतर पता नहीं होता. बचपन मनुष्य मात्र को समान देखने की सर्जनात्मक नजर का नाम है. बिल्लू की इस नजर का उसके पिता के लिए भी मायने है पर वह मजबूर है. बचपन की उम्मीदें अब युवा काल में रूप बदलने लगती है. पिता के ज़िद्द में बिल्लू वन विभाग की चौकीदारी स्वीकार कर लेता है. पर वह इसे अपनी इच्छा के विरुद्ध मानकर पहचान बनाने की सोचता है और पिता के विरुद्ध जाकर पान की दुकान खोल लेता है.
चमनबहार का दर्शक होने के लिए प्रेमी मन का होना बेहद जरूरी है. जो भी दर्शक अपने जवानी की रंगीनियत को मन में न मारकर जीवन में उतारा होगा. जवानी को शिद्दत से जिया होगा.अपने सपनों की राजकुमारी के बारे में न सिर्फ सोचा होगा बल्कि उसे पाने के लिए जीवंत प्रयत्न किया होगा वह 'चमनबहार' से निकलने वाली आग और उसकी ठंडक को महसूस कर सकता है. प्रेम अग्नि है तो जलधार भी. बिल्लू का पूरा प्रयास चाहे वह शीला और आशु के दबंग रूप के सामने भी अपने प्रेम को बचा पाने की सोच हो या दोनों हंसोड़ डैडी के कैरम क्लब को ध्वस्त करवाने की.अंग्रेजी शिक्षक के प्रति रोष हो या डीएफओ के बिच्छू छाप जैकेट पहनने वाले बेटे को पानठेले से हटाने की. हर जगह बिल्लू अपनी सहज बुद्धि से यह कहते दिखता है-" मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है!"
हर वह स्थल जहां रिंकू को एक नजर भी देखने का अवसर मिल जाय बिल्लू नहीं छोड़ना चाहता. यह अवसर वह किसी भी कीमत पर सामूहिक नहीं बनने देने की बलवती इच्छा रखता है. इसीलिए कई अवसर पर जब रिंकू अपने कुत्ते रुबी को घुमाने ले जाती है तब बिल्लू हर तरह से यह प्रयास करता है कि बाकी युवकों का मुख उनके तरफ रहें ताकि वह अकेला रिंकू को निहार सकें. प्रेम का सबसे बड़ा मूल्य एकांत का वैभव है. प्रेमी और प्रेमपात्र के अलावा कोई तीसरा नहीं.
'चमनबहार ' फ़िल्म के हीरो बिल्लू से लेकर स्कूली छात्र , आशु,शीला, दोनों डैडी और अनाम लड़के की आंतरिक बनावट और उमंग उन्हें एक धरातल प्रदान करती है. वह धरातल है-प्रेम की तलाश. इन्हें आप आवारा कहें...लफंगा कहें या कोई और सम्बोधन, लेकिन हम सब जीवन के सबसे खूबसूरत एहसास के दौर में चमनबहार के भाव से गुजरते हैं. जो नहीं गुजरे वे अभागे हैं या झूठे. फिल्म में रिंकु जब-जब इंट्री करती है तब मुझे आलोक धन्वा के शब्द दिखाई देते हैं-
अब भी
छतों पर आती हैं लड़कियाँ
मेरी ज़िंदगी पर पड़ती हैं उनकी परछाइयाँ.
गो कि लड़कियाँ आयी हैं उन लड़कों के लिए
जो नीचे गलियों में ताश खेल रहे हैं
नाले के ऊपर बनी सीढियों पर और
फ़ुटपाथ के खुले चायख़ानों की बेंचों पर
चाय पी रहे हैं
उस लड़के को घेर कर
जो बहुत मीठा बजा रहा है माउथ ऑर्गन पर
आवारा और श्री 420 की अमर धुनें
पत्रिकाओं की एक ज़मीन पर बिछी दुकान
सामने खड़े-खड़े कुछ नौजवान अख़बार भी पढ़ रहे हैं.
उनमें सभी छात्र नहीं हैं
कुछ बेरोज़गार हैं और कुछ नौकरीपेशा,
और कुछ लफंगे भी
लेकिन उन सभी के ख़ून में
इंतज़ार है एक लड़की का !
उन्हें उम्मीद है उन घरों और उन छतों से
किसी शाम प्यार आयेगा !"
प्रेम के आ जाने का इंतजार इस फ़िल्म को विश्वसनीय बनाता है.
स्थानीय राजनीति की दबंगई आशु के चरित्र को आगे बढ़ाती है. हर स्थिति को वे अपनी माँ के साथ मिलकर अवसर में बदलना जानता है. शीला व्यापारी है लेकिन उसकी भी पृष्ठभूमि में राजनीति है. दोनों डैडी अभाव में भी जीवन के मजे लेना जानते हैं. बिल्लू का पिता दुनियादार बुद्धि का मालिक है. वह अपने एक संवाद में प्रशासनिक तंत्र का राज खोलता है. बिल्लू पूछता है क्या फूट डालो और राज करो की नीति प्रासंगिक है. तब उनके पिता कहते हैं- कान भरो और राज करो. प्रशासनिक अमले के पदसोपान के हर स्तर पर यह वाक्य सच दिखता है. प्रामाणिकता और सहजता के लिहाज से बिल्लू के पिता का कोई जवाब नहीं. ये सभी पात्र मानवीय हैं. अनेक पात्रों के साथ दोनों डैडी भाचा, तनतन,पगले ,बे साले जैसे बिलासपुरिया हिंदी में छत्तीसगढ़ी के फ़्यूजन को अपने चरित्र में दर्शाते हैं. छत्तीसगढ़ी लोकसंगीत की बानगी के साथ रॉक का फ़्यूजन युवा मन के उमंग को बेहतरीन ढंग से प्रगट करता है.
प्रेम के लिए हर रास्ता अपनाने के लिए तैयार बिल्लू की पान की दुकान और उसके व्यक्तित्व को इलाके का थानेदार पीटकर रौंद देता है. बेदम पिटाई के बाद कोई बिल्लू को कोई भी आवारा और समाज विरोधी चरित्र कह सकता है. उसे लड़की के इज्जत को नोटों पर लिखकर बेचने वाला कहकर गालियां दे सकता है, बावजूद यह सब विश्वसनीय लगता है क्योंकि वह प्रेम में है. भले ही हम इस प्रेम को एकतरफा कह दें. लेकिन दिल लगाने के लिए कोई नियमावली और अधिकार तंत्र थोड़े ही है. दिल का मामला नैसर्गिक है.
बिल्लू को इंजीनियर साहब जेल से निकलवाता है. बिल्लू कृतज्ञता ज्ञापित करने इंजीनियर के घर जाता है. वहां दो मार्मिक घटनाएं दृश्य रूप में घटित होती है. प्रथम बिल्लू ध्यान से इंजीनियर साहब और उसके परिवारजनों की तस्वीरों को देखता है. इन तस्वीरों में मां, पिता ,भाई,बहन पूरा भरा- पूरा परिवार है. आगे एक फोटो रिंकू की दिखती है. इस दृश्य में सहज बुद्धि वाला दर्शक भी महसूस करेगा कि बिल्लू के मन में प्रेम का अभाव है. इसका एक रुप मां है तो दूसरा प्रेमिका है.
दूसरा दृश्य वह है जिसमें रिंकू परदे के पीछे से बिल्लू को समभाव से देख रही है. ऐसा महसूस होता है कि बिल्लू के प्रति उसके मन में प्रेम का उदय हो चुका है. रिंकू चाय लेकर आती है और बिल्लू के सामने रख देती है. बिल्लू पश्चाताप से सिर नीचे कर लेता है. वह रिंकू की प्रिय चॉकलेट डेरी मिल्क टेबल में रखकर हारे हुए सिपाही की तरह बाहर की तरफ भागता है. सड़क पर आने के बाद उसकी मुखाकृति और शारीरिक हाव-भाव प्रेम की असफलता को दर्शाते हैं. माहौल पूरी तरह से दर्द से भर उठता है. यह दृश्य फ़िल्म की जान है जो कस्बाई युवक की ईमानदारी और उसके निश्चल पश्चताप को प्रकट करता है.यह फ़िल्म यथार्थवादी रूप का परिचायक है.
फ़िल्म में बिल्लू का जीवन यहां उजाड़ से भरा महसूस होने लगता है. फ़िल्म में हीरोइन लोरमी छोड़ चुकी है और दर्शक को लगता है कोई सकारात्मक हो तो बात बनें. कोई अति उत्साही लेखक और निर्देशक होता तो हीरो को बिलासपुर पहुंचा कर मिलन करवा देता. गाना बज उठता और हीरो-हीरोइन के मिलन समारोह में नृत्य भी हो जाता. लेकिन इसी पाइंट पर अपूर्व की दक्षता दिखाई देती है जो अपूर्व है.
रिंकू के चले जाने के बाद बिल्लू एक बार फिर खाली पड़े बंगले में जाता है. तेज हवा के बीच एक पेज उड़ते हुए आता है जिसके अगले भाग में विषय संबंधी चित्र होता है. अब फ़िल्म का क्लाइमेक्स आता है जब पेज के पिछले हिस्से में बिल्लू सहित पान ठेले का स्केच बना होता है. ये स्केच ही फ़िल्म की आत्मा है. रिंकू कुछ नहीं कहती... लेकिन स्केच सब कुछ कह देता है. प्रेम पर यकीन करते हैं तो फिल्म को अवश्य देखिए.नफरत के इस खौफानाक दौर में आपको अच्छा लगेगा.
बहस में चमन बहार
आंचलिकता के नाम पर ठूंस दिए जाने वाले सस्ते,फूहड़ नाच-गाने से भी बचा गया है,जिसके खतरे इसमें सबसे ज्यादा थे.सफलता के नाम पर इस नकलीपन,सतहीपन से ज्यादातर छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्देशक अभी-भी से उबर नहीं पाए हैं. इस अर्थ में यह उनसे अपनी बिल्कुल अलग, यथार्थवादी और विश्वसनीय पहचान बनाती है.भविष्य के सिनेमा का यह एक सशक्त नाम होने की उम्मीद दिलाता है--अगर बाजारवादी प्रपंचों से बच सकें.
कैलाश बनवासी
नेट फ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर बहसों का दौर चल पड़ा है. यह फिल्म जब देखी तो कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी औसत चंद फार्मूले से लैस फिल्म इतनी बहस तलब हो जाएगी. 'नेट फ्लिक्स' या 'अमेज़न प्राइम' जैसे मीडिया समूह आज सिनेमा या सीरिज के नए स्थापित हो चुके कॉर्पोरेट घराने हैं.जिन्हें फिल्म से उतना ही वास्ता है जितना सिनेमाघर के मालिक को मुनाफे से रहता है. इस फिल्म की एक मित्र से प्रसंशा सुनकर भी इसे देखने का मन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस माध्यम में हिट करने के लिए जैसी सेंसरहीन नग्नता,अश्लीलता, हिंसा, अपराध की अतिरंजना या अराजकता परोसी जा रही है,वह अपने ही देश की बहुत भयानक और अराजक छवि पेश करती है,जो ऐसी विकृतियों को बढ़ावा देती है,जिसके प्रेरणास्रोत ‘गैंग्स ऑफ़ वासेपुर’या ‘बदलापुर’ जैसी घोर आपराधिक,हिंसा और सेक्स और विकृतियों को हाईलाइट करने वाली या बढ़ावा देने वाली हिट’ फ़िल्में रही हैं.
बहरहाल, ‘चमन-बहार’
इस फिल्म को देखने के बाद कुछ निराशाओं ने जन्म लिया. इसलिए कुछ ज्यादा कि यह छत्तीसगढ़ के कस्बाई पृष्ठभूमि पर कही गई कहानी है,लेकिन यह उस आंचलिक सौंधेपन से वंचित है जो यहाँ की संस्कृति की खासियत रही है.जिसमें प्रसिद्ध नाटककार हबीब तनवीर के ज्यादातर नाटक रचे-बसे-पगे हैं. फिल्म देखकर यह तो समझ आया,कि नए निर्देशक की बहुत सफल हो जाने वाली फिल्म बना लेने के बाद भी उसकी दृष्टि में कितनी ही कमियां हैं. मैं निर्देशक से “पथेर पांचाली’ या ‘पार’ या’ गमन’,’मंथन’ जैसी फिल्म की उम्मीद कतई नहीं कर रहा. यहाँ निर्देशक का लोरमी की जमीन से जुड़ाव उसके महज मुंगेली के नए जिले बन जाने की औचकताओं और रोचकताओं तक ही सीमित है. यदि इन जाने-पहचाने नामों की बात छोड़ दी जाये तो यह किसी भी सामान्य कसबे की कहानी हो सकती है. यह निर्देशक की इस अंचल की खासियत को न समझ पाने की चूक है. कुछ किरदार बस हलके-फुल्के से आभास कराते हैं इसकी क्षेत्रीयता का.मैं यहाँ क्षेत्रीयता की वकालत नहीं कर रहा,बल्कि उस सादगी भरे‘छत्तीसगढ़ियापन’ की वकालत कर रहा हूँ जो यहाँ के लोगों के संस्कारों में, नैतिकताओं में यह साँस लेता है, और जिसके सबसे बड़े साहित्यिक प्रतिनिधि कवि-उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल हैं .इसे इस फिल्म को आंचलिकता के नकार के रूप में भी व्याख्यायित की जा सकती है.
फिल्म में बिल्लू एक बहुत सामान्य युवा का किरदार है,जिसकी कोई बहुत महत्वाकांक्षा भी नहीं है. वह नए जिला बने लोरमी के एक मुख्य मार्ग पर अपना पान ठेला खोलता है. इसके पहले वह वन विभाग की नौकरी इसलिए छोड़ चुका है कि एक रात उसका सामना भालू से हो जाता है.वह बेमौत मरना नहीं चाहता. उसका पान ठेला उस वीराने रास्ते पर है --नितांत अकेली दुकान. सामने पुराना जीर्ण-शीर्ण सा सरकारी क्वार्टर है.दुकान में ग्राहकों का टोटा है. पानठेला यों भी नई उम्र के शोहदों,लफुटों का अड्डा होता है. बिना इनके इनकी दुकानदारी नहीं चल सकती. यह सुयोग तब बनता है जब सामने के क्वार्टर में जल संसाधन विभाग के एक छोटे अधिकारी यहाँ रहने आते हैं.इस परिवार में पति-पत्नी के अलावा एक हाई स्कूल पढने वाली बेटी और प्रायमरी क्लास पढनेवाला छोटा बेटा है. साथ एक पैमेरियन--’रूबी’.इस परिवार के आने के बाद कैसे यहाँ का माहौल बदलता है,शहर के लफंगों का अड्डा बन जाता है,यह फिल्म की दूसरी मुख्य कथावस्तु है. तो पहली क्या है? फिल्म की पहली मुख्य कथा-वस्तु है--एक साधारण से लड़के का उस अधिकारी की लड़की के प्रति पनपता प्रेम.जबकि ज्यादातर जो वहां लड़के हैं आवारा हैं,जो अपनी दबंगई या रुतबे से उसे ‘फंसाना’ चाहते हैं. फिल्म इन्हीं दो बिन्दुओं पर केन्द्रित है. कसबे के आवारा लडकों के संस्कार कैसे रहेंगे,यह कोई नयी चीज नहीं दिखा रहा है निर्देशक.वे आवारा सैकड़ों मसाला फिल्मों में देखे गए लफंगों से तनिक अलग नहीं है. अब बात यहाँ स्त्री-विमर्श या पितृसत्तात्म्क चरित्र को बढ़ावा देने की की जा रही है. तो मनोविज्ञान के अनुसार यह आकर्षण कुछ इस वय का है,और कुछ समाज में हावी उन्हीं पतनशील पितृसत्तात्मक सोच का,जो लोगों के दिल-दिमाग में जमाने से बैठा हुआ है,जिसके खिलाफ संघर्ष आज भी जारी है. लेकिन कहानी में चित्रित कस्बा उतना ही आदिम और पिछड़ा है जितना देश में हमारे शिक्षा,स्वास्थ्य,सामाजिक-सुरक्षा के बुनियादी मुद्दे. फिल्म में मुझे यह लड़कों का चरित्र नहीं,बल्कि कस्बे का.उसकी आबो-हवा का चरित्र ज्यदा लगा है,जो बड़े नामालूम ढंग से उनके रूह में,खून में शामिल हो चुका है,और वे लड़की पर अपना कब्जा या एकाधिकार अपनी विजय के रूप में देखते हैं.
इसे देखते हुए मुझे अपनी 90-91 में लिखी कहानी ‘डायरी खबर और सपने’ का रह-रहकर स्मरण आता रहा. इसलिए कि वह भी ऐसे ही कसबाई मुहल्ले में, ऐसे ही एक निम्नवर्गीय लड़के के एक मध्यवर्गीय घर की खूबसूरत लड़की से पनपते किशोर-प्रेम की कहानी है.यह मेरी बहुत प्रिय कहानियों में से एक है. जब इनके दृश्यों को देखा तो वह कहानी अपनेआप मेरे सामने आ गयी,जिसमें मोहल्ले के लडकों के ऐसे ही चरित्र को उकेरा गया है. उस कहानी का यह पैराग्राफ देखिये--
मैं देखता हूँ,तुम जब से इस मुहल्ले में आई हो,यह पिछड़ा और उपेक्षित मोहल्ला रौनकदार हो गया है.नए उम्र के छोकरों की तो छोड़ो,पकी उम्र वाले भी तुम पर नजर जमाये रहते हैं. तुम्हारे घर के सामने लेटेस्ट फ़ैशन का बाज़ार चलता है,जो रोज़-ब रोज़ बदलता है,जिसे तुमने ज़रूर देखा होगा.यहाँ का सब कुछ चमकदार और रंगीन है—जाँघिये से लेकर रुमाल तक!शाम होते ही इन लड़कों का यहाँ मजमा लगता है. उस नीली रोशनी वाले खम्भे के नीचे,जो तुम्हारे मकान से बस इतनी दूरी पर है कि वहाँ से तुम आकर्षक लगती रहो और इधर हम.सबके सब हँसते हैं,गाते हैं,लड़ते हैं. इसलिए कि हम आशिक हैं,और अभी अधीर,उन्मादी और हत्यारे प्रेमी में तब्दील नहीं हुए हैं.फिर भी लड़ाई तो है.हम सबको विश्वास है कि तुम केवल ‘उसी’ पर मरती हो.
मैं भी उन्हीं में से एक हूँ.
यह मनीष है,जो सबसे ज्यादा चक्कर लगता है तुम्हारे घर के,कोल्हू के बैल की तरह,और आज तक ऊबा नहीं है.उसने सबको बता रखा है कि तुम उसे रोज़ हंसकर ‘फ्लाइंग किस’ देती हो...
वह राजेन्द्र,जिसने संजय दत्त की हेयर स्टाइल रखी है,कहता है—वो तो रोज़ स्कूल जाते हुए मुझे ‘विश’करके जाती है...
और मुकेश,जिसके जोड़ का मुहल्ले में कोई डांसर नहीं है,उस साले ने यहाँ तक बता दिया है कि उसने तुम्हें एक बार चूमा है...
विपिन को यह हिसाब करना मुश्किल है कि उसके साथ ‘यामहा’ पर तुम कितनी बार होटल गयी हो और कितनी बार पिक्चर...
दरअसल यहाँ इस जमावड़े के बहाने निर्देशक नायक और बाकी लडकों के द्वंद्व को दर्शाया है.जहां बिल्लू उस पर प्रेम की चाह से खींच रहा है,तो बाकी अपने मर्द या लड़के होने के गौरव बोध से. यह जर्रोर है अपनी असफलता से वह उस अपराध को अंजाम दे देता है,जो उसके चरित्र में नहीं है—दीवालों में नोट में ‘रिंकू नानेरिया बेवफा है’ लिखकर.’यह अपराध उसने कुंठित होकर किया है.यह सच है,इस फिल्म में बिल्लू और कुछ लफंगों—शीला,आशु या पुलिस इंस्पेक्टर जैसों को छोड़ किसी चरित्र को निर्देशकीय पकड़ नहीं दी गयी है.सबमें एक ढीला-ढालापन है. कहानी की गति बहुत धीमी है. कितना ज्यादा समय सड़कों पर लड़की को स्कूटी चलाते,या कुत्ता घुमाते दिखाया गया है. नायिका या लड़की को हद से ज्यादा चुप रखा गया है,जो आजकल की बिंदास लड़की से कतई मेल नहीं खाता. इन बरसों में लडकियाँ बहुत सशक्त हुई हैं—हर क्षेत्र में. ज्यादतर इलाकों में उनका यह कस्बाई अबोधपन गायब हो चुका है. इसीलिए इसी बिंदु पर फिल्म की सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है. रही बात प्रेम के धीरे-धीरे पनपने की,तो उसका भी यहाँ अवसर नहीं है. उस परिवार के चले जाने के बाद संयोग से लड़के के हाथ लगे एक गुलाबी कागज़ में बना ठेलेवाले बिल्लू का स्केच ही रिंकू की तरफ से इसका नामालूम-सा संकेत है,जो उस लड़के के लिए सबसे बड़ी आश्वस्ति और सबसे बड़ी पूंजी है. यहाँ युवा निर्देशक ने प्रेम की इस जरा-सी स्वीकृति को जिस कोमलता और खूबसूरती से एक छोटे से क्षण में दर्शाया है,उससे मुझे प्रसिद्ध ईरानी फिल्मकार माजिद मजीदी की फिल्म ‘बरान’ ( बारिश) की याद दिला गयी. संयोग देखिये,कि उस पूरी फिल्म में भी किशोर नायिका का एक भी संवाद नहीं है.और बिलकुल इसी तरह सबसे आखिर में विदाई के क्षणों में वह किशोर नायक को अपने प्रेम की धुंधली-सी मौन स्वीकृति देती है—कोई मिनट भर अपनी प्रेममयी आँखों से उसे देखते हुए. प्रेम की ऐसी नामालूम अभिव्यक्ति या स्वीकारोक्ति उस जैसे नामहीन साधारण लड़के के लिए जैसा मूल्यवान है ,वह तो प्रेम में डूबे ऐसे लोग ही जान पायेंगे. जिसे मीरा भी जीवन भर कहती रही है—ए री मैं तो प्रेम दीवानी,मेरो दरद न जाने कोय...
इस बहुत सहज फिल्म में अपूर्वधर बड़गैया की निर्देशकीय प्रतिभा के कुछ दृश्य अविस्मर्णीय हैं. बुलेट भड़भड़ाते पुलिस इंस्पेक्टर भगवान तिवारी घोर विश्वसनीय पुलिसवाले लगे हैं. एक दृश्य को भुला पाना मुश्किल है जो उनके बहुत संभावनाशील निर्देशकीय क्षमता का पता देती है. उसके ठेले को तहस-नहस कर दिए जाने के बाद बिल्लू का अपने ठेले पर वापस आकर उसकी दुर्गति देखने का दृश्य. उस तबाह ,टूटे-फूटे ठेले और लावारिस पड़े बिखरे सामानों के दृश्य से एक बार फिर सत्ता के निरंकुश चरित्र को बिना कुछ कहे उजागर कर देता है.या कस्बे के हाट-बाजारों,सडकों या तालाबों के पार में टाइटल दिखाना भी बिलकुल अभिनव प्रयोग है. छत्तीसगढ़ के पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म का संगीत यहाँ के मिजाज से बिलकुल मेल नहीं खाता.यह किसी पॉप-कल्चर फिल्म के गीत-संगीत सा लगता है,जो सुनने में भी चुभता है.जबकि इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया संभावनाएं थीं.
अभी प्रचलित फिल्मों के साथ इस फिल्म को देखने पर यह बिलकुल अलग जोनर की फिल्म बनायी गयी है. यहाँ बात-बात में हत्या,नग्नता,बलात्कार,हिंसा,मानसिक विकृति इत्यादि वेब-सिरिजी फार्मूले से हटकर निर्देशक ने साधारण लोगों के जीवन की साधारण सी कहानी पर एक साफ़-सुथरी फिल्म बनाने की कोशिश की है,जिसके इस पक्ष की प्रसंशा होनी चाहिए.भले ही इसमें आंचलिकता की,लोकेल की वह गंध नदारद है,जिसकी चर्चा ऊपर कर चुका हूँ,लेकिन यह उस आंचलिकता के नाम पर ठूंस दिए जाने वाले सस्ते,फूहड़ नाच-गाने से भी बचा गया है,जिसके खतरे इसमें सबसे ज्यादा थे.सफलता के नाम पर इस नकलीपन,सतहीपन से ज्यादातर छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्देशक अभी-भी से उबर नहीं पाए हैं. इस अर्थ में यह उनसे अपनी बिल्कुल अलग, यथार्थवादी और विश्वसनीय पहचान बनाती है.भविष्य के सिनेमा का यह एक सशक्त नाम होने की उम्मीद दिलाता है--अगर बाजारवादी प्रपंचों से बच सकें।
41, मुखर्जी नगर,सिकोला भाठा,दुर्ग
मोबाइल नंबर- 9827993920









.jpg)
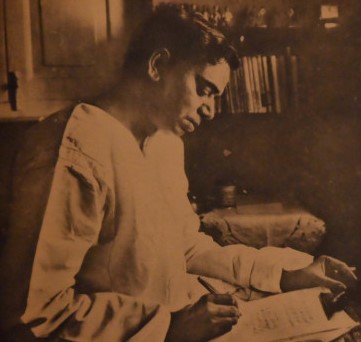






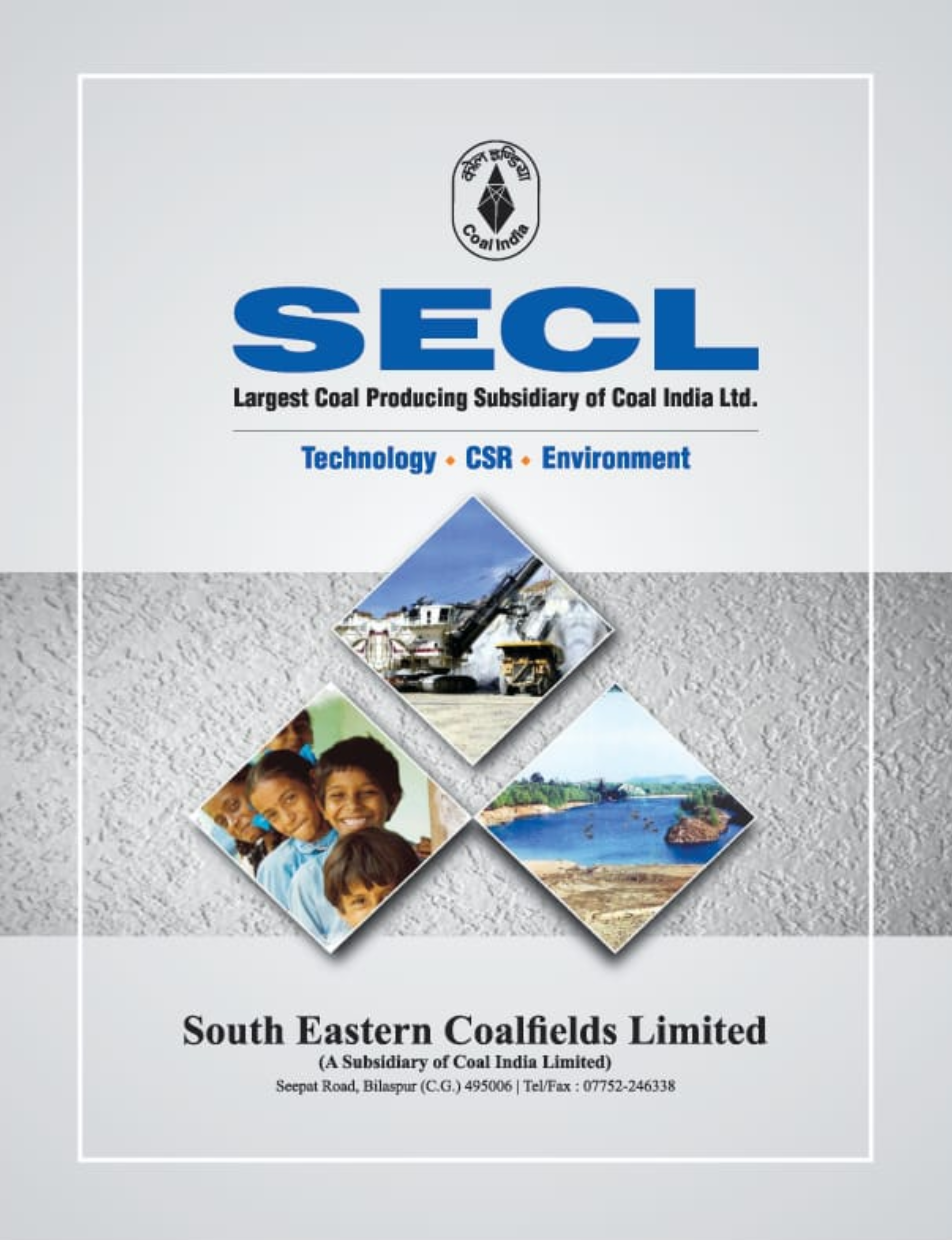












.jpg)









