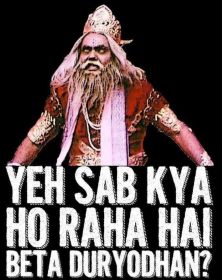फिल्म

बहस में चमन बहार
आंचलिकता के नाम पर ठूंस दिए जाने वाले सस्ते,फूहड़ नाच-गाने से भी बचा गया है,जिसके खतरे इसमें सबसे ज्यादा थे.सफलता के नाम पर इस नकलीपन,सतहीपन से ज्यादातर छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्देशक अभी-भी से उबर नहीं पाए हैं. इस अर्थ में यह उनसे अपनी बिल्कुल अलग, यथार्थवादी और विश्वसनीय पहचान बनाती है.भविष्य के सिनेमा का यह एक सशक्त नाम होने की उम्मीद दिलाता है--अगर बाजारवादी प्रपंचों से बच सकें.
कैलाश बनवासी
नेट फ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर बहसों का दौर चल पड़ा है. यह फिल्म जब देखी तो कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी औसत चंद फार्मूले से लैस फिल्म इतनी बहस तलब हो जाएगी. 'नेट फ्लिक्स' या 'अमेज़न प्राइम' जैसे मीडिया समूह आज सिनेमा या सीरिज के नए स्थापित हो चुके कॉर्पोरेट घराने हैं.जिन्हें फिल्म से उतना ही वास्ता है जितना सिनेमाघर के मालिक को मुनाफे से रहता है. इस फिल्म की एक मित्र से प्रसंशा सुनकर भी इसे देखने का मन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस माध्यम में हिट करने के लिए जैसी सेंसरहीन नग्नता,अश्लीलता, हिंसा, अपराध की अतिरंजना या अराजकता परोसी जा रही है,वह अपने ही देश की बहुत भयानक और अराजक छवि पेश करती है,जो ऐसी विकृतियों को बढ़ावा देती है,जिसके प्रेरणास्रोत ‘गैंग्स ऑफ़ वासेपुर’या ‘बदलापुर’ जैसी घोर आपराधिक,हिंसा और सेक्स और विकृतियों को हाईलाइट करने वाली या बढ़ावा देने वाली हिट’ फ़िल्में रही हैं.
बहरहाल, ‘चमन-बहार’
इस फिल्म को देखने के बाद कुछ निराशाओं ने जन्म लिया. इसलिए कुछ ज्यादा कि यह छत्तीसगढ़ के कस्बाई पृष्ठभूमि पर कही गई कहानी है,लेकिन यह उस आंचलिक सौंधेपन से वंचित है जो यहाँ की संस्कृति की खासियत रही है.जिसमें प्रसिद्ध नाटककार हबीब तनवीर के ज्यादातर नाटक रचे-बसे-पगे हैं. फिल्म देखकर यह तो समझ आया,कि नए निर्देशक की बहुत सफल हो जाने वाली फिल्म बना लेने के बाद भी उसकी दृष्टि में कितनी ही कमियां हैं. मैं निर्देशक से “पथेर पांचाली’ या ‘पार’ या’ गमन’,’मंथन’ जैसी फिल्म की उम्मीद कतई नहीं कर रहा. यहाँ निर्देशक का लोरमी की जमीन से जुड़ाव उसके महज मुंगेली के नए जिले बन जाने की औचकताओं और रोचकताओं तक ही सीमित है. यदि इन जाने-पहचाने नामों की बात छोड़ दी जाये तो यह किसी भी सामान्य कसबे की कहानी हो सकती है. यह निर्देशक की इस अंचल की खासियत को न समझ पाने की चूक है. कुछ किरदार बस हलके-फुल्के से आभास कराते हैं इसकी क्षेत्रीयता का.मैं यहाँ क्षेत्रीयता की वकालत नहीं कर रहा,बल्कि उस सादगी भरे‘छत्तीसगढ़ियापन’ की वकालत कर रहा हूँ जो यहाँ के लोगों के संस्कारों में, नैतिकताओं में यह साँस लेता है, और जिसके सबसे बड़े साहित्यिक प्रतिनिधि कवि-उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल हैं .इसे इस फिल्म को आंचलिकता के नकार के रूप में भी व्याख्यायित की जा सकती है.
फिल्म में बिल्लू एक बहुत सामान्य युवा का किरदार है,जिसकी कोई बहुत महत्वाकांक्षा भी नहीं है. वह नए जिला बने लोरमी के एक मुख्य मार्ग पर अपना पान ठेला खोलता है. इसके पहले वह वन विभाग की नौकरी इसलिए छोड़ चुका है कि एक रात उसका सामना भालू से हो जाता है.वह बेमौत मरना नहीं चाहता. उसका पान ठेला उस वीराने रास्ते पर है --नितांत अकेली दुकान. सामने पुराना जीर्ण-शीर्ण सा सरकारी क्वार्टर है.दुकान में ग्राहकों का टोटा है. पानठेला यों भी नई उम्र के शोहदों,लफुटों का अड्डा होता है. बिना इनके इनकी दुकानदारी नहीं चल सकती. यह सुयोग तब बनता है जब सामने के क्वार्टर में जल संसाधन विभाग के एक छोटे अधिकारी यहाँ रहने आते हैं.इस परिवार में पति-पत्नी के अलावा एक हाई स्कूल पढने वाली बेटी और प्रायमरी क्लास पढनेवाला छोटा बेटा है. साथ एक पैमेरियन--’रूबी’.इस परिवार के आने के बाद कैसे यहाँ का माहौल बदलता है,शहर के लफंगों का अड्डा बन जाता है,यह फिल्म की दूसरी मुख्य कथावस्तु है. तो पहली क्या है? फिल्म की पहली मुख्य कथा-वस्तु है--एक साधारण से लड़के का उस अधिकारी की लड़की के प्रति पनपता प्रेम.जबकि ज्यादातर जो वहां लड़के हैं आवारा हैं,जो अपनी दबंगई या रुतबे से उसे ‘फंसाना’ चाहते हैं. फिल्म इन्हीं दो बिन्दुओं पर केन्द्रित है. कसबे के आवारा लडकों के संस्कार कैसे रहेंगे,यह कोई नयी चीज नहीं दिखा रहा है निर्देशक.वे आवारा सैकड़ों मसाला फिल्मों में देखे गए लफंगों से तनिक अलग नहीं है. अब बात यहाँ स्त्री-विमर्श या पितृसत्तात्म्क चरित्र को बढ़ावा देने की की जा रही है. तो मनोविज्ञान के अनुसार यह आकर्षण कुछ इस वय का है,और कुछ समाज में हावी उन्हीं पतनशील पितृसत्तात्मक सोच का,जो लोगों के दिल-दिमाग में जमाने से बैठा हुआ है,जिसके खिलाफ संघर्ष आज भी जारी है. लेकिन कहानी में चित्रित कस्बा उतना ही आदिम और पिछड़ा है जितना देश में हमारे शिक्षा,स्वास्थ्य,सामाजिक-सुरक्षा के बुनियादी मुद्दे. फिल्म में मुझे यह लड़कों का चरित्र नहीं,बल्कि कस्बे का.उसकी आबो-हवा का चरित्र ज्यदा लगा है,जो बड़े नामालूम ढंग से उनके रूह में,खून में शामिल हो चुका है,और वे लड़की पर अपना कब्जा या एकाधिकार अपनी विजय के रूप में देखते हैं.
इसे देखते हुए मुझे अपनी 90-91 में लिखी कहानी ‘डायरी खबर और सपने’ का रह-रहकर स्मरण आता रहा. इसलिए कि वह भी ऐसे ही कसबाई मुहल्ले में, ऐसे ही एक निम्नवर्गीय लड़के के एक मध्यवर्गीय घर की खूबसूरत लड़की से पनपते किशोर-प्रेम की कहानी है.यह मेरी बहुत प्रिय कहानियों में से एक है. जब इनके दृश्यों को देखा तो वह कहानी अपनेआप मेरे सामने आ गयी,जिसमें मोहल्ले के लडकों के ऐसे ही चरित्र को उकेरा गया है. उस कहानी का यह पैराग्राफ देखिये--
मैं देखता हूँ,तुम जब से इस मुहल्ले में आई हो,यह पिछड़ा और उपेक्षित मोहल्ला रौनकदार हो गया है.नए उम्र के छोकरों की तो छोड़ो,पकी उम्र वाले भी तुम पर नजर जमाये रहते हैं. तुम्हारे घर के सामने लेटेस्ट फ़ैशन का बाज़ार चलता है,जो रोज़-ब रोज़ बदलता है,जिसे तुमने ज़रूर देखा होगा.यहाँ का सब कुछ चमकदार और रंगीन है—जाँघिये से लेकर रुमाल तक!शाम होते ही इन लड़कों का यहाँ मजमा लगता है. उस नीली रोशनी वाले खम्भे के नीचे,जो तुम्हारे मकान से बस इतनी दूरी पर है कि वहाँ से तुम आकर्षक लगती रहो और इधर हम.सबके सब हँसते हैं,गाते हैं,लड़ते हैं. इसलिए कि हम आशिक हैं,और अभी अधीर,उन्मादी और हत्यारे प्रेमी में तब्दील नहीं हुए हैं.फिर भी लड़ाई तो है.हम सबको विश्वास है कि तुम केवल ‘उसी’ पर मरती हो.
मैं भी उन्हीं में से एक हूँ.
यह मनीष है,जो सबसे ज्यादा चक्कर लगता है तुम्हारे घर के,कोल्हू के बैल की तरह,और आज तक ऊबा नहीं है.उसने सबको बता रखा है कि तुम उसे रोज़ हंसकर ‘फ्लाइंग किस’ देती हो...
वह राजेन्द्र,जिसने संजय दत्त की हेयर स्टाइल रखी है,कहता है—वो तो रोज़ स्कूल जाते हुए मुझे ‘विश’करके जाती है...
और मुकेश,जिसके जोड़ का मुहल्ले में कोई डांसर नहीं है,उस साले ने यहाँ तक बता दिया है कि उसने तुम्हें एक बार चूमा है...
विपिन को यह हिसाब करना मुश्किल है कि उसके साथ ‘यामहा’ पर तुम कितनी बार होटल गयी हो और कितनी बार पिक्चर...
दरअसल यहाँ इस जमावड़े के बहाने निर्देशक नायक और बाकी लडकों के द्वंद्व को दर्शाया है.जहां बिल्लू उस पर प्रेम की चाह से खींच रहा है,तो बाकी अपने मर्द या लड़के होने के गौरव बोध से. यह जर्रोर है अपनी असफलता से वह उस अपराध को अंजाम दे देता है,जो उसके चरित्र में नहीं है—दीवालों में नोट में ‘रिंकू नानेरिया बेवफा है’ लिखकर.’यह अपराध उसने कुंठित होकर किया है.यह सच है,इस फिल्म में बिल्लू और कुछ लफंगों—शीला,आशु या पुलिस इंस्पेक्टर जैसों को छोड़ किसी चरित्र को निर्देशकीय पकड़ नहीं दी गयी है.सबमें एक ढीला-ढालापन है. कहानी की गति बहुत धीमी है. कितना ज्यादा समय सड़कों पर लड़की को स्कूटी चलाते,या कुत्ता घुमाते दिखाया गया है. नायिका या लड़की को हद से ज्यादा चुप रखा गया है,जो आजकल की बिंदास लड़की से कतई मेल नहीं खाता. इन बरसों में लडकियाँ बहुत सशक्त हुई हैं—हर क्षेत्र में. ज्यादतर इलाकों में उनका यह कस्बाई अबोधपन गायब हो चुका है. इसीलिए इसी बिंदु पर फिल्म की सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है. रही बात प्रेम के धीरे-धीरे पनपने की,तो उसका भी यहाँ अवसर नहीं है. उस परिवार के चले जाने के बाद संयोग से लड़के के हाथ लगे एक गुलाबी कागज़ में बना ठेलेवाले बिल्लू का स्केच ही रिंकू की तरफ से इसका नामालूम-सा संकेत है,जो उस लड़के के लिए सबसे बड़ी आश्वस्ति और सबसे बड़ी पूंजी है. यहाँ युवा निर्देशक ने प्रेम की इस जरा-सी स्वीकृति को जिस कोमलता और खूबसूरती से एक छोटे से क्षण में दर्शाया है,उससे मुझे प्रसिद्ध ईरानी फिल्मकार माजिद मजीदी की फिल्म ‘बरान’ ( बारिश) की याद दिला गयी. संयोग देखिये,कि उस पूरी फिल्म में भी किशोर नायिका का एक भी संवाद नहीं है.और बिलकुल इसी तरह सबसे आखिर में विदाई के क्षणों में वह किशोर नायक को अपने प्रेम की धुंधली-सी मौन स्वीकृति देती है—कोई मिनट भर अपनी प्रेममयी आँखों से उसे देखते हुए. प्रेम की ऐसी नामालूम अभिव्यक्ति या स्वीकारोक्ति उस जैसे नामहीन साधारण लड़के के लिए जैसा मूल्यवान है ,वह तो प्रेम में डूबे ऐसे लोग ही जान पायेंगे. जिसे मीरा भी जीवन भर कहती रही है—ए री मैं तो प्रेम दीवानी,मेरो दरद न जाने कोय...
इस बहुत सहज फिल्म में अपूर्वधर बड़गैया की निर्देशकीय प्रतिभा के कुछ दृश्य अविस्मर्णीय हैं. बुलेट भड़भड़ाते पुलिस इंस्पेक्टर भगवान तिवारी घोर विश्वसनीय पुलिसवाले लगे हैं. एक दृश्य को भुला पाना मुश्किल है जो उनके बहुत संभावनाशील निर्देशकीय क्षमता का पता देती है. उसके ठेले को तहस-नहस कर दिए जाने के बाद बिल्लू का अपने ठेले पर वापस आकर उसकी दुर्गति देखने का दृश्य. उस तबाह ,टूटे-फूटे ठेले और लावारिस पड़े बिखरे सामानों के दृश्य से एक बार फिर सत्ता के निरंकुश चरित्र को बिना कुछ कहे उजागर कर देता है.या कस्बे के हाट-बाजारों,सडकों या तालाबों के पार में टाइटल दिखाना भी बिलकुल अभिनव प्रयोग है. छत्तीसगढ़ के पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म का संगीत यहाँ के मिजाज से बिलकुल मेल नहीं खाता.यह किसी पॉप-कल्चर फिल्म के गीत-संगीत सा लगता है,जो सुनने में भी चुभता है.जबकि इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया संभावनाएं थीं.
अभी प्रचलित फिल्मों के साथ इस फिल्म को देखने पर यह बिलकुल अलग जोनर की फिल्म बनायी गयी है. यहाँ बात-बात में हत्या,नग्नता,बलात्कार,हिंसा,मानसिक विकृति इत्यादि वेब-सिरिजी फार्मूले से हटकर निर्देशक ने साधारण लोगों के जीवन की साधारण सी कहानी पर एक साफ़-सुथरी फिल्म बनाने की कोशिश की है,जिसके इस पक्ष की प्रसंशा होनी चाहिए.भले ही इसमें आंचलिकता की,लोकेल की वह गंध नदारद है,जिसकी चर्चा ऊपर कर चुका हूँ,लेकिन यह उस आंचलिकता के नाम पर ठूंस दिए जाने वाले सस्ते,फूहड़ नाच-गाने से भी बचा गया है,जिसके खतरे इसमें सबसे ज्यादा थे.सफलता के नाम पर इस नकलीपन,सतहीपन से ज्यादातर छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्देशक अभी-भी से उबर नहीं पाए हैं. इस अर्थ में यह उनसे अपनी बिल्कुल अलग, यथार्थवादी और विश्वसनीय पहचान बनाती है.भविष्य के सिनेमा का यह एक सशक्त नाम होने की उम्मीद दिलाता है--अगर बाजारवादी प्रपंचों से बच सकें।
41, मुखर्जी नगर,सिकोला भाठा,दुर्ग
मोबाइल नंबर- 9827993920







.jpg)
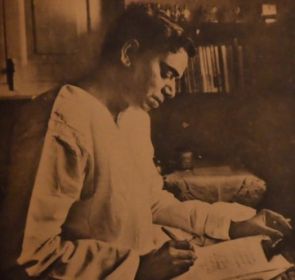




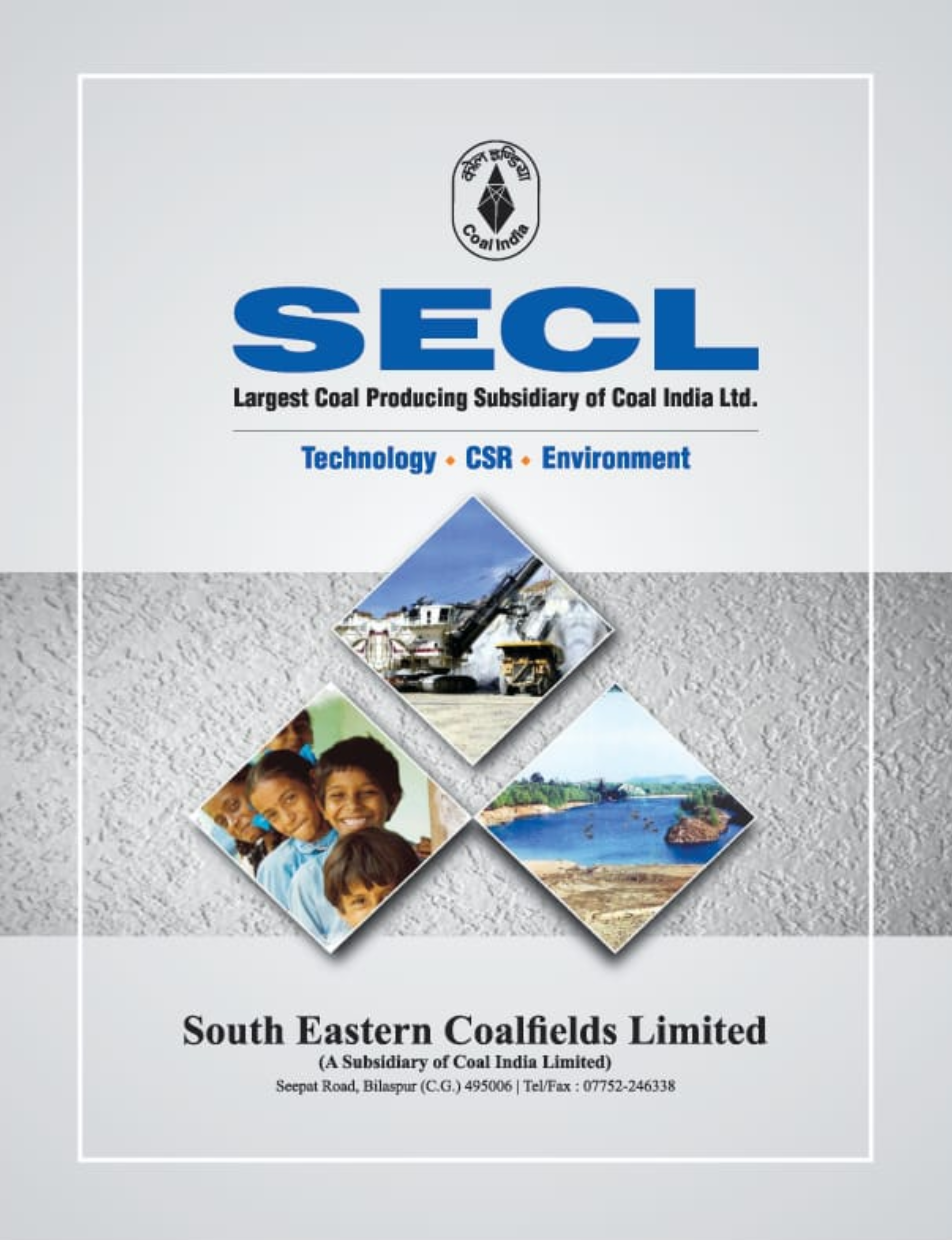



.jpg)






.jpg)