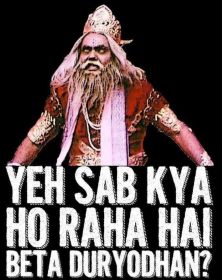फिल्म

मौलिकता का कोई री-टेक नहीं होता
देश के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के पुत्र शाश्वत गोपाल फिल्मों से मौलिकता के क्षरण को लेकर चिंता जता रहे हैं. भले ही उनका यह लेख हिंदी फिल्मों के तथाकथित विकास पर चोट है जहां से गांव-घर, किसान सब गायब है. इस लेख से छत्तीसगढ़ के उन फिल्मकारों को भी गुजरना चाहिए जो डेविड धवन, प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई की फिल्मों की नकल को ही जिंदगी का सच मान बैठे हैं. यह सही है कि आप में कोई भी सत्यजीत रे नहीं है, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि कापी पेस्ट से छत्तीसगढ़ का माथा कभी ऊंचा नहीं होगा.
शाश्वत गोपाल
फिल्म, तस्वीरों का समूह है। असंख्य क्षण जो ठहर गये थे तस्वीरों में, उनके क्रमवार मिलने से बने दृश्यों का एक सिलसिला फिल्म है। जीवन भी फिल्म की तरह है। क्षण बीतते जाते हैं और दृश्य बदलते चले जाते हैं। लेकिन, जीवन के दृश्यों में री-टेक नहीं होता। ज्यादातर हम दूसरों की जिंदगी में अपने दृश्य खोजते हैं, और कल्पना में अपनी फिल्म बनाते भी चलते हैं।
अभी हाल ही में सातवीं कक्षा के विद्यार्थी का भारत पर लिखा निबंध पढ़ा। उस बच्चे की पहली ही पंक्ति थी- ‘भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि की निर्भरता मानसून पर है।’ ये पंक्तियाँ हिंदी माध्यम के विद्यार्थी द्वारा लिखी गई थीं। बच्चे द्वारा यह लिखा जाना गुज़र चुके दृश्य का री-टेक था। लेकिन, गत कुछ दशकों में देश की स्थिति काफी बदल गई है। शिक्षा और सोच दोनों भाषा से विभाजित हो गये से लगते हैं। एक ओर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएँ तो दूसरे छोर अंग्रेजी। इस विभाजन में संवेदना का विभाजन भी है, जो कुछ भयावह सा है। अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थी के निबंध में आज किसान नहीं है। जीडीपी, गैजेट्स, पैकेज जैसे शब्दों से बने वाक्य हैं। ये ऐसे वाक्य हैं जिनके अर्थों की पहुँच ग्लोब्लाइजेशन के पंख के सहारे दुनिया के कोने-कोने तक है। लेकिन, गति इतनी तेज है कि अपना देश, आस-पड़ोस इन्हें दिखाई ही नहीं देता। आज का तथाकथित विकास यही है। भारतीय पर्दे पर इन दिनों देखें तो यही विकास नज़र आता है।
किसान, फिल्मों के केंद्र में अब नहीं हैं। भारत में तेजी से सिकुड़ते खेत, रोज़ होती किसानों की दुखद मौतें फिल्मों के दृश्य भी नहीं हैं। लेकिन, राजनीति और राजनीतिज्ञ फिल्मों के आज अहम हिस्से हैं। फिल्म ‘सरकार-1,2,3’ बन गई। ‘राजनीति’ और ‘इंदु सरकार’ बन गईं। इन दिनों भी एक फिल्म चर्चा में है ही। दो प्रमुख राजनैतिक पार्टियाँ आम जरूरी मुद्दों के बदले इस फिल्म को लेकर वाक-द्वंद्वरत हैं। फिल्मों पर प्रतिक्रियाएँ देखें तो लगता है कि लोकतंत्र में विरोध का महत्व क्या खत्म हो रहा है या किया जा रहा है? दुखद यह है कि ये प्रतिक्रियाएँ ठेठ दर्शकों की नहीं होतीं। सहनशीलता घट रही है। शायद इसकी वजह भी यह है कि हम आज सामाजिक समाज में नहीं रहते। घर-घर में घर और बाहर की राजनीति हावी है। पंजायतीराज के बाद तो गाँवों से दादा, काका, दाई जैसे संबोधन राजनीतिक पार्टियों के नामों से प्रतिस्थापित हो गये। पहले ऐसा नहीं था। वास्तविक जीवन में री-टेक कभी होता भी नहीं। लेकिन लगता है अच्छाइयों, देशज परंपराओं, संस्कृति का री-टेक जीवन और फिल्मों में बार-बार होते रहना चाहिए। वी. शांताराम, बिमल रॉय, महबूब खान, गुरु दत्त जैसे फिल्मकारों ने सन् साठ के दशक के आस-पास गांवों, किसानों पर आधारित अनेक फिल्में बनाईं। हमारा जो कल था, वह सुनहरा था। उसमें भारतीयता घुली हुई थी। आज की फिल्में पश्चिमी तौर-तरीकों से भरी हुई हैं। एक सी लगती हैं। एक फिल्म किसी दूसरे का री-टेक लगती है। यह संकेत मौलिकता के क्षरण का भी है।
री-टेक से फिल्म पीछे लौट जाती है। वह केवल एक सहारा है, पिछले को भूलने नहीं देने का। इससे आगे केवल बढ़ता है तो वह है ‘समय’। जो गुज़र जाता है। खर्च हो जाता है। हम समय, जीवन, देश, आस-पड़ोस धीरे-धीरे सब कुछ खो रहे हैं। आज मौलिकता का संकट है। फिल्मों में तो यह संकट ज्यादा है। सत्यजीत रे का सिनेमा भारतीयता को उसके तमाम संघर्षों, असीम संवदेनाओं के साथ बार-बार सामने लाने वाला सच था। लेकिन, इनमें संघर्षों के दोहराव नहीं थे। आज की फिल्मों में लहलहाते खेत तो हैं, लेकिन कर्ज़ में डूबे, हर दिन मौत के करीब जाते किसान नहीं हैं। किसानों का वह सत्य नहीं है जो वास्तविक-सच है। सत्यजीत रे के बाद भारतीयता के ऐसे तमाम् सच फिल्मों से छूटते चले गये।
दो वर्ष पूर्व पर्दे पर आई ‘कालीचाट’ फिल्म ने सत्यजीत रे के बाद भारतीय संघर्ष को प्रतिबिंबित न कर पाने के एक लंबे खालीपन को कुछ भरा। कालीचाट एक प्रकार की चट्टान का नाम है। इस तरह की चट्टानें मालवा क्षेत्र में काफी हैं। ये चट्टानें इतनी मजबूत होती हैं कि आधुनिक मशीनों से भी आसानी से नहीं टूटतीं। लेकिन, कहा जाता है कि इसके नीचे जल का अथाह भंडार रहता है। सुनील चतुर्वेदी के उपन्यास पर बनी कालीचाट फिल्म की कथा इसी तरह की मजबूत चट्टान, एक किसान परिवार और आशाओं के अनंत क्षितिज के ईर्द-गिर्द बुनी है। जीवन की संवेदनाओं, वेदनाओं के कटु सत्य को फिल्म के निर्देशक सुनील शर्मा ने इतने करीब ला दिया है कि वह अंतः मन को झकझोर देती है। इस तरह की कुलबुलाहट सत्यजीत रे द्वारा निर्मित फिल्मों से प्रतिबिंबित होती थी। देखें तो आज भी होती है। जीवन की चुनौतियाँ आज भी वही हैं, जो तब थीं। लेकिन, आज हमारी अंतःदृष्टि के बीच आधुनिक फिल्म का बाज़ार रूपी वह पर्दा आ गया है जो हमें बहला कर रखना चाहता है। वह हमें अपने संघर्षों की याद नहीं दिलाना चाहता। भूल जाने का अहसास अधिक उपभोक्ता बनाता है। संघर्ष, चुनौतियाँ हमें ज्यादा उपभोक्ता बनने के लिए कम समय देती हैं, उससे दूर ले जाती हैं। उदारीकरण के शुरुआती दौर के आस-पास सत्यजीत रे पर भारत की चुनौतियों, तकलीफों को बेचने के आरोप काफी लगे कि वे भारतीय संघर्ष, गरीबी जैसे विषय अपनी फिल्मों के माध्यम से बेचते हैं। उनकी और उनकी फिल्मों की आचोलना के लिए ‘गरीबी का सौंदर्यीकरण’ जैसे शब्दों का उपयोग किया गया।
यह आरोप इसलिए हैं क्योंकि सच और वास्तविकता को सामने लाने वाले दृश्य को बे-अर्थ बनाना पूँजीवाद का लक्ष्य है। कला आज बची है तो वह संघर्षों, अभावों के बीच ही बची है। पूँजी, कला को खरीद सकती है, पोस सकती है, लेकिन उसे कभी सृजित नहीं कर सकती। बहुत कुछ भुलाकर-गँवाकर ही कुछ सृजन हो पाता है। उदारीकरण ने दुनिया के उन देशों के परंपरागत आधारों को तेजी से बदला जिनकी सांस्कृतिक नींव कमज़ोर पड़ने लगी थी। सत्यजीत रे ने भारतीयता को हमेशा केंद्र में रखा। रुमानियत से इतर उनकी फिल्मों ने वास्तविक यथार्थ को ज्यादा करीब से दिखाया। सच को देखना हमेशा कठिन होता है। क्योंकि वो हमें हमारे वर्तमान और भविष्य के लक्ष्य के साथ तुलनात्मक दुविधा में डालता है।
फिल्म विधा में पैसा लगाना केवल लाभ की दृष्टि को सामने रखकर ही संभव हो पाता है। प्रयोग,यथार्थपरक, जीवन से सीधे जुड़े मुद्दों पर ज्यादातर फिल्मी कहानियाँ गढ़ी नहीं जातीं। क्योंकि उसमें पैसा लगाने वाला जानता है कि दर्शक उस यथार्थ को देखना पसंद नहीं करता जो वास्तविक है। वह कल्पना में कुछ घंटे जीना चाहता है, जो उसे कुछ घंटों का काल्पनिक सुख दे दे। सत्यजीत रे ने फिल्म पाथेर पांचाली में अपनी पत्नी के गहने बेचकर जीवन के यथार्थ को सामने लाया था। तब के दर्शक वर्ग ने जीवन के उस कटु सत्य को देखा भी। 1955 में बनी पाथेर पांचाली कलकत्ता के सिनेमाघरों में 13सप्ताह तक हाउसफुल रही। फ्रांस के कान फिल्म महोत्सव में इसे ‘बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट’ का सम्मान भी मिला। आज की पीढ़ी शायद इस फिल्म की परिभाषा को समझ भी नहीं पाए। बाज़ार ने संवेदनाओं और अपनी चीजों से होने वाले लगाव को तोड़ दिया है। संवेदन शून्य एवं लगभग भावहीन युवाजन से इस तरह की फिल्में देखने के संदर्भ में कोई आशा नहीं करना ही ठीक होगा। दूसरी ओर लोकतंत्र में राजनीति और संसद चाहती भी यही है कि लोग यथार्थ से दूर अपनी-अपनी कल्पनाओं में खोए रहें, ताकि उनकी रोटी सिकती जाए। कभी जले नहीं।
सत्यजीत रे ने इस राजनैतिक रोटी की कभी चिंता नहीं की। वे यथार्थ के सच को 70 एमएम के सहारे समाज के बड़े कैनवास पर दिखाना चाहते थे। उनकी फिल्मों के फ्रेम छायाचित्र की तरह हैं। वे अपनी फिल्मों के महत्वपूर्ण दृश्यों के रेखाचित्र शूटिंग के पहले ही बना लिया करते थे। यह एक कला का दूसरी कला के साथ संयोजन था। पाथेर पांचाली का संगीत सत्यजीत रे और रविशंकर ने 11 घंटे में ही रचा था। कला का सृजन और उसका प्रस्तुतिकरण समय पर निर्भर नहीं करता। आज की फिल्मों में कथा कई बार एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के बीच खो जाती है। सत्यजीत रे इन्हीं फ्रेमों के बीच के खालीपन को संवेदनाओं से भर देते थे। दरअसल उनकी कथा का आगे बढ़ना छूट चुके दृश्यों के अर्थों की गहराई के साथ-साथ होता था।
सत्यजीत रे के जीवन में कला और सृजन शब्द अपने अर्थों के साथ शुरू से रहे। उनकी शिक्षा का बड़ा हिस्सा विश्व-भारती विश्वविद्यालय में गुज़रा। वे पूर्वी कला से प्रभावित भी थे। शुरूआती दिनों में उन्होंने पेशेवर चित्रकारी की। पुस्तकों के आवरण-चित्र बनाने का काम किया। जिसमें जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी शामिल थी। बांग्ला उपन्यास पाथेर पांचाली के लघु बाल संस्करण पर भी उन्होंने कार्य किया, जिसका नाम था आम ऑटिर भेंपू (आम की गुठली की सीटी)। अपनी पहली फिल्म उन्होंने इसी कथा पर बनाई। सत्यजीत रे की यह खूबी थी कि वे प्रत्येक कार्य में, हर चीज़ को कला की दृष्टि से तौलते थे। उन्होंने दो फाँट भी बनाए – ‘राज बिज़ार’ और ‘राय रोमन’।
कुछ जीवनानुभव के बाद उनके जीवन-दृश्य चित्रों में बदलते गये और समय के साथ-साथ एक-एक चित्र मिलकर फिल्मों के फ्रेम बनते चले गये। सन् 1950 के करीब वे लंदन गये। लंदन में उन्होंने 99 फिल्में देखीं। करीब-करीब एक फिल्म से कुछ ज्यादा रोज़। वे लंदन में तीन महीने रहे। स्थिर चित्रों से चलचित्रों की ओर उनका जाना साइकिल के सहारे हुआ। लंदन प्रवास में वित्तोरियो दे सीका की इतालवी फिल्म लाद्री दी बिसिक्लेत (बाइसिकल चोर) भी उन्होंने देखी थी। इस फिल्म ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और वे चलचित्र की ओर मुड़ गये।
रे ने वृत्तचित्र बनाये, छोटी-छोटी फिल्में बनाईं और लंबी फीचर फिल्में भी। कुल 37 फिल्म कृतियों की रचना उन्होंने की। फिल्मों से जुड़े ज्यादातर कामों से उन्होंने अपने आपको सीधे तौर पर जोड़कर रखा। पटकथा लेखन, कलाकारों का चयन, संगीत, कला निर्देशन, संपादन, फिल्मों के पोस्टर, प्रचार-सामग्री की रचना जैसे तमाम काम वे स्वयं करते या उनके सीधे निर्देशन में ये सब होता। उन्होंने कहानियाँ लिखीं और फिल्म को एक आचोलक दृष्टि से भी देखा। फिल्मों के माध्यम से अद्वितीय योगदान के लिए भारत रत्न, मानद आस्कर सहित 32 राष्ट्रीय फिल्म पुररस्कार उन्हें और उनके कामों को मिले। पुरस्कार किसी को बड़ा नहीं बनाते, काम बड़ा बनाता है।
ऐसा कह सकता हूँ कि रे अपनी फिल्मों के प्रत्येक क्षण से जुड़े रहते थे। वे फिल्म बनने की पूरी प्रक्रिया की गहराई में डूब जाते। फिल्म लिखते भी स्वयं, संवाद को गढ़ते भी खुद। अभिनय की बारीकियों को पहले ही दर्ज कर लेते। उनकी टीप देखें तो उसमें फिल्मांकन के स्थानों का विवरण होता, कभी-कभी इतना ज्यादा कि मानस पटल पर वह दृश्य उभर जाता। इसमें उनके बनाये रेखांकन होते। पर्दे पर दिखने वाले चेहरों के भाव और संपादन की कुछ हिदायतें भी। कल्पनाओं से भरी संगीत की गूँज-अनुगूँज तो जरूर उसमें होती।
सत्यजीत रे की फिल्मों की पांडुलिपि आज हमें नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनकी प्रतिलिपियाँ कभी बनाई ही नहीं गईं। वे जब भी अपनी पांडुलिपि के साथ अभिनेताओं और फिल्मी साथियों के साथ बैठते और चर्चा करते तब उनकी पांडुलिपि उनके हाथों में होती और वे उसे छाती से सटाकर रखते और दर्शक उनकी फिल्मों को ह्रदय से।
जिस तरह उनके स्थिर चित्र बहुत सारा कुछ और कहते थे उसी तरह उनके चलचित्र भी थे। फिल्म ‘शतरंज के खिलाड़ी’ के एक महत्वपूर्ण लंबे दृश्य में केवल तीन सौ शब्द ही उच्चरित हुए हैं। उनकी फिल्मों में इतनी सरलता थी कि उसकी गहराई आसानी से समझ में नहीं आती। आलोचकों ने रे की फिल्मों की गति की तुलना ‘राजसी घोंघे’ से भी की है। लेकिन, उन्होंने आलोचनाओं का उत्तर कभी उस तरह पलटकर नहीं दिया। उनकी कृतियाँ ही उत्तर हैं और प्रतिप्रश्न भी।
अकीरा कुरोसावा कहते थे - “राय की फिल्मों को धीमा नहीं कहा जा सकता। वे तो विशाल नदी की तरह शांति से बहती हैं। उनका सिनेमा न देखना इस जगत में सूर्य या चंद्रमा को देखे बिन रहने के समान है।”
फिल्म में प्रत्येक फ्रेम एक जैसा नहीं होता। मौलिकता का कभी कोई री-टेक नहीं हो सकता।
पता- शाश्वत गोपाल
सी-217, शैलेन्द्र नगर,
रायपुर-492001, छ्त्तीसगढ़
दूरभाषः (मो.) 9179518866
ई-मेलः [email protected]







.jpg)
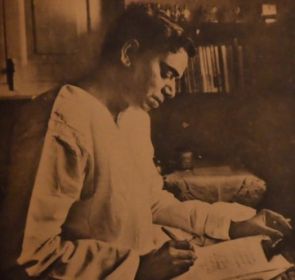




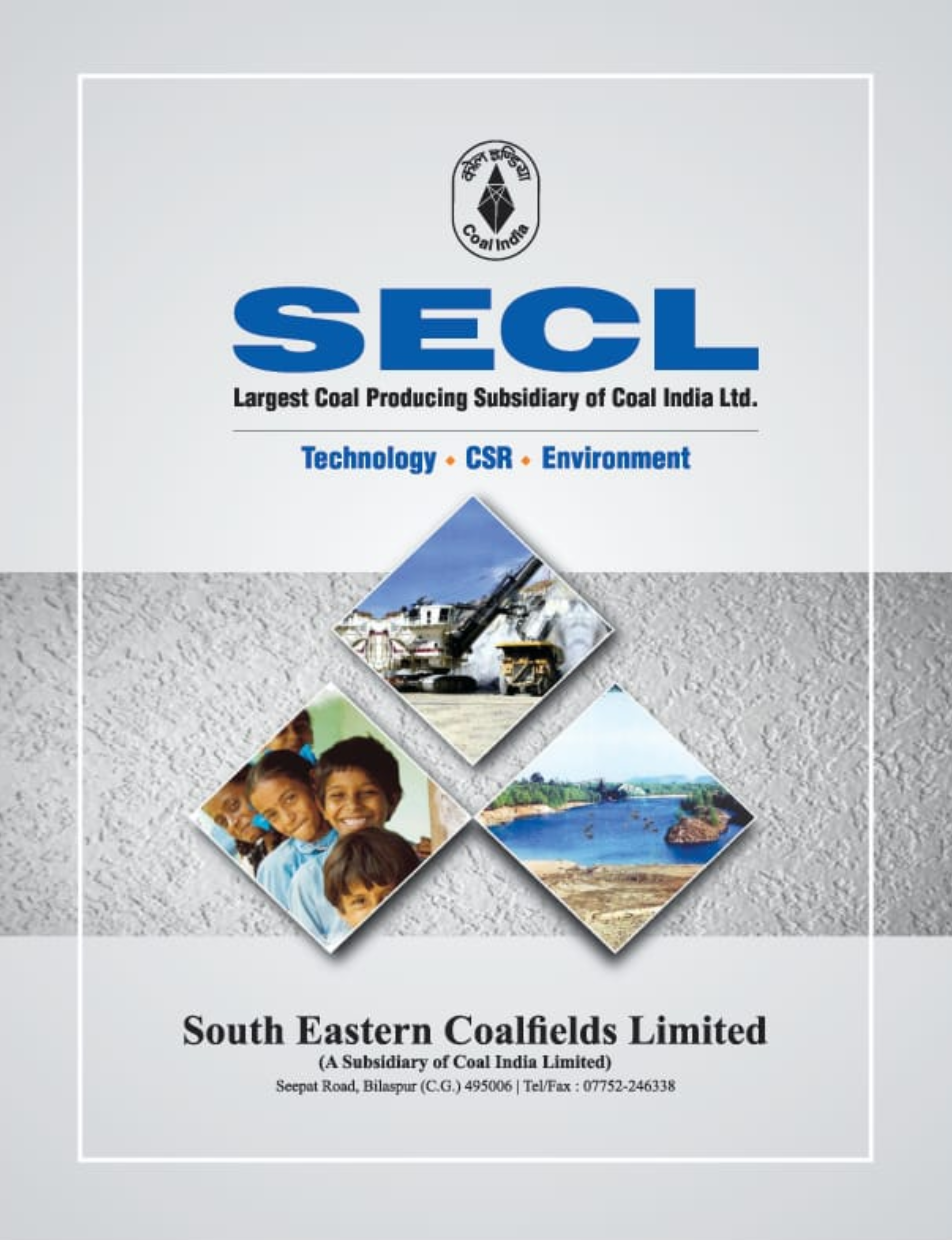



.jpg)






.jpg)