विशेष टिप्पणी
अरे...रवीश कुमार ने तो रूला दिया
देश के प्रसिद्ध पत्रकार रवीश कुमार ने रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने के बाद अपने दर्शकों/ पाठकों और चाहने वालों के प्रति आभार जताया है. आभार पढ़कर रुलाई छूट जाती है.
आप भी रो लीजिए...कभी-कभी ऐसा रोना भी अच्छा लगता है.
आपका लिखा हुआ मिटाया नहीं जा रहा है। सहेजा भी नहीं जा रहा है। दो दशक से मेरा हिस्सा आपके बीच जाने किस किस रूप में गया होगा, आज वो सारा कुछ इन संदेशों में लौट कर आ गया है। जैसे महीनों यात्रा के बाद कोई बड़ी सी नाव लौट किनारे लौट आई हो। आपके हज़ारों मेसेज में लगता है कि मेरे कई साल लौट आए हैं। हर मेसेज में प्यार,आभार और ख़्याल भरा है। उनमें ख़ुद को धड़कता देख रहा हूं। जहां आपकी जान हो, वहां आप डिलिट का बटन कैसे दबा सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी का मेसेज डिलिट नहीं हो रहा है। चाहता हूं मगर सभी को जवाब नहीं दे पा रहा हूं।
व्हाट्स एप में सात हज़ार से अधिक लोगों ने अपना संदेशा भेजा है। सैंकड़ों ईमेल हैं। एस एम एस हैं। फेसबुक और ट्विटर पर कमेंट हैं। ऐसा लगता है कि आप सभी ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया है। कोई छोड़ ही नहीं रहा है और न मैं छुड़ा रहा हूं। रो नहीं रहा लेकिन कुछ बूंदे बाहर आकर कोर में बैठी हैं। नज़ारा देख रही हैं। बाहर नहीं आती हैं मगर भीतर भी नहीं जाती हैं। आप दर्शकों और पाठकों ने मुझे अपने कोर में इन बूंदों की तरह थामा है।
आप सभी का प्यार भोर की हवा है। कभी-कभी होता है न, रात जा रही होती है, सुबह आ रही होती है। इसी वक्त में रात की गर्मी में नहाई हवा ठंडी होने लगती है। उसके पास आते ही आप उसके क़रीब जाने लगते हैं। पत्तों और फूलों की ख़ुश्बू को महसूस करने का यह सबसे अच्छा लम्हा होता है। भोर का वक्त बहुत छोटा होता है मगर यात्रा पर निकलने का सबसे मुकम्मल होता है। मैं कल से अपने जीवन के इसी लम्हे में हूं। भोर की हवा की तरह ठंडा हो गया हूं।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आस-पास मेरे जैसे ही लोग हैं। आपके ही जैसा मैं हूं। मेरी ख़ुशी आपकी है। मेरी ख़ुशियों के इतने पहरेदार हैं। निगेहबान हैं। मैं सलामत हूं आपकी स्मृतियों में। आपकी दुआओं में। आपकी प्रार्थनाओं में। आपने मुझे महफ़ूज़ किया है। आपके मेसेज का, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता है। बस आपका हो जाया जा सकता है। मैं आप सभी को होकर रह गया हूं। बेख़ुद हूं। संभालिएगा मुझे। मैं आप सभी के पास अमानत की तरह हूं। उन्हें ऐसे किसी लम्हें में लौटाते रहिएगा।
बधाई का शुक्रिया नहीं हो सकता है। आपने बधाई नहीं दी है, मेरा गाल सहलाया है। मेरे बालों में उंगलियां फेरी हैं। मेरी पीठ थपथपाई है। मेरी कलाई दबाई है। आपने मुझे प्यार दिया है,मैं आपको प्यार देना चाहता हूं। आप सब बेहद प्यारे हैं। मेरे हैं।
( रवीश कुमार )
|
|
|
मैं पत्रकार बोलूंगा...तुम रवीश कुमार समझना
रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे अवार्ड की घोषणा के साथ ही जनता को ऐसे लग रहा है जैसा उनका अपना कोई जीत गया है. जो जनता मोदी को उनकी कथित कलाबाजियों की वजह से पराजित नहीं कर पाई थीं वह रवीश कुमार को मैग्सेसे अवार्ड दिए जाने से खुद को जीता हुआ महसूस कर रही है.सोशल मीडिया में रवीश कुमार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. तरह-तरह की प्रतिक्रिया आई है. किसी ने लिखा है- रवीश...तुमने दिल जीत लिया. किसी का कहना है-कमल का फूल पकड़कर पत्रकारिता का गला घोंटने वाले पत्रकारों...अब उस पत्रकार को अवार्ड मिला है जिसने कलम को पकड़कर पत्रकारिता के साथ-साथ हमारी उम्मीदों को जिंदा रखा.एक प्रतिक्रिया यह भी है- मैं पत्रकार बोलूंगा... तुम रवीश कुमार समझना.
रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए बधाई....मगर पाठकों यह जानना भी जरूरी है कि रवीश कुमार का चयन इस अवार्ड के लिए क्यों किया गया. रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देने वाली संस्था ने इस अवार्ड के लिए रवीश कुमार की पत्रकारिता को लेकर जो टिप्पणी की है वह हिंदुस्तान के छह सालों के हालात पर भी टिप्पणी है. आप जान सकें इसलिए इसका हिंदी अनुवाद किया है- मयंक सक्सेना ने.
पिछले कुछ सालों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज़ाद और ज़िम्मेदार पत्रकारिता के स्पेस को सिकुड़ते देखा है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं: नई सूचना प्रोद्योगिकी के कारण बदलता मीडिया का स्वरूप, ख़बर और रायशुमारी का बाज़ारीकरण, सरकार का बढ़ता नियंत्रण और सबसे चिंताजनक है लोकप्रिय अधिनायकवाद और धार्मिक-जातीय-राष्ट्रवादी कट्टरपंथियों का अपने सतत विभाजनकारी, असहिष्णु और हिंसक तरीके से उभार।
इन बढ़ते ख़तरों के विरोध में भारत में एक अहम आवाज़ हैं टीवी पत्रकार रवीश कुमार। हिंदीभाषी राज्य बिहार के जितवापुर गांव में पैदा हुए और पले-बढ़े रवीश ने अपने शुरुआती रुझान के मुताबिक अपनी परास्नातक डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और पब्लिक अफेयर्स में ली। 1996 में उन्होंने एनडीटीवी ज्वाइन किया और एक फील्ड रिपोर्टर के तौर पर शुरुआत की। देश की 42 करोड़ हिंदी भाषी जनता के बीच एनडीटीवी ने जब अपना हिंदी चैनल एनडीटीवी-इंडिया लॉंच किया तो रवीश कुमार का अपना शो शुरु हुआ - प्राइम टाइम। आज एनडीटीवी के सीनियर एक्सीक्यूटिव एडीटर के तौर पर रवीश कुमार, देश के सबसे प्रभावशाली टीवी पत्रकारों में से एक हैं।
हालांकि उनकी सबसे बड़ी विशेषता वो पत्रकारिता है, जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ऐसे मीडिया के माहौल में, जो एक दखलअंदाज़ सत्ता से डरा हुआ है, जो कट्टर राष्ट्रवादी ताकतों और ट्रोल्स से ज़हरीला हो गया है और फ़ेक न्यूज़ से भरता जा रहा है और जहां बाज़ार की रेटिंग्स ने सारा दांव 'मीडिया शख्सियतों', 'पीत पत्रकारिता' और दर्शकों को लुभाने वाली सनसनी पर लगा रखा है, रवीश पत्रकारिता की सभ्य, संतुलित और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग शैली को ही पेशेवर पत्रकारिता बनाए रखने पर अड़े हुए हैं। एनडीटीवी पर उनका कार्यक्रम 'प्राइम टाइम' ताज़ातरीन सामाजिक मुद्दों को उठाता है, गंभीर बैकग्राउंड रिसर्च करता है और मुद्दे को एक या उससे भी अधिक एपीसोड्स में एक बहुआयामी चर्चा के साथ सामने रखता है। इस कार्यक्रम में मुद्दे असल ज़िंदगी में आम लोगों की अनकही दिक्कतों की बात करते हैं - जो सीवर में नंगे हाथ-पैर उतरने वालों और रिक्शाचालकों से लेकर सरकारी कर्मचारियों और किसानों की तक़लीफ़ से अर्थाभाव से जूझते सरकारी स्कूलों और अकर्मण्य रेलवे तंत्र तक हो सकते हैं। रवीश सरलता से गरीब जनता से संवाद करते हैं, खूब यात्राएं करते हैं और अपने दर्शकों से संपर्क में रहने के लिए सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं और इसके ज़रिए भी अपने कार्यक्रम के लिए स्टोरीज़ तैयार करते हैं। जन-आधारित पत्रकारिता की लगातार कोशिश करते हुए, वो अपने न्यूज़रूम को जनता का न्यूज़रूम कहते हैं।
रवीश भी कई बार कुछ नाटकीयता का सहारा लेते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये प्रभावी तरीका है। उन्होंने 2016 में एक अनोखे ढंग के शोर में नाटकीय ढंग से बताया था कि कैसे टीवी न्यूज़ शोज़ में बहस का स्तर कितना गिर चुका है। शो की शुरुआत में स्क्रीन पर आते हुए रवीश बताते हैं कि कैसे टीवी न्यूज़ शोज़ गुस्सैल और कानफो़ड़ू आवाज़ों के अंधेरे जगत में बदल गए हैं। उसके बाद स्क्रीन काली हो जाती है और अगले एक घंटे तक स्क्रीन काली रहती है और पीछे से असल टीवी शोज़ के कर्कश ऑडियो, ज़हरीली धमंकियां, बौखलाहट भरी रट, साउंडबाइट्स और दुश्मन का खून बहाने को तत्पर भीड़ का शोर सुनाई देते रहते हैं। रवीश के मुताबिक उनके लिए हमेशा संदेश अहम है, जिसे दिया जाना ही चाहिए।
एक एंकर के तौर पर रवीश हमेशा भद्र हैं, संतुलित हैं और सूचना से सुसज्जित रहते हैं। वो अपने अतिथि पर हावी नहीं होते बल्कि उनको अपनी बात कहने का मौका देते हैं। वो चिल्लाते नहीं, लेकिन सबसे ऊंचे शक्ति की ज़िम्मेदारी भी गिनाते हैं और देश में सार्वजनिक-विमर्श में भूमिका के लिए मीडिया की भी निंदा कर डालते हैं: इस वजह से उनको लगातार अलग-अलग तरह की कट्टर शक्तियों की धमकिय़ों और ख़तरों का सामना करना पड़ता रहा है। इन सारी मुश्किलों और बाधाओं के बावजूद भी रवीश एक समीक्षात्मक, सामाजिक तौर पर जवाबदेह मीडिया के स्पेस को बढ़ाते रहने के अपने प्रयासों में लगे रहे हैं। एक ऐसी पत्रकारिता में भरोसा रखते हुए, जिसके केंद्र में आम लोग हैं, रवीश पत्रकार के तौर पर अपनी भूमिका को मूलभूत रूप से परिभाषित करते हैं, "अगर आप लोगों की आवाज़ बन सकते हैं, तो ही आप पत्रकार हैं।"
2019 के रेमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए रवीश कुमार का चुनाव करते हुए, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ उनके उच्चतम कोटि के तिक पत्रकारिता के प्रति अडिग समर्पण को ध्यान में रखता है: उनका नैतिक साहस जिसके दम पर वो सच के लिए खड़े होते हैं, उनकी ईमानदारी, आज़ादी और उनके उस सैद्धांतिक विश्वास को सम्मानित करता है, जिसके मुताबिक पत्रकारिता लोकतंत्र की उन्नति में अपना सबसे आदर्श लक्ष्य तब हासिल करती है, जब वो सच को साहस से बोलती है, बेआवाज़ों की आवाज़ को सत्ता के सामने ताकत देती है, लेकिन अपनी भद्रता नहीं खोती...
( मूल साइटेशन - रेमन मैगसेसे पुरस्कार की वेबसाइट से )
छत्तीसगढ़ में अंडे का विरोध... संघी गिरोह की चाल!
राजकुमार सोनी
छत्तीसगढ़ की सरकार आंगनबाड़ी केंद्र और मध्यान्ह भोजन में गर्भवती माताओं और बच्चों को पोषक आहार के रुप में अंडा देना चाहती है. बहुत से लोग सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और इसे एक अच्छा कदम बता रहे हैं, लेकिन कतिपय संगठन और लोग ( जिसमें कुछ तथाकथित शाकाहारी भाजपाई पत्रकार भी शामिल है.) विरोध जता रहे हैं. कुछ खुलकर विरोध कर रहे हैं तो कुछ का विरोध सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली... मुहावरे को चरितार्थ करने वाली शैली में हैं. इस विरोध को देखकर लग रहा है कि सब असंतुष्ट भूपेश सरकार को पलट देने की हड़बड़ी में हैं. चूंकि भोजन में अंडे देने का समर्थन करने वाले संगठन और उससे जुड़े लोग झंडे-बैनर लेकर सड़कों पर उतर नहीं रहे और केवल प्रेस विज्ञप्ति तक ही सीमित है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि अंडे ने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है.
निजी तौर पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं किस तरफ हूं तो कहूंगा कि मैं अंडा खाने वालों के साथ हूं और चाहता हूं कि एक बच्चे को एक या दो नहीं बल्कि खाने में पूरे चार अंडे मिलने चाहिए. जिन लोगों ने कभी गरीब बच्चों को बड़े चाव से अंडा खाते नहीं देखा वे इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे कि अंडा क्या होता है ? मैं एक ऐसे परिवार से हूं जहां अंडा खाने के पहले ख्वाब देखना होता था. जब कभी भी घर में अंडा आता तो हम पांच भाई इस ताक में रहते थे कि कब अंडा उबलेगा और कब हमें खाने को मिलेगा. कई बार तो अंडे के बंटवारे को लेकर भाइयों के बीच झड़प भी हो जाया करती थी. एक अंडे के कई हिस्से हो जाया करते थे. एक उबले हुए अंडे में थोड़ा सा नमक और काली मिर्च छिड़ककर खाने का मजा क्या होता है इसे वही समझ सकता है जो इसे रोज खाता है. जिसके भोजन में काजू-कतली शामिल रहती है वे इस बात को कभी नहीं जान पाएंगे कि अंडे का स्वाद क्या है. मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के गांवों में अब भी कई घर ऐसे होंगे जहां रहने वाले बच्चों के लिए अंडा एक ख्वाब है. ख्वाब देखने वाले बच्चे अंडे का इंतजार करते हैं. उनका इंतजार हर हाल में खत्म होना चाहिए. अंडे का विरोध करने महान नेताओं से यह भी कहना चाहूंगा कि किसी बच्चे के मुंह से उसकी पसंद का निवाला छीनने की कोशिश भी मत करिए. संभल जाइए... बच्चा आपका वोट बैंक नहीं है, लेकिन देश का भविष्य अवश्य है. कम से कम देश का भविष्य स्वस्थ रहने दीजिए.
वैसे अंडा वितरण योजना के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने इसे लेकर कोई बाध्यता नहीं रखी है. जो बच्चे अंडा खाना चाहेंगे उन्हें अंडा दिया जाएगा जो नहीं चाहेंगे उन्हें उतनी ही कैलोरी का कोई अन्य पोषक तत्व देने की योजना भी बनाई गई है. सरकार ने खानपान की स्वतंत्रता का ख्याल रखा है बावजूद इसके सोमवार को एक विधायक ने विधानसभा में यह आशंका जताई कि अगर कोई शाकाहारी बच्चा अंडे को आलू समझकर खा लेगा तब क्या करिएगा ? अब आशंकाओं का कोई हकीम तो होता नहीं है. ये हो जाएगा... वो हो जाएगा... कहने का हक तो सबको है. वैसे विधायक महोदय ने विधानसभा में खुद को लेकर एक मजेदार बात भी बताई. विधायक ने कहा- मैं मटन खाता हूं. चिकन खाता हूं और अंडा भी खाता हूं, मगर फिर भी चाहता हूं कि बच्चों को भोजन में अंडा न दिया जाय. विधायक का कथन सुनकर बचपन में सुना हुआ एक मुहावर भी याद आया- आप गुरूजी बैगन खाए और दूसरों को ज्ञान सिखाएं. ( बैगन मत खाना... बैगन में कीड़े होते हैं.)
छत्तीसगढ़ में भाजपा के समय से विज्ञप्ति आधारित पत्रकारिता चल रही है अन्यथा पत्रकारों के लिए एक अच्छा विषय यह भी हो सकता था कि कौन-कौन सा जनप्रतिनिधि अंडा खाता है? छुपकर खाता है या सार्वजनिक जीवन में भी खाता है ? अंडे का विरोध करने वाले ठीक-ठाक ढंग से यह नहीं बता पाते हैं कि अगर बच्चों को खाने में अंडा न दिया जाए तो फिर क्या दिया जाय. क्या बच्चों को लड्डू-पेड़ा बांटना चाहिए. किसी संगठन ने सोयाबीन देने की बात कहीं है. पाठकों को याद होगा कि प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थीं तब सरकार ने स्कूलों में सोयाबीन दूध के वितरण की योजना बनाई थीं. इसके लिए मनीष शाह नाम के एक दलाल से अनुबंध भी किया गया था. खूब हो-हल्ला हुआ कि बच्चों को पौष्टिक सोयाबीन का दूध दिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या... दलाल शाह कई करोड़ रुपए का भुगतान लेकर बैठ गया. हालांकि यह दलाल अब भी सक्रिय है और इन दिनों इसकी आवाजाही मंत्रालय में भाजपा सरकार के स्वामीभक्त अफसरों के कमरों में देखी जा सकती है.
वैसे काफी पहले अंडे को लेकर फैलाए गए तमाम भ्रम टूट गए हैं. खानपान का अध्ययन करने वाले चिकित्सकों ने मान लिया है कि अंडा बढ़ते हुए बच्चों के लिए प्रोटीन का एक उत्तम विकल्प है. अंडे में विटामिन सी जैसे एक- दो तत्व छोड़कर सभी तरह के पोषक तत्व मिलते हैं. एक सर्वे यह भी बताता है कि छत्तीसगढ़ के 38 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार है और अनुसूचित जनजाति के बच्चों में कुपोषण की यह दर 44 फीसदी है. छत्तीसगढ़ में 83 फीसदी आबादी अंडे का सेवन करती है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देश के 15 से अधिक राज्यों में मध्यान्ह भोजन आंगनबाड़ी केंद्रों में कई सालों से अंडे का वितरण किया जा रहा है. सवाल यह है कि आखिर हम अपने नौनिहालों को क्या कुपोषित ही रहने देना चाहते हैं ? सच तो यह भी है कि शाकाहार या मांसाहार के नाम पर किसी भी समुदाय-विशेष को अन्य लोगों के खानपान पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है और इसका हमारी संस्कृति से भी कोई लेना-देना भी नहीं है. किसी बच्चे के अंडा खा लेने से संस्कृति नष्ट हो जाएगी और किसी के केला-मौसंबी-संतरा खा लेने से संस्कृति बच जाएगी यह सोचना सिवाए मूर्खता के और कुछ नहीं है. श्रीमान जी प्रदेश की 80 फीसदी आबादी अपने भोजन में मांस का उपयोग करती है. अगर आप शाकाहारी है तो शाकाहारी बने रहिए... आपके शाकाहार होने पर तो कोई विरोध नहीं करता ? चूंकि आप शाकाहार है, इसलिए संस्कृति के रक्षक है यह सोचना ठीक नहीं है. अंडा खा लेने से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाता है. दरअसल प्रदेश में अंडे का जो विरोध दिख रहा है उसके पीछे संघी गिरोह की कसरत साफ तौर पर दिखाई दे रही है. इस गिरोह को लगता है कि लोग समझ नहीं रहे हैं. सबको पता है कि कौन किस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा उछाल रहा है. किसका क्या मकसद है. संघी गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को कुपोषित बनाए रखने की साजिश रचता ही रहा है. इस बार भी यहीं खेल खेला जा रहा है. अफसोस इस बात का है कि इस गिरोह को चारों खाने चित्त कर देने वाला कोई माकूल जवाब अब तक नहीं दिया जा सका है.
अरे... संडे हो या मंडे, हर रोज खाओ अंडे
पर...समझे प्यारे समझो, चड्डियों के हथकंडे
अरबन नक्सल का हौव्वा खड़ा करके किनके हित साध रहा है संघ ?
भंवर मेघवंशी, सम्पादक-शून्यकाल
आरएसएस के प्रचार विभाग द्वारा संकलित और विश्व संवाद केंद्र,जयपुर द्वारा प्रकाशित 50 पृष्ठ की एक पुस्तिका "कौन है Urban Naxals"कल ही पढ़ने को मिली।
जैसा कि इसकी प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि -' समाज की सतत सजगता हेतु मुख्यधारा के हिंदी समाचार पत्र पत्रिकाओं में "अरबन नक्सल" विषयों पर प्रकाशित आलेखों का संकलन है यह पुस्तिका। इसके लेखकों में अजय सेतिया, विवेक अग्निहोत्री, मनु त्रिपाठी, मकरंद परांजपे, ज्ञानेंद्र भरतिया, आशीष कुमार अंशु,अभिनव प्रकाश,नीलम महेंद्र,हितेश शंकर,अवधेश,शौर्य रंजन,अंजनी झा और यादवेन्द्र सिंह शेखावत जैसे लोग शामिल है। ज्यादातर आलेख पांचजन्य अथवा अन्य दक्षिणपंथी विचार समूह की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुये है।
पुस्तिका साफ कहती है कि 'बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम' जैसी फ़िल्म बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री की देन है अरबन नक्सल शब्द,जिनकी इसी नाम से एक किताब भी आ चुकी है।इस किताब की भूमिका मकरंद परांजपे द्वारा लिखी गई है,ऐसा परांजपे का खुद कहना है।
किताबें लिखी जाती है,प्रकाशित होती है,वितरित होती है,बिकती है,यह सामान्य बात है,इसमें कोई दिक्कत नहीं है,लोकतांत्रिक देश में हर तरह के विचार का साहित्य छपेगा,बंटेगा और बिकेगा भी,मगर खतरनाक बात यह है कि पढ़ने पर यह प्रचार पुस्तिका पूरी तरह से दुष्प्रचार पुस्तिका जैसी लगती है।
इस पुस्तिका के माध्यम से देश भर में गरीब दलित आदिवासी व अल्पसंख्यक समुदाय के मूलभूत मानवीय अधिकारों के लिए दशकों से लड़ रहे लोगों को द्वेषपूर्ण ढंग से टारगेट करते हुए लांछित किया गया है,इस पुस्तिका की भूमिका में ही यह नफरत उजागर हो जाती है ,जहां साफ तौर पर यह लिख दिया जाता है कि - 'जो अपनी पहचान प्रगतिशील, सिविल सोसायटी या लिबरल के रूप में चाहते हैं,एनजीओ, मानवाधिकार, साहित्यिक व कला मंच जिनके माध्यम है,एक दूसरे को मैग्सेसे व उनके समकक्ष पुरुस्कार दिलाना जिनकी फितरत है,पत्रकारिता,पुस्तक ,फ़िल्म जिनके आतंक फैलाने के हथियार है,असहिष्णुता व अभिव्यक्ति की आज़ादी जिनके प्रिय जुमले हैं,प्राध्यापक, पत्रकार, अधिवक्ता व एक्टिविस्ट होना जिनका पैसा है,जनसुनवाई और आरटीआई जिनके माध्यम है ,प्रधानमंत्री, भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो अपना शत्रु मानते हैं,जिन्हें वाममार्गी,माओवादी ,कम्युनिस्ट कहा जाता है,परन्तु एक ही शब्द का सम्बोधन देना हो तो वह है- अरबन नक्सल ।
यह प्रचार पुस्तिका सलवा जुडूम की भूरी भूरी प्रशंसा करती है,महेंद्र कर्मा को बार बार उद्धरित करती है ,बस्तर के पूर्व आईजी कल्लूरी के श्रीमुख से कहलवाती है कि -'बस्तर से नक्सली सालाना 1100 करोड़ की वसूली करते हैं,यह पैसा उन माओवादियों को नहीं मिलता है,जो हथियार लेकर जंगल मे आंधी पानी और मलेरिया से जूझ रहे हैं,यह पैसा पहुंचता है नक्सलियों के अरबन नेटवर्क के पास,ये एक छोटा वर्ग है जो गैर सरकारी संगठन व मानव अधिकार के नाम पर ,अध्येता या शोधार्थी के नाम पर इस दावे के साथ बस्तर में मौजूद होता है कि हम वहां काम कर रहे हैं।'
पुस्तिका कईं सामाजिक कार्यकर्ताओं,पत्रकारों,लेखकों,रंगकर्मियों ,प्राध्यापकों को शहरी सफेदपोश नक्सली के रूप में चिन्हित करती है,उनकी नजर में मेधा पाटकर,अरुंधति रॉय,स्वामी अग्निवेश,राहुल पंडिता,अरुणा रॉय ,नंदिनी सुंदर जैसे लोग अरबन नक्सल है ,वरवर राव,सुधा भारद्वाज,अरुण फरेरा, गौतम नवलखा,वेरनन गोंजाल्विस,फादर स्टेन स्वामी,सुसान अब्राहम,आनंद तेलतुंबड़े ,कबीर कला मंच,यलगार परिषद तो है ही।
इन्हें भीमा कोरेगांव का दलित गौरव और आदिवासियों का पत्थलगढ़ी का आंदोलन भयानक नक्सली साज़िश लगती है ,यह जेएनयू को देशद्रोह का अड्डा और टुकड़े टुकड़े गैंग,अवार्ड वापसी गैंग ,पाकिस्तान परस्त,मुस्लिमों के प्रति प्रेम से भरे हुए,भारत विरोधी व हिन्दू विरोधी जैसे विशेषणों से तो सबको नवाजते ही हैं।
इस दुष्प्रचार पुस्तिका के मुताबिक- "वाम विचार प्रेरित आतंकवाद के लिए बड़े शहरों के साहित्यक,विश्वविद्यालय व अन्य बौद्धिक मंच,कला ,मीडिया ,पत्रकार और यहां तक कि फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े पढ़े लिखे ,किंतु उसी विचार को मानने वाले लोग,जो प्रोपेगैंडा कर जन असंतोष को भड़का कर नक्सलवाद के पक्ष में माहौल बनाते हैं।इन्हीं लोगों को अरबन नक्सल कहा गया है।"
पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर बॉक्स में एक लघु आलेख किन्ही यादवेन्द्र सिंह द्वारा लिखित प्रकाशित है, जिसका शीर्षक इस प्रकार है-
" राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अरबन नक्सल की आहट"
इस आलेख में कहा गया है कि "राजस्थान के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय को पूर्व योजना के मुताबिक अरबन नक्सल वाद का अड्डा बनाया जा रहा है,यहां का सोशल वर्क डिपार्टमेंट कईं बार निखिल डे को व्याख्यान हेतु बुलाता है,जो कि मजदूर किसान शक्ति संगठन में अरुणा राय के सहयोगी है व अरबन नक्सल को बढ़ावा दे रगे है। कल्चर व मीडिया विभाग से प्रतिवर्ष इंटर्न्स mkss भेजते हैं"। किताब के अंदरूनी मुखपृष्ठ पर एक कार्टून के साथ "मी टू अरबन नक्सल" वाली फ़ोटो भी छापी गयी है,जिसमें प्रशांत भूषण,अरुंधति रॉय,अरुणा रॉय व जिग्नेश मेवाणी आदि नजर आते है।
कुल जमा इस प्रचार पुस्तिका के ज़रिए राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश की सिविल सोसायटी व जन आंदोलन के चेहरों को शहरी माओवादी के रूप में प्रचारित करके उनके विरुद्ध आम जन के मानस में घृणा,विद्वेष फैलाना है,उनके काम पर सवालिया निशान लगाते हुए उनके बारे में दुष्प्रचार करना है,ताकि ये लोग और इनके संगठन गरीब,दलित,मजदूर,किसान ,आदिवासी व पीड़ित अल्पसंख्यकों के साथ एकजुटता में खड़े न हो सके।
यह दुष्प्रचार काफी वक्त से जारी है,जब इस तरह की असत्य बातें एक सुनियोजित षड़यंत्र के तहत लोगों के बीच प्रचारित कर दी जाती है तो उसका परिणाम मॉब लिंचिंग और हमलों व हत्याओं के रूप में सामने आती है।
यह बहुत भयानक स्थिति है,इस उकसाने व भड़काने वाली ,नफरत पैदा करने वाली कार्यवाही की भर्त्सना की जानी चाहिए, ऐसी दुष्प्रचार प्रोपेगैंडा पुस्तिकाओं के प्रकाशकों व लेखकों के ख़िलाफ़ कानून सम्मत कार्यवाही होनी चाहिए,अन्यथा इस प्रकार की प्रवृति बढ़ेगी और सामाजिक न्याय व बदलाव के काम ग्रासरूट पर करना दूभर हो जाएगा। इससे यह सवाल भी उठना स्वाभाविक है कि आरएसएस क्यों अपने प्रचार विभाग के ज़रिए इस प्रकार का साहित्य प्रचारित करवा रहा है,उसका क्या हिडन एजेंडा है,वह किसके हित साध रहा है,क्या यह पूंजीवाद और सांप्रदायिकता के गर्भनाल रिश्तों को मजबूती देने की कोशिश है या जीवन लगा देने वाले सेवा भावी सामाजिक कार्यकर्ताओं को जानबूझकर बदनाम करने का प्रयास ?
कुछ न कुछ तो है !
|
|
|
स्वास्थ्य संकट पर रिपोर्टिंग करती पत्रकारिता को टेटेनस हो गया है, टेटभैक का इंजेक्शन चाहिए
रवीश कुमार
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि मुज़फ़्फ़रपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कालेज अस्पताल में एक साल के भीतर 1500 बेड जोड़े जाएंगे। जिसे बढ़ा कर 2500 बेड का कर दिया जाएगा। अस्पताल 49 साल पुराना है। इस वक्त 610 बेड है।
उसी अस्पताल के कैंपस में एक सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल बन रहा है जो शायद तैयार होने के करीब है। जिसमें 300 बेड होगा। अगर इसे 610 में जोड़ लें तो जल्दी ही 910 बेड बन कर तैयार हो जाएगा। उसके बाद 600 अतिरिक्त बेड इस अस्पताल में बनाने के लिए कम से कम दो अस्पताल बनाने होंगे। फिर 2500 का टारगेट पूरा करने के लिए दो और बनाने होंगे। वैसे हमें नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री ने साल भर के भीतर 1500 बेड बनाने का एलान किया है उसमें पहले से बन रहे 300 बेड के अस्पताल का हिसाब शामिल है या नहीं।
एक सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल के लिए एक बेड की लागत 85 लाख से 1 करोड़ आती है। इस लागत में इमारत और उसमें होने वाली हर चीज़ और डाक्टर की लागत शामिल होती है। अगर 1500 बेड बनेगा तो नीतीश कुमार सरकार को एक साल के भीतर 1500 करोड़ ख़र्च करने होंगे।
2017-18 में बिहार सरकार का बजट ही 7002 करोड़ का था। जो 2016-17 की तुलना में 1000 करोड़ कम हो गया था। अस्पतालों के निर्माण का बजट करीब 800 करोड़ था। क्या बिहार से बीमारियां भाग गईं थीं जो हेल्थ का बजट 1000 करोड़ कम किया गया? ये जानकारी पॉलिसी रिसर्च स्टडीज़ की साइट से हमने ली है।
अगर एक यात्रा में नीतीश कुमार अख़बारों में हेडलाइन के लिए 1500 से 2500 करोड़ के बजट के अस्पताल का एलान कर गए तो यह भी बता देते कि पैसा कहां से आएगा। इस बजट में तो पूरे बिहार का बजट ही समाप्त हो जाएगा। 130 बच्चों की मौत की संख्या छोटी करने के लिए 2500 बिस्तरों का एलान घिनौना लगता है। शातिर दिमाग़ का खेल लगता है। सबको पता है कि पत्रकार पूछेंगे नहीं कि पैसा कहां से आएगा। एक ही कैंपस में 5 अस्पताल का एलान क्यों कर गए? 2500 बिस्तर का मतलब आप 500 बेड के हिसाब से देखें तो 5 अस्पताल बन सकते हैं। क्या इन 5 अस्पतालों को आप आस-पास के ज़िले में नहीं बांट सकते थे? जिससे सबको मुज़फ़्फ़रपुर आने की ज़रूरत न होती और लोगों की जान बचती?
610 बेड के अस्पताल के लिए तो अभी डॉक्टर नहीं हैं। यही नहीं 49 साल पुराने श्री कृष्ण मेडिकल कालेज अस्पताल में पिडियाट्रिक की पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई नहीं होती है। अगर यहां पीजी की दस सीट भी होती तो कम से कम 40 जूनियर या सीनियर रेज़िडेंट तो होते ही। बिहार के प्राइवेट कालेज में जो बाद में खुले हैं वहां पीजी की सारी सीटें हैं क्योंकि उनसे करोड़ रुपये की सालाना फीस ली जाती है।
आम तौर पर तीन बेड पर एक डॉक्टर होना चाहिए। अगर 1500 बेड की बात कर रहे हैं तो करीब 200-300 डॉक्टर तो चाहिए ही।बेड बनाकर फोटो खींचाना है या मरीज़ों का उपचार भी करना है। जिस मेडिकल कालेज की बात कर गए हैं वहां मेडिकल की पढ़ाई की मात्र 100 सीट है। 2014 में हर्षवर्धन 250 सीट करने की बात कर गए थे। यहां सीट दे देंगे तो प्राइवेट मेडिकल कालेजों के लिए शिकार कहां से मिलेंगे। गेम समझिए। इसलिए नीतीश कुमार की घोषणा शर्मनाक और मज़ाक है। अस्पताल बनेगा उसकी घोषणा पर मत जाइये। देश में बहुत से अस्पताल बन कर तैयार हैं मगर चल नहीं रहे हैं। गली-गली में खुलने वाले एम्स की भी ऐसी ही हालत है।
2018 में बिहार सरकार ने एक और कमाल का फैसला किया। पटना मेडिकल कालेज में 1700 बेड हैं। इसे बढ़ाकर 5462 कर दिया जाएगा। ऐसा करने से यह दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बन जाएगा। इसके लिए 5500 करोड़ का बजट रखा गया। चार-पांच साल में बनकर तैयार हो जाएगा। यह बना तो बेलग्रेड के सबसे बड़े अस्पताल से आगे निकल जाएगा। ज़रूर कोई अफसर रहा होगा जो बी से बेलग्रेड और बी से बिहार समझा गया होगा और सबको मज़ा आया होगा। इसी बेड को अगर आप पूरे बिहार में बांट देते तो कई ज़िलों में एक एक अस्पताल और बन जाते। इसके लिए पटना मेडिकल कालेज की पुरानी ऐतिहासिक इमारतें ढहा दी जाएंगी।
पटना में पीएमसीच के अलावा इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज भी है जिसे एम्स कहते हैं। यह आज तक दिल्ली के एम्स का विकल्प नहीं बन सका है। यहां भी नीतीश कुमार ने इसी जून महीने में 500 बेड का उद्घाटन किया था। पटना के लिए पीएमसीएच और एम्स काफी है। रिकार्ड बनाने से अच्छा होता 5462 बेड को पूरे बिहार में बांट देते तो किसी को सहरसा और आरा से पटना नहीं आना पड़ता। लेकिन अस्पताल भी अब 300 फीट की मूर्ति की सनक की तरह बनने लगे हैं।
फिर भी आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि 5462 बेड के अस्पताल के लिए 1500 डाक्टर कहां से लाओगे। पीएमसीच में ही 40 परसेंट डाक्टर कम हैं। बिहार में 5000 डाक्टरों की कमी है। क्या इसके लिए नीतीश कुमार सरकारी कालेजों में मेडिकल की सीट बढ़वाने वाले हैं या प्राइवेट मेडिकल कालेज खोल कर कमाने की तैयारी हो रहा है। डॉक्टर सरकारी मेडिकल कालेज क्यों ज्वाइन करेगा। एक एक करोड़ की फीस देकर एम बी बी एस करेगा और दो दो करोड़ में पीजी तो वह सरकारी कालेज में क्यों जाएगा। अपने पैसे को वसूल कहां से करेगा। आप जानते हैं कि जो भी नीट से पास करता है उसे मजबूरन इन प्राइवेट कालेज में जाना पड़ता है। ग़ुलामी का यह अलग चक्र है जिसे समाज ने सहर्ष स्वीकार किया है। प्राइवेट कालेजों का शुक्रिया कि एक करोड़ ही पांच साल का ले रहे हैं वर्ना यह जनता सरकार से सवाल किए बग़ैर पांच करोड़ भी दे सकती थी।
श्री कृष्ण मेडिकल कालेज में जो डाक्टर साढ़े चार साल की पढ़ाई के बाद इंटर्नशिप कर रहे हैं उन्हें ढाई महीने से सैलरी नहीं मिली है। 15000 रुपये मिलते हैं। हो सकता है पूरे बिहार के इंटर्न की यही हालत हो। ज़ाहिर है बिहार सरकार के पास पैसे नहीं होंगे। तो फिर फिलहाल आप सभी जनता 2500 बिस्तर की घोषणा से काम चलाइये।
हरियाणा के झज्जर में नेशनल कैंसर इस्टिट्यूट NCI बन रहा है। इसकी योजना मनमोहन सरकार में बनी थी। मगर चुनाव के समय ही ख़्याल आया और जनवरी 2014 में मनमोहन सिंह ने इसकी आधारशिला रखी। अगले एक साल तक कुछ नहीं हुआ। 2015 के आखिर में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जे पी नड्डा भूमि पूजन करते हैं। आधारशिला और भूमिपूजन में आप अंतर कर सकते हैं। 23 अक्तूबर 2016 को जे पी नड्डा ट्वीट करते हैं कि 2018 में अस्पताल चालू हो जाएगा। 710 बेड के इस अस्पताल को एम्स की निगरानी में बनवाया जा रहा है जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय भी मॉनिटर करता है। जब दिसंबर 2018 में इस अस्पताल की ओ पी डी चालू की गई तो 710 बेड का कहीं अता-पता नहीं था। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जब इसका उद्घाटन करते हैं तो 20 बेड ही तैयार था। आज भी बेड 20 के ही आस-पास हैं। चुनाव करीब था, हेडलाइन लूटनी थी तो एलान हो गया।
जब यह अस्पताल तीन साल में 20 बेड से आगे नहीं जा सका, 710 बेड नहीं बना सका, कैंसर के कितने ही मरीज़ उपचार के ख़र्चे और कर्ज़े में डूब कर मर जाते हैं, तब नीतीश कुमार 2500 बेड बनवा देंगे। 1500 बेड एक साल में बनवा देंगे। चार साल में पटना में 5462 बेड का अस्पताल बनवा देंगे। पूरे राज्य का स्वास्थ्य बजट इन दो घोषणाओं को पूरा करने में ही खप जाएगा।
आप इन जानकारियों का क्या कर सकते हैं? इसे लेकर टीवी एंकरिंग क्या ही करेंगे। पत्रकारिता को टेटेनेस हो गया है। टेटभैक का इंजेक्शन भी काम नहीं करेगा। बेहतर है इन तथ्यों को भावुक वाक्य विन्यासों में मिलाकर चीखें। पुकारें लोगों को। स्क्रीन पर दरीदें वगैरह लिखें। मुज़्फ़्फ़रपुर की जनता या बिहार की जनता जब एक कैंपस में 30 से अधिक बच्चियों के साथ हुए बलात्कार पर सड़क पर नहीं आई तो 130 बच्चों की मौत पर क्यों आएगी? हम मौत को भावुकता और आक्रोश में बदल रहे हैं वो भी एक दो लोगों से आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्या तथ्यों पर आधारित ये सवाल कुछ बदलाव कर सकते हैं? इसका जवाब मुझे नहीं मालूम। तब तक आप चीखते रहें।
बोलने वाले बोलते क्यों नहीं ?
ओम थानवी
लोग पूछते हैं, राजग को प्रचंड जनादेश मिला है। आप अब भी आलोचक क्यों हैं? कोई बताए कि क्या जनादेश आलोचना का हक़ छीन लेता है?
मेरा गिला राजनेताओं से उतना नहीं, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों की अपनी ही बिरादरी से है। आपको याद होगा, जब पत्रकार मोदी के गिर्द सेल्फ़ी के लिए झूमने लगे, उनकी कितनी फ़ज़ीहत हुई थी। पर आज घर बैठे जयकारे लगाने में भी उन्हें (या साथियों को) कोई झिझक नहीं।
किसे शक कि मोदी की वक्तृता बहुत लोक-लुभावन है। लिंग-दोष के बावजूद शब्दों और अभिव्यक्ति के हुनर पर उनका अधिकार है। उनका आत्मविश्वास और बढ़ा है। मगर साथ में अहंकार भी: "मोदी ही मोदी का चैलेंजर (चुनौती) है"!
जो हो, परसों के सुदीर्घ भाषण में "छल को छेदना है" जुमला सुनकर पत्रकार मित्र इतने फ़िदा हुए कि तमाम पुराने वादों की पोल, बड़ी पूँजी के बढ़ावे, कालेधन की मरीचिका, बेक़ाबू महँगाई और बेरोज़गारी, नोटबंदी-जीएसटी के प्रकोप में उद्योग-व्यापार और खेतीबाड़ी के पतन, किसानों के आत्मदाह, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विचलन, शासन में संघ परिवार के दख़ल, रफ़ाल के रहस्य, पुलवामा की विफलता और बालाकोट के रेडार के छल तक को भुला गए।
प्रधानमंत्री ने ग़रीबी और ग़रीबों की बड़ी बात की। संविधान पर श्रद्धा उँडेली। क्या 2014 संविधान न था? या महँगाई, ग़रीबी और बेरोज़गारी? क्या संविधान की शपथ में उसके प्रति आदर और ज़िम्मेदारी का तत्त्व निहित नहीं होता है? फिर यह दिखावा क्यों?
उन्होंने राजग के साढ़े तीन सौ मौजूद सांसदों (और प्रकारान्तर छोटे-बड़े अन्य नेताओं) को "छपास और दिखास" से आगाह किया। पर इसके सबसे आला प्रमाण तो वे ख़ुद हैं। रोज़ कौन बंडी-कुरते बदलता है? कैमरा-क्रू के साथ जाकर कौन केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाता है? बग़ैर मुखारविंद खोले लाइव प्रेस काँफ़्रेंस में और कौन आ बैठता है? कभी मीडिया से बेरुख़ी और कभी साक्षात्कारों की झड़ी कौन लगा देता है? तो, इस एकाधिकार में अपने सहयात्रियों को उनका संदेश आख़िर क्या है? बस यही, कि आप सब परदे में रहें। मैं हूँ ना।
अपने भाषण में ठीक एक घंटे बाद जाकर उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात की। पत्रकार मित्र इस समावेशी पुट पर और लट्टू हुए हैं। मोदी अचानक उनके लिए सर्वधर्मसमभावी हो गए। कितने आराम से पत्रकार भूल गए कि प्रधानमंत्री ही पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब वहाँ क़त्लेआम हुआ।
पिछले चुनाव में उन्होंने श्मशान-क़ब्रिस्तान का राग छेड़ा था। इस दफ़ा पाकिस्तान (जिसे चुनाव बाद के भाषण में सिरे से छिटका दिया) और सर्जिकल के शोर के पीछे हिंदू राष्ट्रवाद की पुकार थी। और अभी, सेंट्रल हॉल में, उनके सामने बैठे भाजपा के नवनिर्वाचित सांसदों में एक भी मुसलमान नहीं था।
आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह, संगीत सोम आदि के साथ अब आतंक की मौतों वाले मालेगांव बमकांड की ज़मानतयाफ़्ता साध्वी प्रज्ञासिंह पार्टी की शोभा बढ़ा रही है। गांधीजी के हत्यारे गोडसे को उसने देशभक्त कहा। चुनाव का नाज़ुक दौर था, मोदी ने कहा वे साध्वी को माफ़ नहीं करेंगे। पर पार्टी के मार्गदर्शक आडवाणी ने साध्वी के सर पर हाथ रख दिया है।
क्या ऐसे क्षुद्र और कट्टर ‘नेताओं’ को साथ रखकर जीतेंगे मोदी अल्पसंख्यकों का विश्वास? इन्हें साथ लेकर घृणा और सांप्रदायिकता की क्या वही हरकतें नहीं होंगी, जो पिछले पाँच दिनों में मुसलमानों के साथ हिंसा की वारदातों में लगभग हर रोज़ हुई हैं?
गाय के नाम पर हत्याएँ जब पहले बढ़ीं तब हिंसक तत्त्वों को प्रधानमंत्री ने देर से सही, पर चेतावनी दी थी। लेकिन उसे उन तत्त्वों ने मानो आशीर्वाद समझा और बेख़ौफ़ अपने मन और (कथित गोरक्षा) मत के वशीभूत सामूहिक हिंसा करते चले गए। उन्होंने मुसलमानों और दलितों पर कायराना नृशंस अत्याचार के वीडियो भी बेख़ौफ़ प्रचारित किए। समाज के ताने-बाने को द्वेष और दुष्प्रचार से उधेड़ने वाला इससे घृणित काम और क्या होगा?
गुज़रे पाँच सालों में दादरी से राजसमंद तक मुसलमानों के साथ इतना ख़ूनख़राबा हो गया है कि देश के नागरिक के नाते मोदी सरकार से उन्हें "भ्रम और भय" के अलावा कोई विश्वास हासिल नहीं हुआ है। अब उन्होंने अगर समावेशी समाज और विश्वास की बात की है तो हमें ज़रूर इसे एक बार उम्मीद की नज़र से देखना चाहिए।
लेकिन छल-छलावे और संदेह के ऐसे विकट परिवेश में लट्टू पत्रकारिता से किस सरोकारी को कोफ़्त न होगी, जिसका ज़िक्र मैंने शुरू में किया। इसीलिए मुझसे कहे बिना रहा न गया। हालाँकि अब नए काम में टीका करने को वक़्त कहाँ मिलता है।
राजनीति की दशा जैसी हो, बोलने वालों को ज़रूर बोलना चाहिए। विवेकशील पत्रकार और बुद्धिजीवी अपना मनोबल क्यों खोएँ?
समाचार पत्र में नमो नम: चलेगा तो जनता की सुध कौन लेगा?
शिरीष खरे कभी तहलका में मध्यप्रदेश के प्रभारी थे. तहलका के बाद उन्होंने राजस्थान पत्रिका में अपनी सेवाएं दी और तबादले में छत्तीसगढ़ आ गए. यहां आकर उन्होंने कई मसलों पर गंभीर रिपोर्टिंग की. विशेषकर आदिवासी मामलों पर उनकी कलम खूब चली. इन दिनों वे पुणे में हैं और एक स्वयंसेवी संस्था के लिए कार्यरत हैं. अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मशहूर श्री खरे ने अपना मोर्चा डॉट कॉम के लिए यह खास टिप्पणी भेजी है. इस टिप्पणी में उन्होंने माना है कि मीडिया में फिलहाल साष्टांग और दंडवत होने खौफनाक का दौर चल रहा है.
लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नरेन्द्र मोदी की जीत ने 'राजस्थान पत्रिका समूह' के स्वामी गुलाब कोठारी का हृदय परिवर्तन कर दिया है। यही वजह है कि टेलीविजन पर मोदी का वक्तव्य सुनने के बाद उन्होंने अपने समाचारपत्र में मोदी के नाम एक भक्तिमय संपादकीय लिखा है। यहां उन्हें मोदी की वाणी में सरदार पटेल और महात्मा गांधी से लेकर विवेकानंद सब साथ-साथ नजर दिखाई दिए। 'राजनीति के समुद्र में क्षीरसागर की थाह नापने' टाइप भावपूर्ण भूमिका बांधने के बाद अचानक ही वे मुद्दे पर आ जाते हैं। कहते हैं कि राजस्थान पत्रिका का मूल क्षेत्र राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से आपकी भावी योजनाओं के साथ समर्पित है। इस तरह, वे खुद को निसंकोच और बेझिझक मोदीजी के लिए समर्पित कर देते हैं। इस तरह, अगले पांच वर्ष सरकारी विज्ञापन और कारोबार को देखते हुए नई सरकार के सामने साष्टांग दंडवत होने में वे कोई दुविधा महसूस नहीं करते हैं।
देखा जाए तो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही लगभग पूरे के पूरे मीडिया के बिकने और मोदी की गोद में बैठकर मोदी के प्रचार में काम करने की यही कहानी है। लेकिन, गुलाब कोठारी की बात दूसरी है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने सरकार की स्तुति में जो घोषणा की है, वैसी घोषणा किसी ने नहीं की है।
यहां तक कि रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज और इंडिया टीवी से लेकर दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे तमाम मीडिया संस्थान जो चुनाव अभियान के दौरान मोदी के प्रचार में बढ़-चढ़कर आगे रहते हैं, उन्होंने भी कभी सीधे-सीधे मोदी के पक्ष में खड़े होने का ऐलान नहीं किया। लेकिन, गुलाब कोठारी ने दूसरी बार मोदी के बहुमत हासिल करने के मौके पर जिस तरह से खुद को प्रोजेक्ट किया है, उससे स्पष्ट कि अब वे मोदी भक्ति की होड़ में सबसे आगे आना चाहते हैं।
चुनाव के दौरान सबने देखा कि किस तरह से मीडिया संस्थानों ने प्रधानमंत्री के साक्षात्कार, भाषण और धार्मिक यात्रा का कवरेज किया और विपक्षी दलों सहित उनके मुद्दों को अदृश्य बनाए रखा। ठीक इसी अंदाज में अब यदि कोठारी अपने समाचारपत्र को मोदी के संकल्प के लिए समर्पित कर देंगे तो सवाल है कि समाचार, प्रचार और प्रोपेगंडा के बीच के अंतर कहां रह जाएगा? इस कार्यकाल में समाचारपत्र सिर्फ 'नमो नम:' करेगा तो जनता की सुध कौन लेगा?
अंत में कोठारी की यह टिप्पणी अपने संस्थान के सभी कर्मचारी पत्रकारों को यह स्पष्ट संदेश है कि उन्हें अब न मंहगाई देखनी है, न बेकारी, न बदहाल अर्थव्यवस्था और अपराध-आतंकवाद, अब आपको कीबोर्ड की जगह घंटी बजानी है और अपने स्वामी के भी स्वामी की भक्ति में मन रमाना है।
अखबार की पलटीमार परम्परा !!
गिरीश पंकज
बंदर जैसी गुलाटी मारने की कला कभी-कभी किसी अखबार विशेष से भी सीखी जा सकती है। राजस्थान से निकलने वाले एक बड़े अखबार को हम ताज़ा उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। इसके मालिक एक तरफ नैतिकता की बड़ी-बड़ी बातें करते रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के अखबार में निकृष्ट किस्म के अश्लील विज्ञापन भी छपते रहे हैं। मैं उनके इस पाखंड को देखकर शुरू से चकित रहा हूं कि ईमानदारी और बेईमानी के बीच आखिर कैसे इतना " सुंदर" संतुलन बनाकर ये पत्रकारिता कर रहे हैं। इस अखबार के पिछले कुछ सालों का ट्रैक- रिकॉर्ड भी जब हम देखते हैं, तो चकित रह जाना पड़ता है। इस अखबार का मालिक हर रविवार को बेहतर मनुष्य बनने के जीवन- दर्शन का मंत्र पढ़ाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ राग दरबारी भी गाता है। कमाल है। सत्ता के साथ सुर बदलने की कला इस देश में कुछ पत्रकारों में स्पष्ट नजर आती है। यह अखबार भी इसी परंपरा का अनुगामी है।
वर्तमान लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के पहले तक राजस्थान के इस अखबार में कांग्रेस का गुणगान अधिक नजर आता था। पर्याप्त लाभ न मिलने के कारण शायद इनके सेठ मोदी सरकार से कुछ खार भी खाए हुए थे। छत्तीसगढ़ से जब यह अखबार शुरू हुआ, तब भाजपा की सरकार थी। उस वक्त इनको विज्ञापन मिलने में दिक्कत होने लगी, तो उन्होंने भाजपा के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। जितना हो सकता था, भाजपा सरकार को कोसने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हमारे जैसे अनेक लोगों को लगता था कि वाह, क्या अखबार है । इनकी पत्रकारिता के क्या कहने! लेकिन बहुत बाद में पता चला कि मामला कुछ और है। विज्ञापन न मिलने के कारण इनके अंदर की पत्रकारिता उफन कर बाहर आ रही है। लेकिन जैसे ही बाद में इनको सरकार की ओर से विज्ञापनरूपी टुकड़े डाले जाने लगे, तो अखबार ने अपने सुर भी बदलने शुरू कर दिए। और हालत यह हुई कि ईमानदारी से पत्रकारिता करने वाले कुछ लोगों को इसी अखबार ने हटाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया क्योंकि ये पत्रकार भाजपा सरकार की गलत हरकतों के विरुद्ध खबरें लिख रहे थे। अखबार की इस घटिया कार्रवाई के विरुद्ध मैंने उस वक्त भी प्रतिवाद किया था कि यह कौन-सी पत्रकारिता है कि जो सरकार के खिलाफ लिख रहा है, उस रिपोर्टर को आप अपने अखबार से बाहर का रास्ता दिखा दे क्योंकि आपको सरकार के विज्ञापन चाहिए?
इसी अखबार ने मोदी सरकार के आने के बाद तो यकायक यू-टर्न सा ही ले लिया है ।जैसे ही इस चुनाव में मोदी को अप्रत्याशित बहुमत मिला, तो इस अखबार के मालिक ने फौरन पलटी मार ली । 25 मई के अंक में उन्होंने प्रथम पृष्ठ पर बड़ी उदारता के साथ मोदी-वंदना की है। उनकी टिप्पणी की भाषा पढ़ कर सामान्य पाठक भी समझ गया कि अखबार मालिक कितना बड़ा मक्खनबाज़ है,विचारबदलू है । वैसे यह किसी एक अखबार की बात नहीं है। इस देश में समय-समय पर कुछ अखबार सत्ता के अनुसार पाला बदलते रहे हैं। इस अखबार ने भी उसी पलटीमार -परंपरा का निर्वाह किया है। इस अखबार के बारे में पहले से भी लोग यह कहते रहते हैं कि जब जब सरकारें बदलती है इस अखबार के सुर भी बदलते रहते हैं। शायद यह समय-सापेक्ष-पत्रकारिता का नया फंडा है कि जिधर बम,उधर हम। आर्थिक दृष्टि से बम-बम रहने के लिए मीडिया की यह 'घुटनाटेक पत्रकारिता' अंततः पत्रकारिता का ही नुकसान करेगी। पत्रकार को निष्पक्ष होकर , तटस्थ होकर पत्रकारिता करनी चाहिए, न किसी दल के साथ राग और न किसी दल के साथ द्वेष। यही उस का मूल मंत्र होना चाहिए। अगर इस भावना से पत्रकारिता होगी तो सरकार किसी की भी रहे, अखबार निर्भीक हो कर उसके खिलाफ लिख सकेगा। बिकी हुई पत्रकारिता सत्ता को आईना नहीं दिखा सकती। और जब और राग दरबारी गाने लगती है, तो बुरी तरह एक्सपोज़ भी हो जाती है।
वैसे ऐसा नहीं है कि यह इकलौता अखबार है ।अनेक अखबार समय-समय पर सुर बदलते रहते हैं । अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पलटीमार-चरित्र भी साफ-साफ नजर आने लगा है । दस दिन पहले तक जिन चैनलों को लग रहा था कि नरेंद्र मोदी की वापसी संभव नहीं है, तो वे नरेंद्र मोदी को कोसते नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी बहुमत में आए, इन चैनलों के सुर बदल गए। यानी मोदी शरणम गच्छामि हो गए। पत्रकारिता तो किसी भी तरह की लाभ हानि की भावना से उठकर की जाने वाली साधना है लेकिन अब शायद पत्रकारिता को मिशन समझने वाला वह दौर ही नहीं रहा। जिस दौर को देखते और जीते हुए कुछ लोग पत्रकारिता किया करते थे ।
गुलाब की पत्तियों के बीच दुबका लोकतंत्र
नथमल शर्मा
बिलासपुर। देश में आम चुनाव हो रहे हैं । दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम अगले पांच बरस के लिए अपनी सरकार चुन रहे हैं । चार चरण पूरे हो चुके हैं और आधी से ज्यादा (374) लोकसभा क्षेत्रों के जनादेश मुहरबंद हो चुके हैं । इन तीन सौ चौहत्तर क्षेत्रों के करोड़ों लोग बाएं हाथ की उंगली पर अमिट स्याही लगाकर खुश हैं (शायद)। परिणाम आते तक इनकी ऊंगलियों से स्याही के निशान मिट चुके होंगे । वैसे तो इस ये चुनाव कोई निशान ही नहीं छोड़ रहा । देश के आम चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं है । यह सबसे गंभीर और भयावह है । लोगों को किस तरह "चुप समाज" में बदल दिया गया है ।
नोटबंदी की नाकामी ,जीएसटी की उलझनों, पंद्रह लाख रुपये के जुमले (?) से शुरू हुई चर्चा राफेल तक आकर ठहरी और फ़िर कोर्ट-कचहरी में उलझकर रह गई । शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, महंगाई, रोजगारी, खेती-किसानी, काला धन, विकास, पीने का साफ़ पानी, सफ़ाई के लिए तरसते मोहल्ले और गांव-शहर भी । इन सब मुद्दों पर अभी तक तो कोई चर्चा नहीं हुई । देश के आम चुनाव में सारे बिंदु मोदी - मोदी में आकर समाहित हो गए। सिमट कर रह गए । यहां तक कि शहजादा,नामदार, पप्पू भी चर्चा से गायब । चोर से चौकीदार को अलग करते हुए चौकीदार को प्रचार ले उड़ा । और चोर कह रहे देखते ही रह गए । देख भी रहे हैं । पिछली बार चाय वाला कहा तो वही प्रचार ब्रांड हो गया । इस बार चौकीदार । ये है हमारे देश का आम चुनाव । राजनीतिक दलों ने घोषणा पत्र बनाए । चुनाव के दो - चार दिन पहले जारी किए । लेकिन सिवाय दो चार लोक-लुभावन घोषणाओं के किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई । यानी कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा,तृणमूल, आदि ने भी अपने-अपने घोषणा पत्रों पर पूरी गंभीरता से चर्चा नहीं की । यहां तक इन दलों के कार्यकर्ताओं को तो छोड़िए नेताओं को भी पूरा घोषणा पत्र पता नहीं होगा । जाहिर है इस पर भाषणों में तो बात होती ही नहीं ।और अपने देश में समाज के बौद्धिक वर्ग , पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं किसी को भी ये जरूरी ही नहीं लगता कि राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों पर गंभीरता से चर्चा की जाए ।
इस चुनाव में चर्चा है मोदी- मोदी । यानी अगले पांच बरस के लिए अपनी सरकार चुनने में हमें व्यक्ति को चुनना है । मज़े की बात यह भी कि इस बार तो भाजपा ने खुद को मोदी से छोटा कर लिया है । भाजपा के विज्ञापनों में यही नारा है "अबकी बार मोदी सरकार " । यह नारा "अबकी बार भाजपा सरकार " भी तो हो सकता था । होना ही था । लेकिन नहीं । अब हम अपने लोकतन्त्र को व्यक्ति की गोद में बैठाने तैयार हैं । दुखद यह कि कांग्रेस और बाकी विरोधी दलों ने इस पर एक शब्द नहीं कहा । शायद इसलिए कि इनका कहा बूमरेंग हो जाता ।कांग्रेस,सपा,बसपा,तृणमूल,बीजद, जैसे दलों से भी तो आंतरिक लोकतंत्र कब का खत्म हो गया । ये सब दल भी तो एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द ही है । लोकतंत्र का दम भरने वाले हम मतदाताओं, जागरूक नागरिकों ने कहां पहुंचा दिया है लोकतंत्र को । जहां लोक हाशिये पर है और व्यक्ति का तंत्र हावी है ।
ऐसे माहौल में हो रहे हैं देश में चुनाव । ध्यान देने लायक बात यह भी है कि लोगों में भी इस पर कोई गंभीर बात नहीं होती । हम भारतीय खूब राजनीतिक चर्चा करते हैं । हर व्यक्ति देश के तमाम राज्यों का विश्लेषण कर देता है । चुनावी मुद्दों की गंभीरता समझनी हो तो चुनाव प्रबंधन सम्हाल रहे नेताओं से बात करिये । लगेगा कि बाकी सब बेकार की बातें हैं । सबसे बड़ी बात है जाति । किस क्षेत्र या गांव में किस जाति के लोग कितने है और वह किसे वोट देंगे । बस सारा गणित इसी पर । अब देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ आए । चुनावी भाषणों में बताया कि गुजरात में तेली ही मोदी है । जैसे छत्तीसगढ़ में साहू वैसे गुजरात में मोदी । यानी यहाँ के साहू हमारे । किसी चुनाव में देश के प्रधानमंत्री को अपनी जात बताना पड़ जाए । गज़ब है । ये तो एक उदाहरण ही है । हर गांव, शहर में चुनावी आकलन इसी के आस-पास ही तो है । कुर्मी किस तरफ़ ज्यादा वोट करेंगे या कि ठाकुर, ब्राह्मण किसे वोट दे रहे हैं । मुस्लिम किसके वोट बैंक हैं तो अन्य जातियां किस किसको वोट कर रही है । ये तो हालात है । और हम लोकतंत्र के जिम्मेदार नागरिक होने का दंभ पाले उंगलियों में निशान लगवा रहे हैं ।
जाति के अलावा धर्म भी एक अघोषित तौर पर घोषित मुद्दा ही है । तभी तो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अली बली कहने का साहस (दुस्साहस) करता है तो कोई नेत्री बजरंग बली को दलित जाति की बता देतीं हैं । कोई नेता किसी के अंतर्वस्त्रों की निम्न बात भी करता है तो कोई नेत्री अपने क्षेत्र में जूते बांटती है और उसी की प्रतिद्वंद्वी नेत्री इस जूते बांटने को क्षेत्र की जनता का अपमान बताती हैं ।
और हां राष्ट्रवाद भी अघोषित तौर पर घोषित मुद्दा । सैनिकों के नाम पर वोट मांगे जाएं । फिर चुनाव आयोग की फटकार के बाद थोड़ा चुप हो जाएं । पर बात को तो चर्चा में ला ही दिया जाए । जो ज्यादा विरोध करे वो देशद्रोही ।
इस तरह के माहौल में हो रहे हैं चुनाव । बुनियादी सवाल गायब है । सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां बताए तो बेहतर होता और विरोधी दल सत्ता की नाकामी के साथ ही वो खुद क्या करेंगे ये समझा पाते तो कुछ बात होती । पर ऐसा कुछ है नहीं । विरोधियों के लिए मोदी ख़तरा है तो सत्ता दल के लिए मोदी ही जरूरी है । इस सवाल विहीन, विचार विहीन दौर पर लाकर खड़ा कर दिया गया है समाज को । यहां पूछने वाले चुप हैं । बोलने वाले चिल्ला रहे हैं । इस शोर में आम आदमी की आवाज़ कहीं नहीं और गुलाब की पत्तियों की बौछार के बीच लोकतंत्र दुबक कर रह गया है, वह उन कांटों की चुभन महसूस कर रहा है जिनसे गुलाब तोड़े गये । दुबके लोकतंत्र और चुप समाज की तस्वीर में आम चुनाव हो रहे हैं । फिर भी लोकतंत्र पर भरोसा रखने वालों की ताकत से डर तो रहें हैं ही नेता । हां, भव्य रैलियों और कड़प लगे कुर्तों के साथ खुद के सबसे ताकतवर होने का भ्रम पाले हुए सरकार बना लेने और बन जाने को आतुर वे हाथ हिलाते बढ़ रहें हैं आगे । हम अब भी नहीं चेते तो लोकतंत्र में तटस्थ होने के अपराधी होंगे और इतिहास माफ़ नहीं करेगा हमें ।
यह विडंबना ही है कि इस चुनाव में कोई नारा तक भी नहीं है। पहले सकारात्मक, नकारात्मक मुद्दे नहीं तो नारे तो चर्चित होते ही थे । "जय जवान जय किसान ", "हरित क्रांति ", "गरीबी हटाओ ", "कांग्रेस का हाथ सबके साथ ", "ठाकुर बामन बनिया चोर बाकी के सब डीएस फोर","तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार ", "बोफोर्स के दलालों को जूते मारो सालों को", "अच्छे दिन आएंगे ", "विकास ", "विकास पागल हो गया है "। लेकिन इस चुनाव में शुरू में भीड़ कहती रही "चौकीदार चोर है " और फिर सिर्फ "मोदी मोदी " । देश के आम चुनाव का नारा मोदी मोदी ??
इतना ही नहीं आधे ज्यादा हो चुके चुनाव में किसी पत्रकार की कोई रिपोर्ट चर्चित नहीं । किसी संपादक के किसी संपादकीय या लेख की चर्चा तक नहीं । चैनलों की चर्चा तो सिर्फ बिके हुए हैं तक ही होकर रह गई । कहा जाता था कि अखबार जनमानस तैयार करते हैं, पर अब ऐसा कुछ नहीं रहा । अब तो चैनल या अखबार सूचनाएं तक नहीं देते, विश्लेषण की तो बात ही छोड़िए । विज्ञापनों से आटे पड़े अखबारों में खबरों के लिए बची जगह में नेताओं के मुद्दे विहीन भाषणों के अंश ही तो होते हैं । अब गावों में जाकर या शहरों के ही मोहल्लों में जाकर लोगों से बात करने की तकलीफ़ कोई पत्रकार नहीं उठाता । उसे पता है कि उसके कार्पोरेट मीडिया मालिक को इसकी ज़रूरत नहीं, उनके पास तो विज्ञापनों के पैकेज के साथ ही खबरों के पुलिंदे भी आ जाया करते हैं ।
यह इस भयावह समय का आम चुनाव है जिसका नारा मोदी मोदी होकर रह गया है । विवेक हीन और उन्मादी भीड़ मोदी मोदी चिल्लाती सड़कों पर है जिसे देखकर आम आदमी डरा हुआ है । डर रहा है । कुछ सौ लेखक, कलाकार अपील जारी कर रहे हैं । इस खतरे को पहचानिए । मोदी को आने से रोकिए। ये कुछ सौ ही हैं । मुट्ठी भर भी नहीं । विचार वान समाज के विचारहीन में बदलते दौर में आज गांधी या प्रेमचंद सा एक भी लेखक तो नहीं दिखता जिसके आव्हान को लोग पढें, विचार करें । खाया- पीया,अघाया मध्य वर्ग मस्त है और मोदी के बिना उद्धार नहीं कहकर ऑनलाइन पिज़्ज़ा आर्डर कर रहा है । वंदे मातरम् भले ही याद न हो पर स्वैगी, ज़ोमैटो, अमेज़न जैसे शब्द याद है नन्हे - मुन्नों को भी और विडंबना कि इस याद होने पर फेसबुक पर ऐसी ही किसी पोस्ट को लाइक करते हुए मम्मी पापा गर्वित हैं । देश में आम चुनाव हो रहे हैं ।
कुछ इस तरह से भी तलाशा जा रहा है पुनीत गुप्ता को
मानुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान
भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान
रायपुर. इस कहावत को हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं. इसका सीधा सा अर्थ यहीं है कि जब मनुष्य का अच्छा समय होता है तो उसे खुद को बलवान समझने की भूल नहीं करनी चाहिए. क्योंकि जब वक्त खराब होता है तो अर्जुन जैसे धुंरधर का धनुष भी पोंगली बनकर रह जाता है.अगर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह इस कहावत का अर्थ समझ लेते तो हाल-फिलहाल अपमान की जिस तंग गली से वे गुजर रहे हैं उस तंग गली से गुजरने की उन्हें जहमत नहीं उठानी पड़ती. लेकिन शायद... राजनीति में यह धारणा भी कायम है कि क्या सम्मान और कैसा अपमान....। मगर ऐसा नहीं है. अपनी इमेज को चमकाने के लिए करोड़ों रुपए फूंकने वाले रमन सिंह भी शायद भली-भांति जानते होंगे कि राजनीति गंदी तो होती है, लेकिन उसमें चलता तो वहीं है जिसे जनता साफ-सुथरा मानती है. राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पन्द्रह साल तक डाक्टर रमन सिंह की इमेज चाउंर वाले बाबा यानी दानदाता की बनी हुई थीं... अगर पूर्व मुख्यमंत्री संविदा में पदस्थ अफसर अमन सिंह और विवादास्पद आईपीएस मुकेश गुप्ता के चक्रव्यूह में नहीं फंसते तो शायद चौथीं बार भी जनता उन पर अपना बेशुमार प्यार लुटाती.अब आलम यह है कि उनके और उनके परिजनों के खिलाफ छोटे-बड़े हर शख्स ने मोर्चा खोल रखा है. ( यहां तक उनकी अपनी पार्टी के लोग भी पीछे नहीं है.)
हाईकोर्ट से राहत पाने के बाद भी मंगलवार को पुनीत गुप्ता अपना बयान दर्ज करवाने के लिए गोलबाजार थाने नहीं पहुंचे. इस बीच एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें यह कहा गया था कि घोटाले के आरोपी पुनीत गुप्ता क्या बीमार पड़ गए हैं. आखिर वे पुलिस को बयान देने से डर क्यों रहे हैं. इस तस्वीर को गौर से देखिए. तस्वीर में पुनीत गुप्ता को मोस्ट वांटेड बताया गया है और पता बताने वाले को 51 रुपए ( 51 हजार नहीं ) ईनाम देने की घोषणा की गई है.
बघेल ने भेजा आईना तो क्या गलत किया
राजकुमार सोनी
रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक आईना क्या भेज दिया सूबे की सियासत में भूचाल आ गया. हालांकि ऑनलाइन आर्डर किया गया आईना अभी प्रधानमंत्री निवास तक पहुंचा भी नहीं होगा, लेकिन उससे पहले भाजपा के छोटे- बड़े स्तर के सभी नेता नाराज हो गए हैं. भाजपा नेताओं को लग रहा है कि भूपेश बघेल को आईना नहीं भेजना चाहिए था. भाजपा नेता इधर-उधर बयान तो दे रहे हैं,लेकिन वे यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि बघेल को आईने की जगह और कौन सा दूसरा सामान भेजना था जिससे लोकतंत्र थोड़े समय के लिए ही सही सुरक्षित और मजबूत रह पाता. ( जिस देश में लेखक/ पत्रकार/ वकील/ संस्कृतिकर्मी/ फिल्मकार भाजपा को वोट न देने की अपील कर रहे हो तो समझ लीजिए लोकतंत्र किस खतरनाक मुहाने पर खड़ा कर दिया गया है. सबको लग रहा है कि अगर दोबारा मोदी आ गए तो देश नफरत की आग में झुलसकर रह जाएगा. यह कुछ वैसा ही है जैसा हाल के विधानसभा चुनाव में डाक्टर रमन सिंह की सरकार को लेकर कायम था. सबको यह लगने लगा था कि लोकतंत्र निलंबित कर दिया गया है. )
हालांकि आईना भेज देने से भी लोकतंत्र सुरक्षित रह जाएगा इसकी गारंटी कम है. कब एक बम पड़ोसी देश में जाकर गिर जाएगा और पिल-पिल करते हुए भक्त बिल से निकलकर कहने लगेंगे- मोदी है तो मुमकिन है. फिर भी आईना विरोध का... एक सिबांल तो है ही. जब कोई किसी से चिढ़ जाता है तो कहना नहीं भूलता- जाओ... पहले आईने में अपनी सूरत देख लो. बघेल के आईना भेजने के पीछे भी शायद यहीं भाव काम कर रहा है. बघेल ने कहा है- प्रधानमंत्री जी... मैं आपको आईना भेज रहा हूं. इस आईने को आप ऐसी जगह लगाएंगे जहां से आप सबसे अधिक बार गुजरते हो. हो सकता है कि आप आईने का इस्तेमाल न करें. किसी कूड़ेदान में फेंक दें. लेकिन फिर भी आप आईना देखने से बच नहीं पाएंगे. जनता आपको जल्द ही आईना दिखा देगी.
बहरहाल आईना दिखाने पर नेता प्रतिपक्ष धरम कौशिक ने बघेल को राहुल और सोनिया गांधी को भी आईना भेजने की सलाह दी है. कलक्टरी छोड़कर राजनीति में गए ओपी चौधरी ने भी विनम्रता पूर्वक अपनी बात रखी हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह की प्रतिक्रिया बड़ी अजीब है. उनका कहना है- अभी बघेल महज सत्तर दिन के मुख्यमंत्री है, लेकिन वे पन्द्रह साल के मुख्यमंत्री और पांच साल के प्रधानमंत्री को आईना दिखाने का कृत्य कर रहे हैं. यह एक छोटी मानसिकता है. रमन सिंह के इस कथन के बाद बघेल ने भी पलटवार करते हुए कहा है- सवाल सत्तर दिन या सत्तर साल का नहीं है. इस देश में हर किसी को सवाल करने का अधिकार है और मैं वहीं कर रहा हूं. बघेल ने आगे कहा है- मैं किसी भी सवालों से कभी नहीं भागता इसलिए तीन अप्रैल को शाम सात बजे सभी सवालों का जवाब देने के लिए फेसबुक पर लाइव भी रहूंगा. वैसे बघेल की बात में दम तो है. रमन सिंह के पन्द्रह साल के कार्यकाल में पत्रकार सवाल पूछने से डरते थे. जो पत्रकार सवाल करता था उस पर सुपर सीएम और उनके गैंग के लोग एफआईआर दर्ज करवा देते थे. असहमति लोकतंत्र की खूबसूरती होती है इसे रमन सिंह कभी समझ ही नहीं पाए. उन्हें और उनको घेरकर रखने वालों को न जाने क्यों लगता था कि असहमति को कुचलकर ही सत्ता पर काबिज रहा जा सकता है.
खैर.. अब जब कल बघेल फेसबुक पर लाइव रहेंगे तब कई सारी बातों का खुलासा हो सकता है. हो सकता है कि कोई कल यह भी पूछ बैठे कि मोदी तो शेविंग करते नहीं है फिर भी आपने उनको फैटेंशी सिल्वर शेविंग एंड मेकअप वाला आईना क्यों भेज दिया.
बहरहाल आईना राजनीति पर कुछ शायरी याद आ रही है. कृष्ण बिहारी नूर कहते हैं- धन के हाथों बिके हैं सब क़ानून अब किसी जुर्म की सज़ा ही नहीं. चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं. प्रसिद्ध कवि गुलजार ने लिखा है- आईना देखकर तसल्ली हुई. हमको इस घर में जानता है कोई. अब से कुछ अरसा पहले देशबन्धु अखबार में एक कॉलम घूमता हुआ आईना काफी लोकप्रिय हुआ था. यह आईना इधर-उधर घूमता रहता था और कई बार कई रसूखदार लोग नाराज हो जाया करते थे. इस टिप्पणी को लिखते हुए पंड़ित राजनारायण मिश्र जो इस कॉलम को लिखते थे उनकी याद भी आ रही है. किसी अखबार में अगर घूमता हुआ आईना जैसा कोई दमदार कॉलम होता या मीडिया गोदी मीडिया नहीं होता तो शायद भूपेश बघेल को भी ऑनलाइन आईना भिजवाने की आवश्यकता नहीं होती. लेकिन कंसोल इंडिया के इस युग में यह संभव नहीं हो पाया.
युद्ध और उन्माद : मीडिया की नकारात्मक भूमिका
क्या आप इन ढाई महीने के लिए चैनल देखना बंद नहीं कर सकते? कर दीजिए- रवीश कुमार
जो रमन नहीं कर पाए वो भूपेश ने कर दिखाया
राजकुमार सोनी
अब से कुछ अरसा पहले रामगोपाल वर्मा निर्देशित और नागार्जुन अभिनीत एक फिल्म आई थी-शिवा. इस फिल्म में खलनायक का एक जोरदार संवाद था- गुंडे और मवालियों का धंधा लोगों के भीतर पैदा किए गए डर से ही चलता है. जिस रोज लोग डरना बंद कर देंगे... धंधा बंद हो जाएगा. फिल्म के संवाद का जिक्र मैं यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका थोड़ा सा संदर्भ छत्तीसगढ़ से भी जुड़ता है. याद करिए जोगी का कार्यकाल. जब जोगी सत्ता में आए तो उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा के अफसर मुकेश गुप्ता को लाठी भांजने की पूरी छूट दी. प्रदेश में शिवसेना के एक प्रमुख पदाधिकारी धनंजय परिहार से हर अफसर और व्यापारी खौफजदा था. धमकी-चमकी, मारपीट और उगाही के हजारों मामले चल रहे थे.जोगी के कहने पर एक रोज मुकेश गुप्ता ने धनंजय परिहार का जुलूस निकाल दिया तो लोगों ने जमकर तालियां बजाई. लोगों को लगा कि आतंक खत्म हो गया है, लेकिन यह एक भ्रम था. थोड़े दिनों के बाद ही रामावतार जग्गी हत्याकांड हो गया और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनके पुत्र अमित जोगी के साथ-साथ मुकेश गुप्ता विवादों में घिर गए. जोगी पर आरोप लगा कि वे राजनीतिज्ञ नहीं ब्लकि तानाशाह के तौर-तरीकों से सरकार चला रहे हैं.उनके प्रिय अफसर मुकेश गुप्ता हर छोटी-मोटी बात पर लाठी चलाने और गोली से भून देने की धमकी देने लगे. प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा भाजपाई ( रमन सिंह और उनके समूह से जुड़े लोगों को छोड़कर ) होगा जो उनसे प्रताड़ित न हुआ हो. भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय को लाठी-डंडों से पीटा गया. उनके पैर की हड्डी टूट गई. आज भी जब कभी वे उस मंजर का जिक्र करते हैं तो उनके चेहरे पर अपनी ही सरकार के दोगले रवैये का अफसोस साफ तौर पर दिखाई देता है. सच तो यह है कि जोगी को सत्ता से खदेड़ने के पहले भाजपाई... मुकेश गुप्ता को लूप लाइन में भेजने की बात किया करते थे, लेकिन हुआ इसके उलट. भाजपा ने सरकार बनते ही मुकेश गुप्ता को सिर पर बिठा लिया. नंदकुमार साय, पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर सहित अन्य कई नेता चीखते-चिल्लाते रह गए, लेकिन उनकी चीख नक्कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह गई. कुछ दिनों बाद सीएम हाउस में अमन सिंह की इंट्री हो गई. बताते हैं कि उन्हें विक्रम सिंह सिसोदिया यह कहकर लाए थे कि साहब यानि रमन सिंह का कुछ कामकाज संभालना है, लेकिन उन्होंने मुकेश गुप्ता के साथ मिलकर साहब का नहीं बल्कि प्रदेश का कामकाज इस भयावह तरीके से कामकाज संभाला कि साहब की इमेज मटियामेट हो गई. जब कभी भी कोई पत्रकार अमन सिंह से मिलता था तो उनका एक ही डायलॉग सुनता था- यार... काम-काम-काम...। साहब के साथ काम करते-करते पंद्रह साल हो गए. पंद्रह साल से सोया नहीं हूं. पता नहीं आराम कब मिलेगा. शायद उनके पंद्रह साल से जरुरत से ज्यादा जागने का ही नतीजा था कि भाजपा पंद्रह सीटों पर सिमटकर रह गई.
बहरहाल... पंद्रह साल से विराजमान खौफ को भूपेश बघेल अपने देशज अंदाज से धीरे-धीरे खत्म करते जा रहे हैं. उन्हें खौफ को खत्म करने के लिए न तो लाठी चलवाने की जरूरत पड़ रही है और न ही गोली चलवाने की. आतंक का पर्याय बन चुके मुकेश गुप्ता पर कार्रवाई इतनी आसान नहीं थीं. हत्या, साजिश तथा लोगों को झूठे मामले में फंसा देने के आरोपों से घिरे मुकेश गुप्ता पर तगड़ी कार्रवाई के बाद आमजन खुश है तो भाजपा का एक बड़ा वर्ग भी गदगद है. ( दो-चार बड़े नेताओं को छोड़कर ) पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता भी बघेल की तारीफ करने से नहीं चूक रहे हैं. शनिवार को भाजपा के एक जिम्मेदार पदाधिकारी से मुलाकात हुई तो उसने कहा- जो काम हमारे रमन सिंह को करना था वो काम भूपेश बघेल ने कर दिखाया है. भूपेश को सैल्यूट.
वैसे इसमें कोई दो मत नहीं कि कंधे पर शॉल ओढ़कर गांव और परिवार के एक मुखिया जैसी उनकी छवि और एक के बाद एक शानदार निर्णय लेने वाले उनके अंदाज को हर कोई पसन्द कर रहा है. भाजपाइयों और कांग्रेसियों को छोड़कर किसी गांव वाले से भी पूछकर देखिएगा तो कहेगा- पहले फास्फोरस वाली भाजी आती थीं, लेकिन अब लाल भाजी खाने का मजा आ रहा है. मेरा किसी जाति विशेष से कोई विरोध नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि गत पंद्रह सालों से प्रदेश में ठकुराई हावी हो गई थीं. ज्यादातर भाजपा नेताओं और अफसरों का रवैया सामंतवादी हो गया था. लगता था कि बस... अब जमींदार आएंगे. गरीब किसान का खेत छीन लेंगे और उसकी फूल जैसी बिटिया को उठाकर ले जाएंगे और होता भी यहीं था.
कहना न होगा कि छत्तीसगढ़ बेहद खूबसूरत है. यह राज्य अपने खांटी देसी स्वाद की वजह से जाना जाता है. जब कभी आप बाहर जाएंगे तो लोग आपसे तीजन बाई के बारे में पूछेंगे. सुरूजबाई खांडे, हबीब तनवीर के बारे में जानना चाहते हैं. यहां के धान और उगने वाली साग-सब्जियों की भी जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन पंद्रह साल से छत्तीसगढ़ का देसी स्वाद गायब हो गया था. दो-चार को छोड़कर अधिकांश नेता छत्तीसगढ़ियों को लुभाने के लिए छत्तीसगढ़ी में बोलते-बतियाते थे लेकिन ज्यादातर की छत्तीसगढ़ी नकली थीं.अब भूपेश बघेल गांव-गांव जा रहे हैं तो गांव का आदमी भी उनसे मिलने के लिए शहर आ रहा है. अभी इसी सात फरवरी को जब उन्होंने गृह प्रवेश किया तो एक खास बात नजर आई. उनकी विधानसभा के हजारों-हजारों ग्रामीण बधाई देने के लिए सीएम हाउस पहुंचे थे. बघेल ने एक-एक ग्रामीण से मुलाकात की. मुख्यमंत्री निवास में कोट-पैंट-टाई में सेन्ट छिड़कर घूमने वाले अफसरों की जमात भी मौजूद थीं, लेकिन ग्रामीण... शहरी आतंक को खूंटी पर टांगकर बगैर कांटा-चम्मच के सुस्वादु भोजन का लुत्फ उठाने में मशगुल थे. हालांकि बहुत से अफसरों को यह लग रहा था कि कहां देहातियों के बीच फंस गए... लेकिन यह दृश्य सचमुच में आतंक से मुक्ति और जीत का दृश्य था.
बघेल सरकार का एक माहः आगे-आगे देखिए होता है क्या
दिवाकर मुक्तिबोध
17 जनवरी को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस-राज की स्थापना को एक माह पूरा हो गया। 17 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। फिलहाल उनकी सरकार को फटाफट काम करने वाली सरकार मानना चाहिए जिसका लक्ष्य स्पष्ट है। पार्टी का घोषणा-पत्र उसके सामने है जिसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण वायदों पर सरकारी फऱमान जारी हो चुका है। लेकिन यह एक पहलू है जिसमें लोक-कल्याण की भावना प्रबल है। दूसरा पहलू है - राजनीतिक। लक्ष्य है, पूर्ववर्ती भाजपा शासन के दौरान सतह पर आई गड़बडिय़ों एवम् कुछ महाघोटालों की पुन: जाँच। नए सिरे से जाँच की आवश्यकता क्यों है, यह अलग प्रश्न है। इसका तार्किक आधार भी हो सकता है। यह भी संभव है, नई जाँच से नए तथ्य और छिपे हुए चेहरे भी सामने आएं जो जरूरी है पर इसके पीछे राजनीतिक मंशा को भी बखूबी महसूस किया जा सकता है। मंशा है, आगामी अप्रैल-मई में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के पूर्व घोटालों में कथित रूप से लिप्त भाजपा नेताओं, मंत्रियों व अफसरों पर फंदा कसना तथा उन्हें जनता की अदालत में खड़े करना। तीन-चार बड़े प्रकरणों, झीरम घाटी नरसंहार, करीब 36 हजार करोड़ का नागरिक आपूर्ति घोटाला, ई-टेंडरिंग में 4 हजार 600 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी व जनसम्पर्क-संवाद विभाग में भारी वित्तीय अनियमितताओं पर जाँच कमेटी बैठा दी गई है। झीरम का मामला एसआईटी को सौंपा गया है जबकि शेष तीनों राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) को। यह बड़ी हैरत की बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नान घोटाले जिसमें चार्ज शीट अदालत में पेश हो चुकी है, की पुन: जाँच का प्रबल विरोध किया। और इसे वे बदले की कार्रवाई मानते हैं। लेकिन यह जाहिर सी बात है कि सत्ता परिवर्तन के साथ ही भ्रष्टाचार के पुराने दबे, अधदबे मामले बाहर निकाले जाते है व सतही जाँच के बाद रूकी हुई फाइलों पर पड़ी धूल साफ की जाती है और जरुरत के हिसाब से फिर से जाँच बैठाई जाती है। यह सामान्य प्रशासनिक-राजनीतिक प्रक्रिया है। इसमें असहज जैसा कुछ भी नहीं। और जब किसी एक पार्टी का शासन 15 सालों तक चलता रहा हो तो इस दौरान भारी-भरकम गड़बडिय़ों की आशंका स्वाभाविक है जो रमन सरकार के दौर में हुई भी है।
नई कांग्रेस सरकार इसी आशंका का समाधान चाहती है। इसलिए रमन सिंह की प्रतिक्रिया घबराहट भरी राजनीतिक प्रतिक्रिया है। यों भी विधासभा चुनाव में भारी पराजय से उनका व पार्टी का मनोबल गिरा हुआ है। सिर्फ 15 विधायक चुनकर आए हैं। पराजय के बाद पार्टी में गुटीय प्रतिद्वंद्विता जो डेढ़ दशक से सत्ता के दबाव की वजह से दबी हुई थी, उभरकर सामने आई है। हाल ही में जिलेवार समीक्षा बैठकों में नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने पराजय के लिए सरकार, अफसरशाही व प्रादेशिक नेतृत्व को दोषी ठहराते हुए अपनी खीज निकाली तथा उसके बाद सार्वजनिक रूप से आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। इसके पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में भी गुटीय राजनीति का इजहार हो चुका था। बृजमोहन अग्रवाल व ननकीराम कंवर की दावेदारी को ठिकाने लगाकर रमन सिंह अपने समर्थक धरमलाल कौशिक को विपक्ष का नेता बनाने में कामयाब हुए थे। पर पार्टी की हताशा का एक उदाहरण तब सामने आया जब उसके ननकीराम कंवर जैसे सीनियर विधायक ने कांग्रेस सरकार को आवेदन सौंपकर विधानसभा सत्र में ही अपनी ही सरकार के शासनकाल में कुछ आईएएस-आईपीएस अफसरों द्वारा बरती गई अनियमितताओं तथा गड़बडिय़ों की जाँच की माँग की। उनके निशाने पर प्रमुख रूप से सुपर सीएम के रूप में चर्चित निजी प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह व पुलिस महानिदेशक मुकेश गुप्ता थे। राज्य के इतिहास में यह पहली बार है जब विपक्ष का कोई विधायक जो गृह मंतरी जैसे पद पर रहा हो और जिसके अधीन राज्य का पुलिस महकमा हो, दो वरिष्ठतम अफसरों व अन्य के खिलाफ जाँच बैठाने का अनुरोध करे। इससे स्पष्ट होता है कि रमन सरकार के कार्यकाल में मंत्रियों की क्या स्थिति थी? नौकरशाही के सामने वे कितने असहाय थे। और तो और मुख्यमंत्री रमन सिंह भी जिन्होंने 15 वर्षों तक शासन किया, अपने मंत्रियों, नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पा रहे थे। इसका अर्थ है, मुख्यमंत्री अफसरों के एक गिरोह से घिरे हुए थे और उन्हीं के दिमाग से शासन चला रहे थे। दरअसल उन्हें केवल अपनी छवि की चिंता थी जो आम लोगों के सामने हमेशा पाक-साफ बनी रही। इसीलिए ननकीराम कँवर जैसे धाकड़ आदिवासी नेता की भी एक नहीं सुनी गई जबकि वे रमन सरकार को आवेदन पर आवेदन देते गए। अब उन्हीं ननकीराम को कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया और आवेदन पर तुरंत कार्रवाई की। डीजीपी गुप्ता का प्रकरण डीजीपी जेल गिरधारीलाल नायक को सौंपा गया है।
यों एक महीना किसी भी सरकार के कामकाज के आकलन का आधार नहीं हो सकता। पर एक संकेत तो मिलता ही है। भूपेश बघेल का शासन वह संकेत दे रहा है, जो सकारात्मक सोच के साथ बहुत उम्मीद भरा है। एक माह के भीतर जनहित व प्रशासन से संबंधित 15-16 फैसले लेना पहली बार शासन का दायित्व संभालने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं हो सकता लेकिन भूपेश बघेल तपे हुए आक्रामक छवि के नेता है जो अवसरों को गढऩे व माकूल समय पर उनका इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। अजीत जोगी जैसे धुआँधार नेता को उन्होंनेे बाहर का रास्ता दिखाया तथा पार्टी में अपनी राह के लगभग सभी काँटे चुन लिए। बघेल की कर्मठता, दृढ़ प्रशासनिक क्षमता व तेजी से काम करने की प्रवृत्ति सरकार के कामकाज में झलक रही है। दिए हुए समय के भीतर सरकार को रिपोर्ट न सौंपने वाले 13 कलेक्टरों से जवाब तलब करना, उनसे विलंब के लिए स्पष्टीकरण माँगना, यह जाहिर करता है कि यह कोई लुंज-पुंज सरकार नहीं है। लोक-कल्याणकारी कार्यक्रमों के संदर्भ में प्रशासनिक कसावट का यह एक नमूना है। सरकार के खर्चे घटाने की दृष्टि से उन्होंने उन सफेद हाथियों को हटाना शुरू किया है जो राजकोष पर बोझ बने हुए थे। 22 जनवरी को बघेल सरकार ने सुशासन फेलोशिप योजना के तहत नियुक्त किए गए 41 कंसलटेंट की सेवाएँ समाप्त कर दी। इनकी नियुक्तियाँ पिछली सरकार ने की थी जो शैडो कलेक्टर की तरह काम कर रहे थे और जिन्हें शासकीय योजनाओं की मानिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया था। इन्हें सवा से ढाई लाख रूपए प्रतिमाह दिए जा रहे थे। सरकार के कामकाज की यदि ऐसी ही गति बनी रही तो जाहिर है वह एक लोकप्रिय सरकार की अवधारणा को स्थापित व परिभाषित करेगी। बस खतरा केवल एक ही है कि आगे चलकर वह भी पुराने रंग में रंग न जाए।
बघेल सरकार द्वारा एक माह में लिए गए निर्णयों में केवल एक विवादित रहा। वह था, आईपीएस शिवराम कल्लूरी को पुलिस मुख्यालय से हटाकर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में पदस्थ करके नई जिम्मेदारियाँ सौंपना जिसकी अक्टूबर 2016 में बर्खास्तगी व गिरफ्तारी की माँग स्वयं भूपेश बघेल ने की थी। तब बघेल विपक्ष के नेता थे। इस नियुक्ति की बड़ी हैरत भरी व स्तब्धकारी प्रतिक्रिया रही। यह बात हजम नहीं हुई कि जो अधिकारी मानवाधिकार का दोषी है, उसे इतने महत्वपूर्ण विभाग में क्योंकर भेजा गया? इसके पीछे कोई खास रणनीति है? बस्तर में पहले एसपी और बाद में आईजी के रूप में कल्लूरी का कार्यकाल काला कार्यकाल माना जाता है। इस दौरान नक्सलियों के खिलाफ मनचाही जंग लडऩे उन्हें शासन की ओर से अघोषित छूट मिली हुई थी जिसका उन्होंने बेजा फायदा उठाया। कल्लूरी पर नक्सलियों की खोजबीन के नाम पर आदिवासियों पर अत्याचार, मानवाधिकारों का हनन, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी, उनका भयादोहन, उनकी तथा पत्रकारों की बिलावजह गिरफ्तारी जैसे अनेक गंभीर आरोप लगे। मार्च 2011 में सुकमा जिले के ताड़मेटला, मोरपल्ली व तिम्मापुर में कहर बरपाया गया। आदिवासियों के 252 घरों को जला दिया गया। अक्टूबर 2016 में सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में पेश रिपोर्ट में कहा है कि ये घटनाएँ विशेष पुलिस अधिकारियों ने की थी। यही नहीं इस हमले में तीन आदिवासियों की हत्या की गई व महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। कल्लूरी उन दिनों दंतेवाड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे। उन पर कथित माओवादी रमेश नगेशिया की हत्या का आरोप है। कल्लूरी की तानाशाही की वजह से जब रमन सरकार की देशभर में थू-थू हुई और कांग्रेस ने मोर्चा खोला तब मजबूर होकर राज्य सरकार को इस अधिकारी को वहाँ से हटाना पड़ा। अब ऐसे कुख्यात को ईओडब्ल्यू की कमान देना तथा तीन बड़े घोटालों की जाँच का जिम्मा सौंपने के पीछे क्या कोई राजनीतिक मकसद है? रमन सरकार के प्रिय रहे इस अधिकारी से बघेल सरकार शायद यह उम्मीद कर रही है कि उसने जहर को जहर से काटने का इंतजाम कर दिया है। पर इस नियुक्ति से सरकार पर छींटे पड़े हैं। यहाँ सवाल है कल्लूरी ही क्यों? क्या पुलिस विभाग में कल्लूरी से बढ़कर और कोई काबिल अधिकारी नहीं है?
बहरहाल, इस एक मामले को छोड़ दिया जाए तो नई सरकार एक ऐसी कार्यशैली विकसित करने की राह पर है जिसके केन्द्र में गाँव-देहात, गरीब आदिवासी, किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारी, ग्रामीण महिलाएँ, पिछड़े व अति पिछड़े वर्ग के लोग, छोटे उद्यमी एवम् युवा बेरोजगार है। 15 वर्षों तक शासन करने के बावजूद भाजपा सरकार कई बड़ी चुनौतियाँ जिन्हें सुलझाने में वह असफल रही, विरासत में छोड़ गई है। नक्सलवाद, निराशाजनक औद्योगिक वातावरण, जनस्वास्थ्य से बुरी तरह खिलवाड़ करता प्रदूषण, भारी भरकम बेरोजगारी, सरकार में नीचे से उपर तक फैला हुआ संगठित भ्रष्टाचार व बेलगाम नौकरशाही जिसने अंतत: भाजपा सरकार की कब्र खोद दी। यह अच्छा संकेत है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पद सम्हालते ही प्रशासनिक सर्जरी शुरू कर दी और कामकाज का हिसाब माँगना शुरू किया। दरअसल पाँच-पाँच साल की लगातार तीन पारियाँ खेल चुकी रमन सरकार के उन तमाम बड़े फैसलों एवम् कार्य योजनाओं की समीक्षा की जानी चाहिए जिन पर अरबों रूपए खर्च हुए हैं। कांग्रेस को बड़ी उम्मीदों के साथ जनता ने राजसत्ता सौंपी है। पाँच साल चुनौतियों से निपटने भले ही नाकाफी हो, पर आमजनों का विश्वास बनाए रखने के लिए यह पर्याप्त है। जरूरी है सरकार पारदर्शिता, संवेदनशीलता एवम् वैचारिकता का आदर करते हुए काम करें। क्या भूपेश बघेल सरकार एक माह में ही दिखाई पड़ी तेज गति की निरंतरता को कायम रख पाएगी? सवाल बड़ा है पर उम्मीद भी कम नहीं।
पता नहीं रमन सिंह जंगल से कब बाहर निकलेंगे.
राजकुमार सोनी
पूर्व मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह के फेसबुक पेज पर मंगलवार को दंभ से भरी हुई एक अजीब सी तुकबंदी कविता सुनने को मिली. पहले कविता का उल्लेख कर देता हूं फिर आगे कोई बात लिखूंगा. तो महान रचना इस तरह की है-
बदले की जांच से भला, सत्य को कहां आंच आई है
संख्या में अधिक हो जाने से भला
क्या सियारों ने सिंह पर विजय पाई है
गरीबों को चावल देना, तुम्हारी नजर में अपराध है.
मेरे आदिवासी भाइयों का, क्या सरई का बीजा खाना याद है
भूखों को खाना देना अगर मेरे अपराध में गिना जाएगा
तो लाख डिगा ले कदम मेरे, ये अपराध फिर से किया जाएगा
अपने द्वेष के तराजू में मेरे कर्मों को क्या तौलोगे
वर्षों सेवा किया है हमने क्या उस पर भी कुछ बोलोगे
झूठे वादों से तुम पहुंचे हो, अब उन्हें पूरा करने की बारी है
मेरे हौसलों को तोड़ने की चेष्टा न कर
मेरे साथ मेरी छत्तीसगढ़ महतारी है.
वाह- वाह... वाह... वाह... धांसू... धांसू... गजब... गजब...कहना तो मुश्किल होगा लेकिन यह तो कहा ही जा सकता है कि यह कविता सुरेंद्र दुबे शैली की है. इस तुकबंदी कविता में साफ तौर पर जांच का डर नजर आता है. लगता है कि रमन सिंह जांच से विचलित हो गए हैं और खुद को संभालने के लिए कविता-कहानी का सहारा ले रहे हैं. यह सही है कि गरीबों और भूखों का पेट भरना अपराध नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा राशनकार्ड बनाकर गरीबों और भूखों का चावल और उसका पैसा हड़प लेना क्या पराध की श्रेणी में नहींं आता है. कहते हैं कि राजनीतिज्ञ कभी सेवानिवृत नहीं होता. यह बात सौ फीसदी सत्य भी है, मगर जनता द्वारा खारिज किए गए सत्य को भी समय रहते स्वीकार कर लेना समझदारी मानी जाती है.अभी तक रमन सिंह यह मानने को तैयार नहीं है ( शायद ) कि उनके दल को जनता ने खारिज कर दिया है. जनता ने उनके वर्षों की साधना और तपस्या पर जिस तरह का पुरस्कार देने लायक समझा उन्हें उस तरह का पुरस्कार दे दिया है. उनके और उनके कद्दावर अफसरों की अनवरत साधना के चलते ही पार्टी महज पन्द्रह सीटों पर सिमटकर रह गई है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता संभालने के बाद जिस रोज झीरम घाटी की जांच की घोषणा की उसी दिन से रमन सिंह यह कहते आ रहे हैं कि नई सरकार बदलापुर की राजनीति कर रही है. वैसे रमन सिंह ने बदलापुर-बदलापुर कहते-कहते कभी यह नहीं कहा कि आखिर उन्होंने भूपेश बघेल के साथ ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से उन्हें बदला लेने की जरूरत पड़ रही है. जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से भूपेश बघेल की भूमिका की बात है तो वे काफी पहले से यह कहते रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो झीरम घाटी की घटना की जांच होगी. नान घोटाले की जांच होगी. पनामा पेपर में छत्तीसगढ़ के नवाज शरीफ को जेल भेजा जाएगा. अंतागढ़ टेप कांड की जांच की मांग वे कई स्तरों पर कर चुके हैं. फिर भी पूर्व मुख्यमंत्री को अगर लगता है कि भूपेश बघेल उनसे किसी खास बात का बदला ले रहे हैं तो उन्हें जनता को बताना ही चाहिए कि उन्होंने भूपेश बघेल के साथ ऐसा क्या किया था.
बदलापुर-बदलापुर की चीख-चिल्लाहट के पीछे का एक मजेदार वाक्या यह भी है कि यह आवाज सिर्फ और सिर्फ रमन सिंह की तरफ से उठ रही है. एक- दो हारे हुए नेता भी बदलापुर-बदलापुर कर रहे हैं, लेकिन शेष किसी भी बड़े नेता ने यह नहीं कहा कि भूपेश बघेल बदलापुर की राजनीति कर रहे हैं. वैसे पूर्व मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनके पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्टी-पत्री सौंपकर यह क्यों कहा कि साहब... मुकेश गुप्ता के खिलाफ जांच करवा दीजिए. सुना तो यह भी जा रहा था कि सुपर सीएम की पदवी से विभूषित अमन सिंह केंद्र में अपनी नौकरी-चाकरी का जुगाड़ बिठाने में सफल हो गए हैं, लेकिन इधर हाल के दिनों में उनके ही खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय ने जांच के लिए राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिख दिया है. अब अगर पीएमओ के पत्र पर जांच प्रारंभ हो जाएगी तब भी क्या रमन सिंह यहीं कहेंगे कि बदलापुर की राजनीति हो रही है. यह एक यक्ष प्रश्न तो है कि जांच की मांग उनके ही विधायक कर रहे हैं. पीएमओ पत्र लिखकर कह रहा है कि जांच करिए.
सिंह और सियार
कविता में किसी चंद्रवरदाई ने रमन सिंह को सिंह यानि शेर बताया है और कहा है कि संख्या बल में अधिक हो जाने बावजूद सियार कभी भी सिंह पर विजय नहीं पा सकते. हालांकि कविता पढ़ने वाले की आवाज काफी महीन और पतली है जिसे सुनकर सिंघम के आ जाने का अहसास रोमांच के बजाय हास्य में बदल जाता है. पाठकों को याद होगा कि अभी हाल के दिनों में विधानसभा में पूर्व संसदीय मंत्री अजय चंद्राकर ने भूपेश को राजा बताते हुए कहा था कि वे अपने स्वभाव के कारण राजा बने हैं जानवरो के कारण नहीं. उनकी इस टिप्पणी के बाद खूब बवाल मचा था. सत्तापक्ष के विधायकों ने जानवर बताए जाने पर जोरदार आपत्ति जताकर अपना विरोध दर्ज किया था.
अब एक बार फिर संख्या बल में अधिक लोगों को सियार की उपाधि दी गई है. भले ही वह उपाधि कविता में दी गई है. लेकिन जंगल/ सिंह/ शेर/ सियार... इन शब्दों को देखकर लगता है कि रमन सिंह अब भी जंगल से बाहर नहीं निकल पाए हैं. राजनीति के एक बड़े जानकार की टिप्पणी है- जब कोई जनता के दिलों में राज करने के बजाय जंगल में राज करने की फितरत पाल लेता है तो ऐसा शख्स खुद को सिंह बताकर अन्य लोगों को सियार-गीदड़, बंदर-भालू कहने लगता है. पता नहीं रमन सिंह जंगल से कब बाहर निकलेंगे. अब तो रमन सिंह को जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए. पन्द्रह सीटों पर सिमटी हुई पार्टी का कोई नेता अगर बहुमत हासिल करने वाली पार्टी के विधायकों को सियार या गीदड़ कहता है तो यह बहुमत के साथ-साथ लोकतंत्र का अपमान भी है. जो कविता रमन सिंह ने पोस्ट की है वैसी कविता तो कोई हारा हुआ पार्षद भी पोस्ट नहीं करता है.




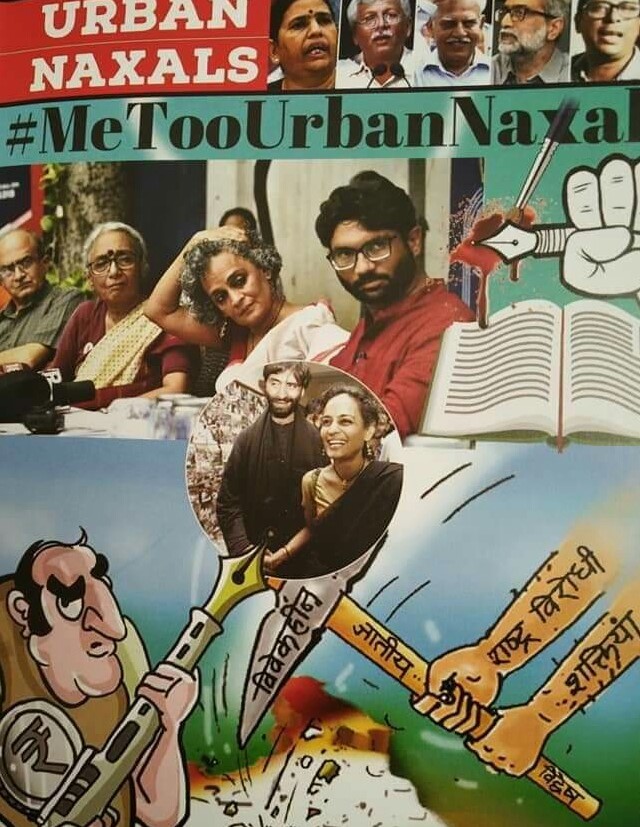






.jpg)





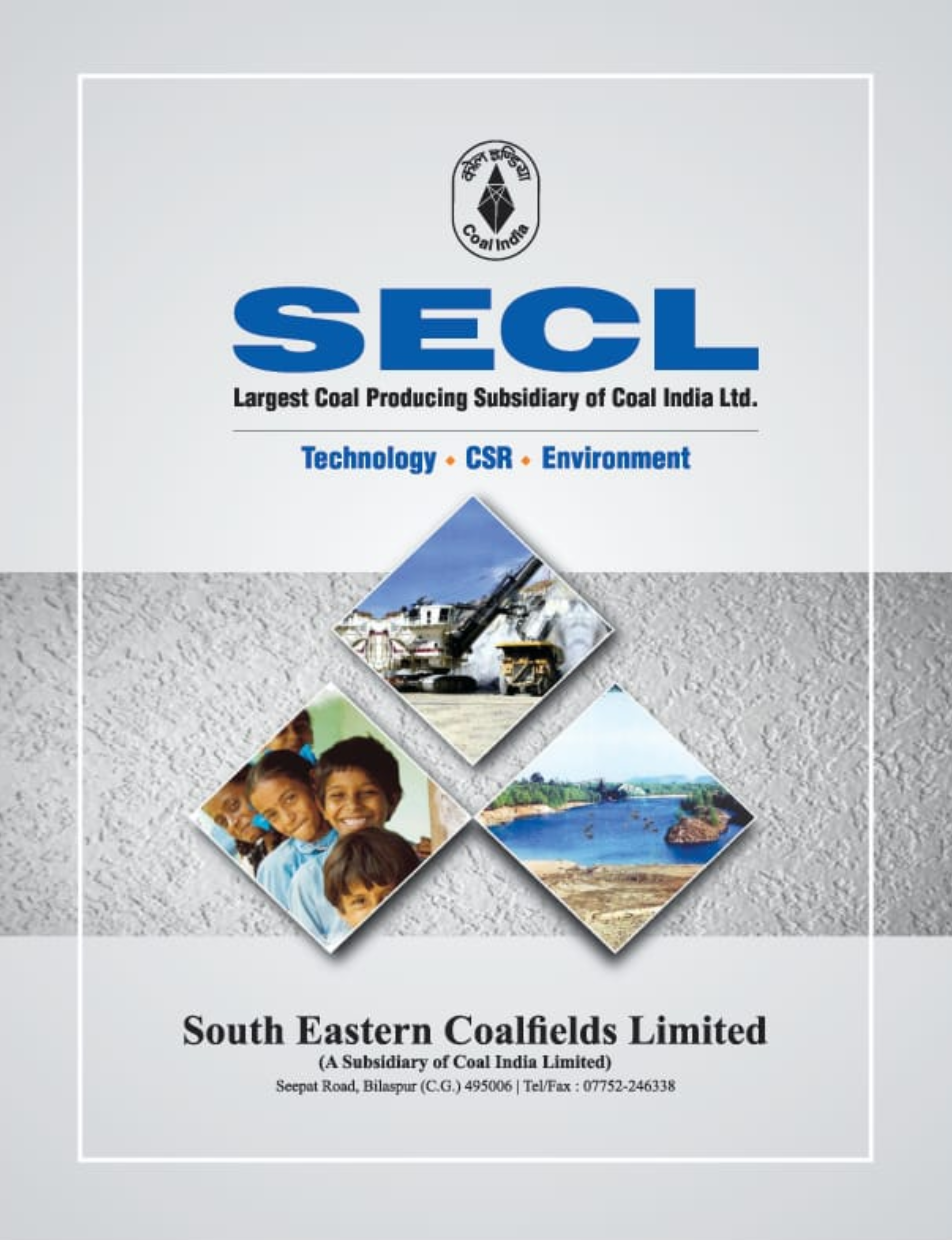












.jpg)









