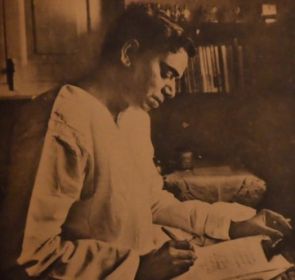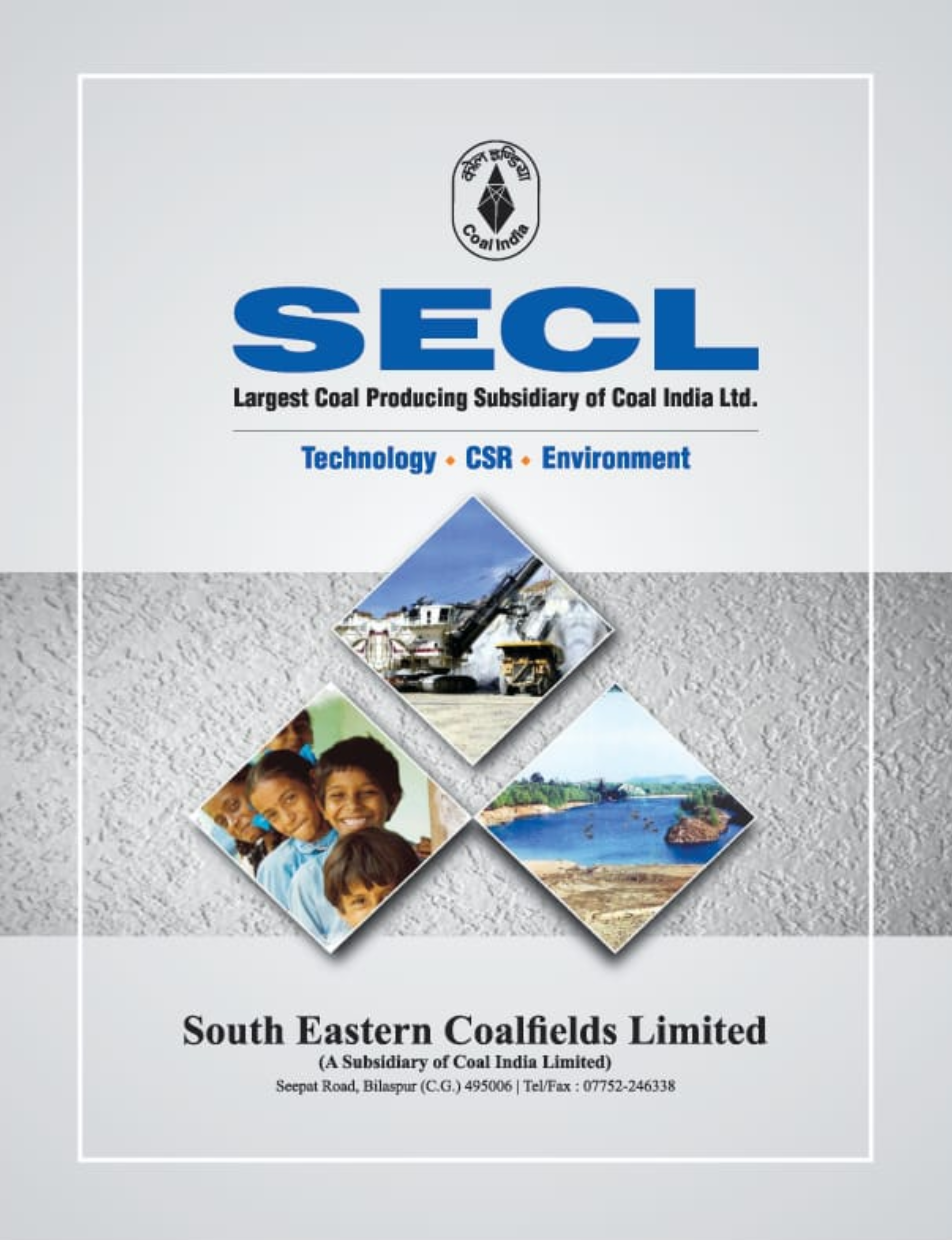फिल्म

घोर व्यावसायिक और यथास्थितिवादी फिल्म- हंस झन पगली फंस जबे.
देश के प्रसिद्ध कथाकार कैलाश बनवासी बता रहे हैं कि हंस झन पगली फंस जबे... महज एक मुनाफा बटोरने वाली फिल्म है. इसका छत्तीसगढ़ के कठोर यथार्थ से जरा भी लेना-देना नहीं है. यह एक घोर यथास्थितिवादी फिल्म है. फिल्म को लेकर कैलाश बनवासी की यह लंबी टिप्पणी बहुत सारे सवाल खड़ा करती है.
कैलाश बनवासी
छोटेलाल साहू द्वारा निर्मित और सतीश जैन द्वारा निर्देशित ‘छत्तीसगढ़ी’(?) फिल्म ‘हंस झन पगली फंस जबे’ को रिलीजिंग दिन ही देखकर पत्रकार राजकुमार सोनी ने अपने वेबसाइट अपना मोर्चा डाट काम में समीक्षा करते हुए टाइटल में लिखा था—‘एक बण्डल फिल्म जो सुपर हिट हो सकती है’.तब मैंने सवाल उठाया था कि भला एक बंडल फिल्म कैसे सुपर हिट हो सकती है? लेकिन राजकुमार सोनी का आंकलन बिलकुल सही निकला. यह फिल्म थिएटरों में रिलीज के एक महीने बाद भी बालीवुड की फिल्मों को मात देते हुए जबरदस्त कमाई कर रही है.इसके इतने ज्यादा हिट होने के कारण इसके वास्तविक कारणों को जानने मैं यह फिल्म देखने गया.और पाया कि राजकुमार सोनी की दोनों बातें सही हैं—फिल्म सुपर हिट हो चुकी है.लेकिन वास्तव में बंडल है. लेकिन मेरी राय उस टिप्पणी से सहमत होते हुए भी कुछ अलग है.
सतीश जैन मुख्यरूप से सिने व्यवसायी हैं,उन्होंने ऐसी फ़िल्में बनाई जिन्हें दर्शक देखने थिएटर जा रहा है. सिनेमा उद्योग में जिस तरह बड़ी-बड़ी फ़िल्में मुंह के बल गिर रही हैं,तमाम लटकों-झटकों के बाद भी फ्लॉप हो रही हैं,ऐसे में ‘हंस झन पगली फंस जबे’ जैसी फिल्म का हिट होना,मुझे एक सामान्य छत्तीसगढ़ी’ दर्शक की हैसियत से ‘अपील’ तो करता ही है. फिल्म में नया कुछ भी नहीं है. एक प्रेम कहानी और नायक-नायिका के पिताओं की आपसी दुश्मनी की कहानी दर्शक बॉबी’ के समय से देखते आ रहे हैं.फिल्म डेविड धवन मार्का हिट करने- कराने के तमाम फार्मूलों- एक्शन,ड्रामा,कॉमेडी -- से लैस है जो कभी ‘मैंने प्यार किया’ की याद दिलाती है तो कभी ‘फूल और कांटे’ की तो कभी ‘हम आपके हैं कौन’ या ‘दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे ’ की.यानि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा,भानुमती ने कुनबा जोड़ा’.स्वीकारना होगा,निर्माता-निर्देशक अपने उद्देस्श्य में सफल हैं. प्रश्न मेरे सामने यही है की छत्तीसगढ़ी दर्शकों ने इसे हाथो- हाथ क्यों लिया? हिंदी की हर दूसरी फिल्म की तर्ज पर बनी इस फिल्म में उन्हें ऐसा क्या नया अनोखा मिल गया जो किसी और फिल्म में नहीं था ? इसका जवाब हमारे सांस्कृतिक स्तर पर छिपा है. क्योंकि यहांं फिल्म की भाषा ही सबसे बड़ा आकर्षण है.लोग अपनी बोली-भाषा में हीरो-हिरोइन को बोलते देखना चाहते हैं,इसलिए,जरा-सा क्लिक मिलते ही लोग टूट पड़े हैं जो लोग इसे देखने जा रहे हैं,देखा जाय तो वे कौन लोग हैं? इसके सबसे बड़े दर्शक वे छत्तीसगढ़ी युवक-युवतियां हैं जो गांवों से कट चुके हैं. जिनका समय के साथ बहुत तेजी से शहरीकरण हो चुका है,और जो मनोरंजन के नाम पर सिनेमाई छल-प्रपंचों के गहरे शिकार हैं. ये छोटे-मोटे अस्थायी कामों में लगे लोग हैं,जिन्हें रोज खाना और रोज कमाना है. ज़ाहिर है ये अपनी संस्कृति से जुड़े होने का भ्रम तो बनाए हुए हैं,जबकि वास्तव में उससे कटते जा रहे हैं.ये वे लोग हैं जिन्हें अपनी भाषा-बोली से बहुत प्यार है लेकिन इस समूह का सांस्कृतिक स्तर अभी भी बीस साल पुराना और पिछड़ा हुआ है. है. दूसरे,इस फिल्म ने अपने केंद्र में छत्तीसगढ़ी जनता या लोगों को तो रखा ही नहीं है! ना यहांं गांव हैं,ना किसान हैं,ना खेतखार,ना बारी-बखरी! ना ही गाय-बैल! कुछ भी तो दूर-दूर तक नहीं है. ना ही उन भीषण समस्याओं की कोई झलक है जिनसे छत्तीसगढ़ आज भी दो-चार है--- किसान या खेती की समस्या, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार,शोषण,,गांवों में आते बदलाव,कुछ भी तो नहीं है. फिर इसे भला छत्तीसगढ़ी फिल्म क्यों कहें? ना ही यहांं की लोक-परम्परा या रीति-रिवाज, ना नाच-गीत हैं ना संस्कृति ! फिर भी सब पसंद कर रहे हैं तो क्या यह नही मान लिया जाय कि लोगों में अपनी स्थानीयता,और संस्कृति के लिए अब वह पहले वाला प्रेम रहा ही नहीं, जो कभी चंदैनी-गोंदा या खुमान साव ने अपने समय में जगाने की कोशिश की थी.इसमें संस्कृति के नाम पर मात्र विवाह के चंद फुटेज हैं. सच तो यह है कि ऐसी फ़िल्में भोजपुरी या पंजाबी किसी भी भाषा में डब की जा सकती है और इससे इसके आंचलिक सौन्दर्य पर कोई खतरा नहीं रहेगा. इस फिल्म में जिसका 40 प्रतिशत हिस्सा बोलेरो-जाइलो-बुलेट जैसी गाड़ियों के दौड़ते रहने,भागमभाग,जबरदस्त हिंसा और नफरत से भरी हुई है,इसमें छत्तीसगढ़ी के नाम पर अगर आप कुछ खोजने निकलेंगे तो सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी.
फिल्म की असली ताकत इसका लोकप्रिय गीत-संगीत है,जिसमें लोकधुनों की छौंक बघारी गई है. संगीत निर्देशक सुनील सोनी और गीतकार रामेश्वर वैष्णव की इस बात के लिए प्रसंशा की जानी चाहिए. यही बात फिल्म के कोरियोग्राफी के बारे में कही जा सकती है. फिल्म नाटक की तरह एक सामूहिक काम है.इसलिए फिल्म बनाना आर्थिक रूप से मुश्किल तो है ही.अपना पैसा लगाकर डूबाना कोई नहीं चाहता. इसलिए व्यावसायिकता सिनेमा की सबसे पहली शर्त हो जाती है.इसे यों कह सकते हैं,कि इन निर्माता-निर्देशकों को अपना व्यवसाय करना अच्छे से आता है.सतीश जैन जब कहते हैं कि मैं वही फ़िल्में बनता हूँ जो लोग पसंद करते हैं, तो इस कथन में उनकी एजेंडे को बखूबी देखा जा सकता है.
लेकिन जैसे ही आप इस फिल्म को कला के मानदंडों पर रखने लगेंगे तो यह रेत की दीवार की तरह भरभराकर गिर जाती है.इसे वस्तुतः छत्तीसगढ़ी मूल्यों-मान्यताओं,संस्कृति या जागृति से कुछ भी लेना-देना नहीं है. अगर होता,तो ऐसी वाहियात फिल्म नहीं बनाते. अपनी विचारधारा में यह फिल्म बहुत हिंसक है और ‘मसल-पावर’ को ही स्थापित करती है. इसमें जिस किस्म की घृणा,घमंड,गुस्सा और नफरत को दिखाया गया है,इससे यह छत्तीसगढ़ी फिल्म कम यूपी-हरियाणा-राजस्थान के घोर सामंती खाप पंचायतों की याद ज्यादा दिलाती है जो बेटे-बेटियों के प्रेम-विवाह पर अपने कथित सम्मान के लिए ‘ऑनरकिलिंग’ तक चले जाते हैं. यह किसी बदलाव की बात नहीं करती,बस दोनों ठेकेदारों की आपसी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और खूनी रंजिश को ही उभारती है. एक समय तो लगने लगता है कि यह ‘ऑनरकिलिंग’ की तरफ बढ़ रही है. यही इस घोर फार्मूला फिल्म में परोसा गया है. हीरो प्रेम के लिए लम्पटई का सहारा लेता है. जिसमें दर्शकों को खुश होते देखा जा सकता है.इस फिल्म को यहांं के बड़े परिवारों में प्रचलित दाऊगिरी और दादागिरी के संदर्भ में ही देख सकते हैं जो कि अब पुरानी बात हो गई है.ऐसे माता-पिता को आज के बदले छत्तीसगढ़ की नयी पीढ़ी खुद ही रिजेक्ट कर देती है. फिल्म में ऐसे जालिम पिताओं को याद करके नायिका का उनका चित्र बनाना ही नहीं,बल्कि भगवान् शंकर और विष्णु का रूप दे देना बेहद हास्यास्पद ही नहीं,दयनीय है. लेकिन चूंकि वह पिता है,और दर्शकों की पितृभक्ति की भावनाओं को कैश करना है,इसलिए उन्हें भगवान् का दर्जा देते दिखा दिया गया है.वस्तुतः यही छत्तीसगढ़ की पिछड़ी मानसिकता है,जिसे बदलने की जरूरत है. रिश्ने-नाते के नाम पर भावात्मक रूप दिखाकर जल्लाद जैसे बापों को सम्मान देना कहांं तक न्यायसंगत है?फिल्म में किसी तार्किकता की तो बात ही नहीं की जाए तो अच्छा होगा. अंधाधुंध फायरिंग हो रही है. हत्या हो रही है और पुलिस का नामोनिशान नहीं .यह समाज में प्रचलित पितृसत्ता को ही मजबूत नहीं करती,प्रेम या कॉमेडी के नाम पर लम्पटई को जगह देती है.इस फिल्म का टाइटल ही लड़की को फंसने-फंसाने के रूप में ही व्यक्त कर रहा है.यह स्त्रीविरोधी भी इस मायने में है कि छत्तीसगढ़ में स्त्रीशक्ति बहुत मजबूत और मुखर है -तीजन बाई,सुरूजबाई खांडे फूलबासन बाई,इत्यादि. लेकिन यहांं नायिका समेत सभी स्त्रियांं दब्बू हैं और महज शो पीस हैं. जो है वह केवल रस्मों को निभाने के लिए.
अगर यह फिल्म लोगों को पसंद आ रही है,तो इसमें निर्माता-निर्देशकों से ज्यादा दर्शकों का दोष है,जो सही फिल्म देखने का स्तर नहीं पा सके हैं. यह घोर यथास्थितिवादी फिल्म है,जो किसी बदलाव के लिए नहीं,वरन सिर्फ मनोरंजन के लिए है.जो अच्छे निर्देशक होते हैं,वे अपनी फिल्म के माध्यम से अपने दर्शकों की सोच,चेतना का स्तर उठाने के लिए प्रयास करते हैं.छत्तीसगढ़ में यहांं की पिछड़ी हुई सोच को बदलने के लिए अच्छे निर्माता-निर्देशकों को इस दिशा में अभी बहुत काम करने की जरूरत है.लेकिन यह ऐसे ही व्यावसायिक फार्मूले से घिरे रहें तो इनसे किसी भी तरह की उम्मीद करना बेमानी है. अभी भी यहांं की उच्चतर भावनाओं का संधान कर, प्रगतिशील जीवन मूल्यों को स्थापित करने वाले फिल्मों की बेहद जरूरत है.जो इसे सिर्फ मुनाफा बटोरने का साधन मात्र नहीं समझे. वैसे ही लोगों से कोई उम्मीद की जा सकती है.
कैलाश बनवासी का दूरभाष नंबर है- 98279 93920









.jpg)